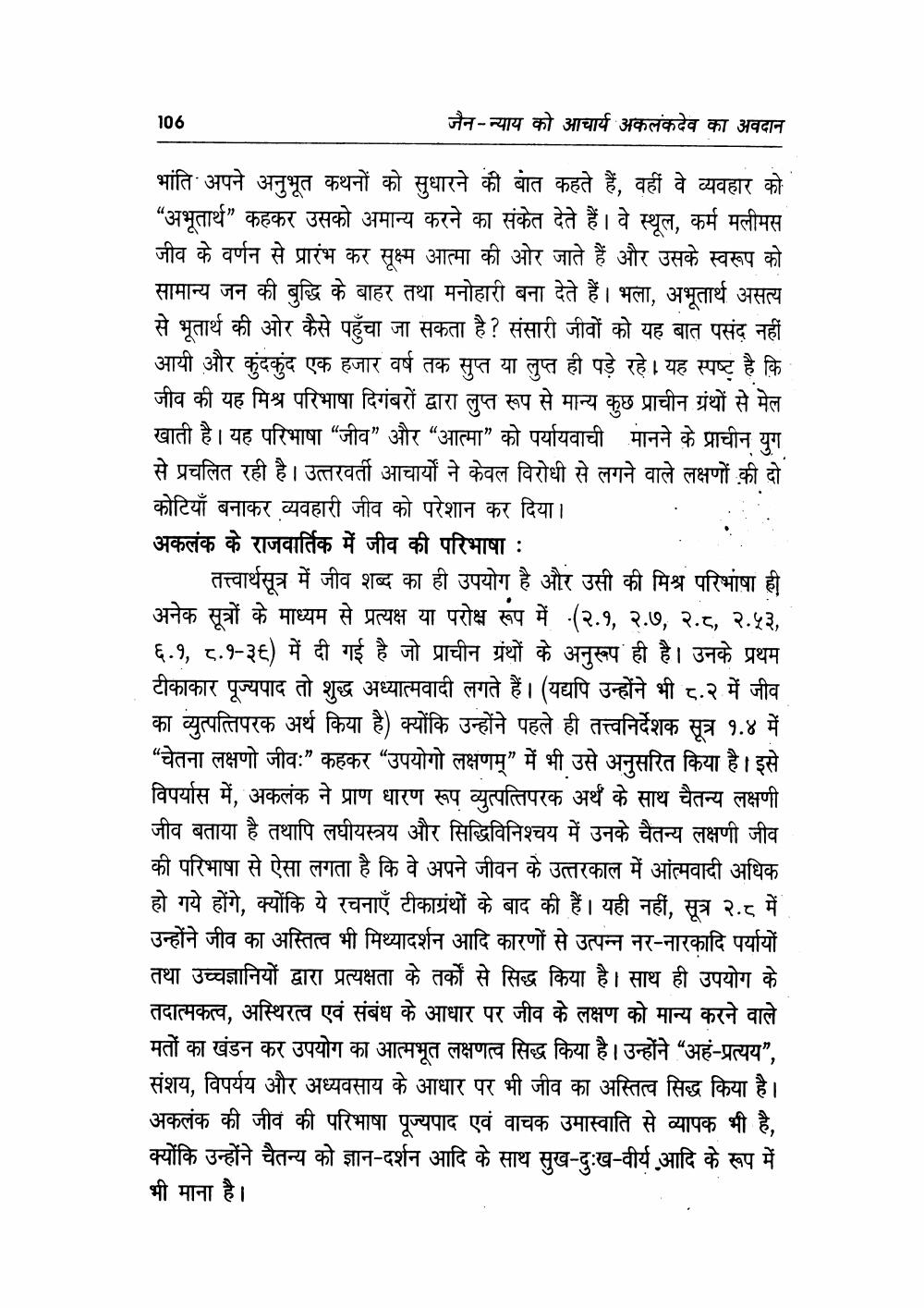________________
106
जैन- न्याय को आचार्य अकलंकदेव का अवदान
भांति अपने अनुभूत कथनों को सुधारने की बात कहते हैं, वहीं वे व्यवहार को “अभूतार्थ" कहकर उसको अमान्य करने का संकेत देते हैं। वे स्थूल, कर्म मलीमस जीव के वर्णन से प्रारंभ कर सूक्ष्म आत्मा की ओर जाते हैं और उसके स्वरूप को सामान्य जन की बुद्धि के बाहर तथा मनोहारी बना देते हैं। भला, अभूतार्थ असत्य से भूतार्थ की ओर कैसे पहुँचा जा सकता है? संसारी जीवों को यह बात पसंद नहीं आयी और कुंदकुंद एक हजार वर्ष तक सुप्त या लुप्त ही पड़े रहे। यह स्पष्ट है कि जीव की यह मिश्र परिभाषा दिगंबरों द्वारा लुप्त रूप से मान्य कुछ प्राचीन ग्रंथों से मेल खाती है। यह परिभाषा “जीव” और “आत्मा” को पर्यायवाची मानने के प्राचीन युग से प्रचलित रही है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने केवल विरोधी से लगने वाले लक्षणों की दो कोटियाँ बनाकर व्यवहारी जीव को परेशान कर दिया। अकलंक के राजवार्तिक में जीव की परिभाषा :
तत्त्वार्थसूत्र में जीव शब्द का ही उपयोग है और उसी की मिश्र परिभाषा ही अनेक सूत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में .(२.१, २.७, २.८, २.५३, ६.१, ८.१-३६) में दी गई है जो प्राचीन ग्रंथों के अनुरूप ही है। उनके प्रथम टीकाकार पूज्यपाद तो शुद्ध अध्यात्मवादी लगते हैं। (यद्यपि उन्होंने भी ८.२ में जीव का व्युत्पत्तिपरक अर्थ किया है) क्योंकि उन्होंने पहले ही तत्त्वनिर्देशक सूत्र १.४ में “चेतना लक्षणो जीवः” कहकर “उपयोगो लक्षणम्” में भी उसे अनुसरित किया है। इसे विपर्यास में, अकलंक ने प्राण धारण रूप व्युत्पत्तिपरक अर्थ के साथ चैतन्य लक्षणी जीव बताया है तथापि लघीयस्त्रय और सिद्धिविनिश्चय में उनके चैतन्य लक्षणी जीव की परिभाषा से ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन के उत्तरकाल में आत्मवादी अधिक हो गये होंगे, क्योंकि ये रचनाएँ टीकाग्रंथों के बाद की हैं। यही नहीं, सूत्र २.८ में उन्होंने जीव का अस्तित्व भी मिथ्यादर्शन आदि कारणों से उत्पन्न नर-नारकादि पर्यायों तथा उच्चज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्षता के तर्कों से सिद्ध किया है। साथ ही उपयोग के तदात्मकत्व, अस्थिरत्व एवं संबंध के आधार पर जीव के लक्षण को मान्य करने वाले मतों का खंडन कर उपयोग का आत्मभूत लक्षणत्व सिद्ध किया है। उन्होंने “अहं-प्रत्यय", संशय, विपर्यय और अध्यवसाय के आधार पर भी जीव का अस्तित्व सिद्ध किया है। अकलंक की जीवं की परिभाषा पूज्यपाद एवं वाचक उमास्वाति से व्यापक भी है, क्योंकि उन्होंने चैतन्य को ज्ञान-दर्शन आदि के साथ सुख-दुःख-वीर्य आदि के रूप में भी माना है।