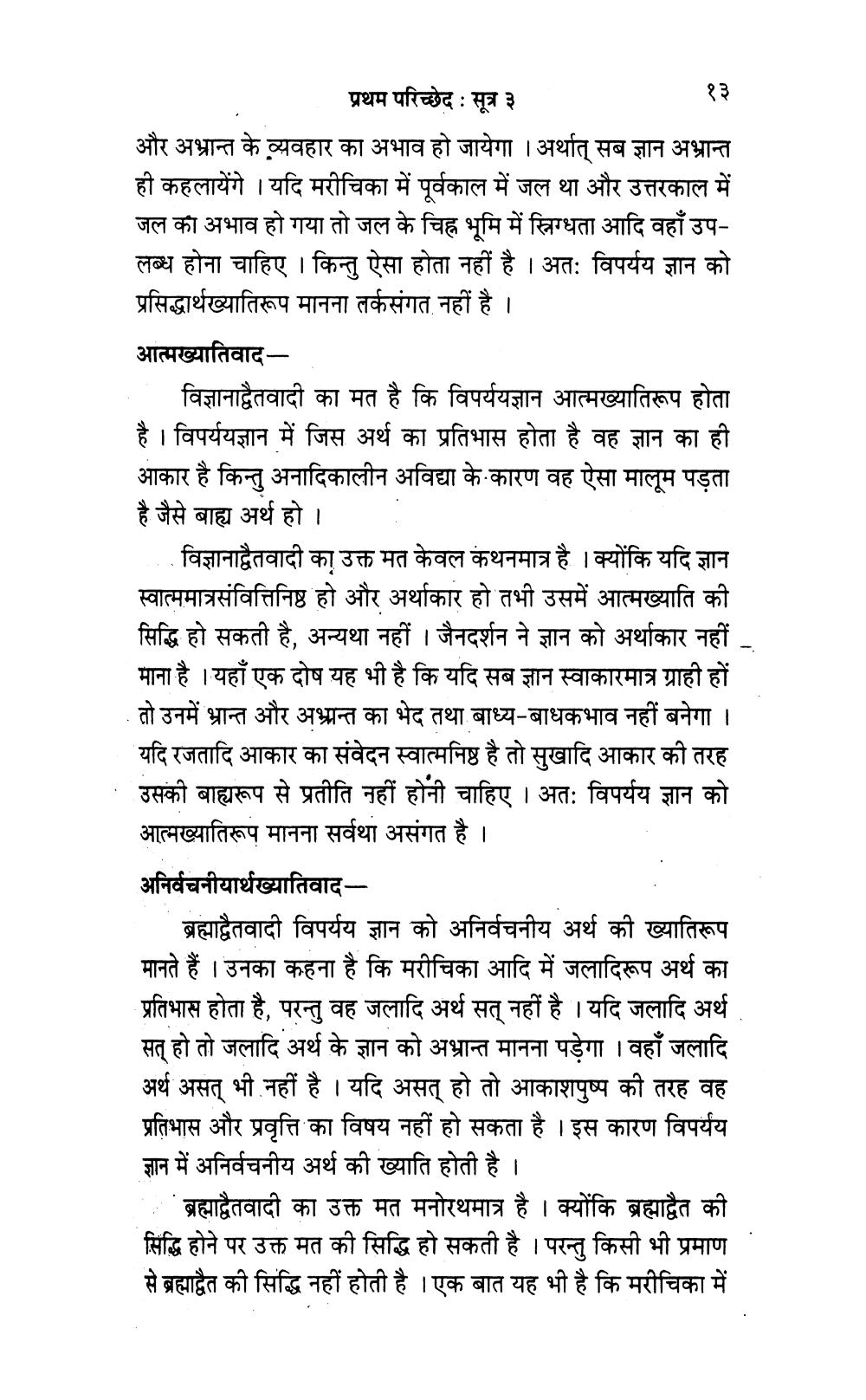________________
प्रथम परिच्छेद: सूत्र ३
१३
और अभ्रान्त के व्यवहार का अभाव हो जायेगा । अर्थात् सब ज्ञान अभ्रान्त ही कहलायेंगे । यदि मरीचिका में पूर्वकाल में जल था और उत्तरकाल में जल का अभाव हो गया तो जल के चिह्न भूमि में स्निग्धता आदि वहाँ उपलब्ध होना चाहिए । किन्तु ऐसा होता नहीं है । अतः विपर्यय ज्ञान को प्रसिद्धार्थख्यातिरूप मानना तर्कसंगत नहीं है ।
आत्मख्यातिवाद
विज्ञानाद्वैतवादी का मत है कि विपर्ययज्ञान आत्मख्यातिरूप होता है । विपर्ययज्ञान में जिस अर्थ का प्रतिभास होता है वह ज्ञान का ही आकार है किन्तु अनादिकालीन अविद्या के कारण वह ऐसा मालूम पड़ता है जैसे बाह्य अर्थ हो ।
विज्ञानाद्वैतवादी का उक्त मत केवल कंथनमात्र है । क्योंकि यदि ज्ञान स्वात्ममात्रसंवित्तिनिष्ठ हो और अर्थाकार हो तभी उसमें आत्मख्याति की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं । जैनदर्शन ने ज्ञान को अर्थाकार नहीं माना है । यहाँ एक दोष यह भी है कि यदि सब ज्ञान स्वाकारमात्र ग्राही हों तो उनमें भ्रान्त और अभ्रान्त का भेद तथा बाध्य - बाधकभाव नहीं बनेगा । यदि रजतादि आकार का संवेदन स्वात्मनिष्ठ है तो सुखादि आकार की तरह उसकी बाह्यरूप से प्रतीति नहीं होनी चाहिए । अतः विपर्यय ज्ञान को आत्मख्यातिरूप मानना सर्वथा असंगत है ।
अनिर्वचनीयार्थख्यातिवाद -
ब्रह्माद्वैतवादी विपर्यय ज्ञान को अनिर्वचनीय अर्थ की ख्यातिरूप मानते हैं । उनका कहना है कि मरीचिका आदि में जलादिरूप अर्थ का प्रतिभास होता है, परन्तु वह जलादि अर्थ सत् नहीं है । यदि जलादि अर्थ सत् हो तो जलादि अर्थ के ज्ञान को अभ्रान्त मानना पड़ेगा । वहाँ जलादि अर्थ असत् भी नहीं है । यदि असत् हो तो आकाशपुष्प की तरह वह प्रतिभास और प्रवृत्ति का विषय नहीं हो सकता है । इस कारण विपर्यय ज्ञान में अनिर्वचनीय अर्थ की ख्याति होती है ।
ब्रह्माद्वैतवादी का उक्त मत मनोरथमात्र है । क्योंकि ब्रह्माद्वैत की सिद्धि होने पर उक्त मत की सिद्धि हो सकती है । परन्तु किसी भी प्रमाण ब्रह्माद्वैत की सिद्धि नहीं होती है । एक बात यह भी है कि मरीचिका में
-