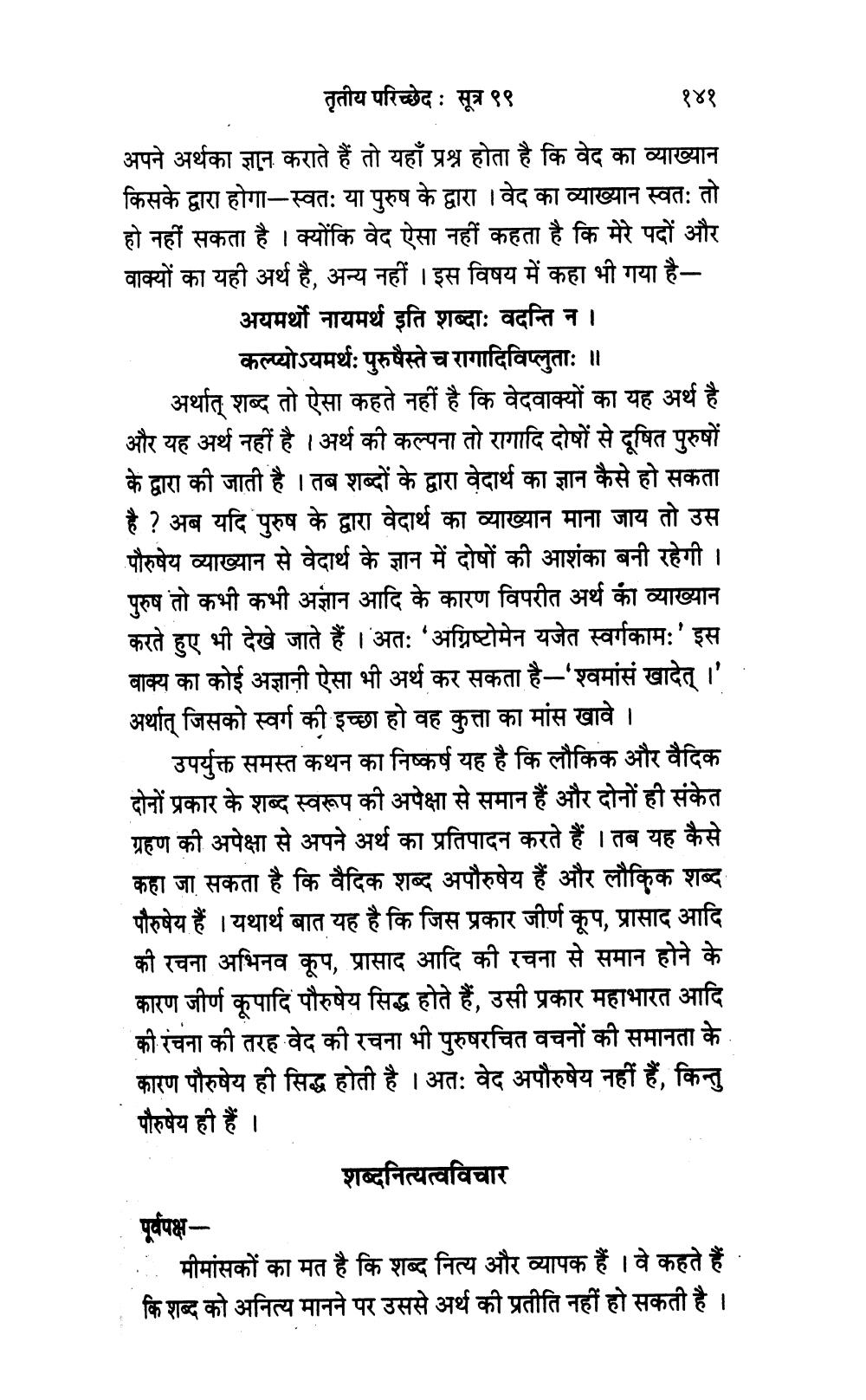________________
तृतीय परिच्छेद : सूत्र ९९
१४१ अपने अर्थका ज्ञान कराते हैं तो यहाँ प्रश्न होता है कि वेद का व्याख्यान किसके द्वारा होगा-स्वतः या पुरुष के द्वारा । वेद का व्याख्यान स्वतः तो हो नहीं सकता है । क्योंकि वेद ऐसा नहीं कहता है कि मेरे पदों और वाक्यों का यही अर्थ है, अन्य नहीं । इस विषय में कहा भी गया है
अयमर्थो नायमर्थ इति शब्दाः वदन्ति न ।
कल्प्योऽयमर्थः पुरुषैस्ते च रागादिविप्लुताः ॥ अर्थात् शब्द तो ऐसा कहते नहीं है कि वेदवाक्यों का यह अर्थ है और यह अर्थ नहीं है । अर्थ की कल्पना तो रागादि दोषों से दूषित पुरुषों के द्वारा की जाती है । तब शब्दों के द्वारा वेदार्थ का ज्ञान कैसे हो सकता है ? अब यदि पुरुष के द्वारा वेदार्थ का व्याख्यान माना जाय तो उस पौरुषेय व्याख्यान से वेदार्थ के ज्ञान में दोषों की आशंका बनी रहेगी। पुरुष तो कभी कभी अज्ञान आदि के कारण विपरीत अर्थ की व्याख्यान करते हुए भी देखे जाते हैं । अतः ‘अग्निष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः' इस वाक्य का कोई अज्ञानी ऐसा भी अर्थ कर सकता है-'श्वमांसं खादेत् ।' अर्थात् जिसको स्वर्ग की इच्छा हो वह कुत्ता का मांस खावे ।
उपर्युक्त समस्त कथन का निष्कर्ष यह है कि लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्द स्वरूप की अपेक्षा से समान हैं और दोनों ही संकेत ग्रहण की अपेक्षा से अपने अर्थ का प्रतिपादन करते हैं । तब यह कैसे कहा जा सकता है कि वैदिक शब्द अपौरुषेय हैं और लौकिक शब्द पौरुषेय हैं । यथार्थ बात यह है कि जिस प्रकार जीर्ण कूप, प्रासाद आदि की रचना अभिनव कूप, प्रासाद आदि की रचना से समान होने के कारण जीर्ण कूपादि पौरुषेय सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार महाभारत आदि की रचना की तरह वेद की रचना भी पुरुषरचित वचनों की समानता के कारण पौरुषेय ही सिद्ध होती है । अतः वेद अपौरुषेय नहीं हैं, किन्तु पौरुषेय ही हैं।
शब्दनित्यत्वविचार पूर्वपक्ष... मीमांसकों का मत है कि शब्द नित्य और व्यापक हैं । वे कहते हैं । कि शब्द को अनित्य मानने पर उससे अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है ।