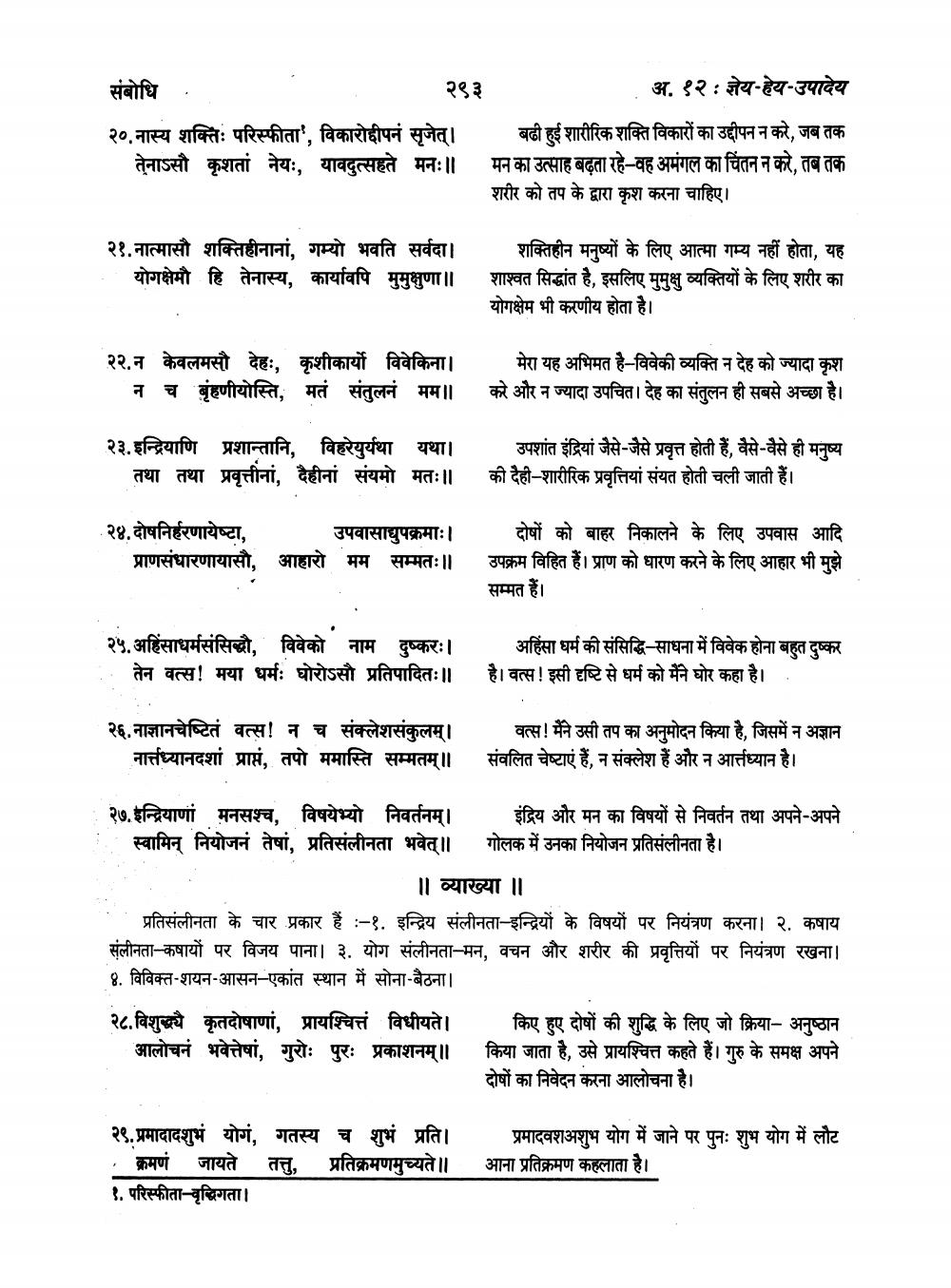________________
संबोधि
२९३
२०. नास्य शक्तिः परिस्फीता', विकारोद्दीपनं सृजेत् । तेनाऽसौ कृशतां नेयः, यावदुत्सहते मनः ॥
२१. नात्मासौ शक्तिहीनानां, गम्यो भवति सर्वदा । योगक्षेमौ हि तेनास्य, कार्यावपि मुमुक्षुणा ॥
२२. न केवलमसौ देहः, कृशीकार्यो न च बृंहणीयोस्ति, मतं संतुलनं
विवेकिना ।
मम ॥
यथा ।
२३. इन्द्रियाणि प्रशान्तानि विहरेयुर्यथा तथा तथा प्रवृत्तीनां, दैहीनां संयमो मतः ॥
२४. दोषनिर्हरणायेष्टा,
उपवासाद्युपक्रमाः । सम्मतः ॥
प्राणसंधारणायासौ, आहारो मम
२५. अहिंसाधर्मसंसिद्धौ, विवेको नाम तेन वत्स! मया धर्मः घोरोऽसौ प्रतिपादितः ॥
दुष्करः ।
२६. नाज्ञानचेष्टितं वत्स! न च संक्लेशसंकुलम् । नार्त्तध्यानदशां प्राप्तं तपो ममास्ति सम्मतम् ॥
२८. विशुद्ध्यै
कृतदोषाणां प्रायश्चित्तं विधीयते । आलोचनं भवेत्तेषां गुरोः पुरः प्रकाशनम् ॥
अ. १२ : ज्ञेय- हेय-उपादेय
बढी हुई शारीरिक शक्ति विकारों का उद्दीपन न करे, जब तक मन का उत्साह बढ़ता रहे-वह अमंगल का चिंतन न करे, तब तक शरीर को तप के द्वारा कृश करना चाहिए।
२९. प्रमादादशुभं योगं, गतस्य च शुभं प्रति । क्रमणं जायते प्रतिक्रमणमुच्यते ॥ १. परिस्फीता - वृद्धिगता ।
तत्तु,
शक्तिहीन मनुष्यों के लिए आत्मा गम्य नहीं होता, यह शाश्वत सिद्धांत है, इसलिए मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए शरीर का योगक्षेम भी करणीय होता है।
मेरा यह अभिमत है-विवेकी व्यक्ति न देह को ज्यादा कृश करे और न ज्यादा उपचित। देह का संतुलन ही सबसे अच्छा है।
उपशांत इंद्रियां जैसे-जैसे प्रवृत्त होती हैं, वैसे-वैसे ही मनुष्य की दैही-शारीरिक प्रवृत्तियां संयत होती चली जाती हैं।
दोषों को बाहर निकालने के लिए उपवास आदि उपक्रम विहित हैं । प्राण को धारण करने के लिए आहार भी मुझे सम्मत हैं।
अहिंसा धर्म की संसिद्धि-साधना में विवेक होना बहुत दुष्कर है । वत्स ! इसी दृष्टि से धर्म को मैंने घोर कहा है।
२७. इन्द्रियाणां मनसश्च विषयेभ्यो निवर्तनम् । स्वामिन् नियोजनं तेषां प्रतिसंलीनता भवेत् ॥ ॥ व्याख्या ॥
प्रतिसंलीनता के चार प्रकार हैं :-१. इन्द्रिय संलीनता - इन्द्रियों के विषयों पर नियंत्रण करना। २. कषाय संलीनता - कषायों पर विजय पाना । ३. योग संलीनता - मन, वचन और शरीर की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना । 8. विविक्त शयन आसन- एकांत स्थान में सोना-बैठना ।
वत्स! मैंने उसी तप का अनुमोदन किया है, जिसमें न अज्ञान संवलित चेष्टाएं हैं, न संक्लेश हैं और न आर्त्तध्यान है।
इंद्रिय और मन का विषयों से निवर्तन तथा अपने-अपने गोलक में उनका नियोजन प्रतिसंलीनता है।
किए हुए दोषों की शुद्धि के लिए जो क्रिया- अनुष्ठान किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना आलोचना है।
प्रमादवशअशुभ योग में जाने पर पुनः शुभ योग में लौट आना प्रतिक्रमण कहलाता है।