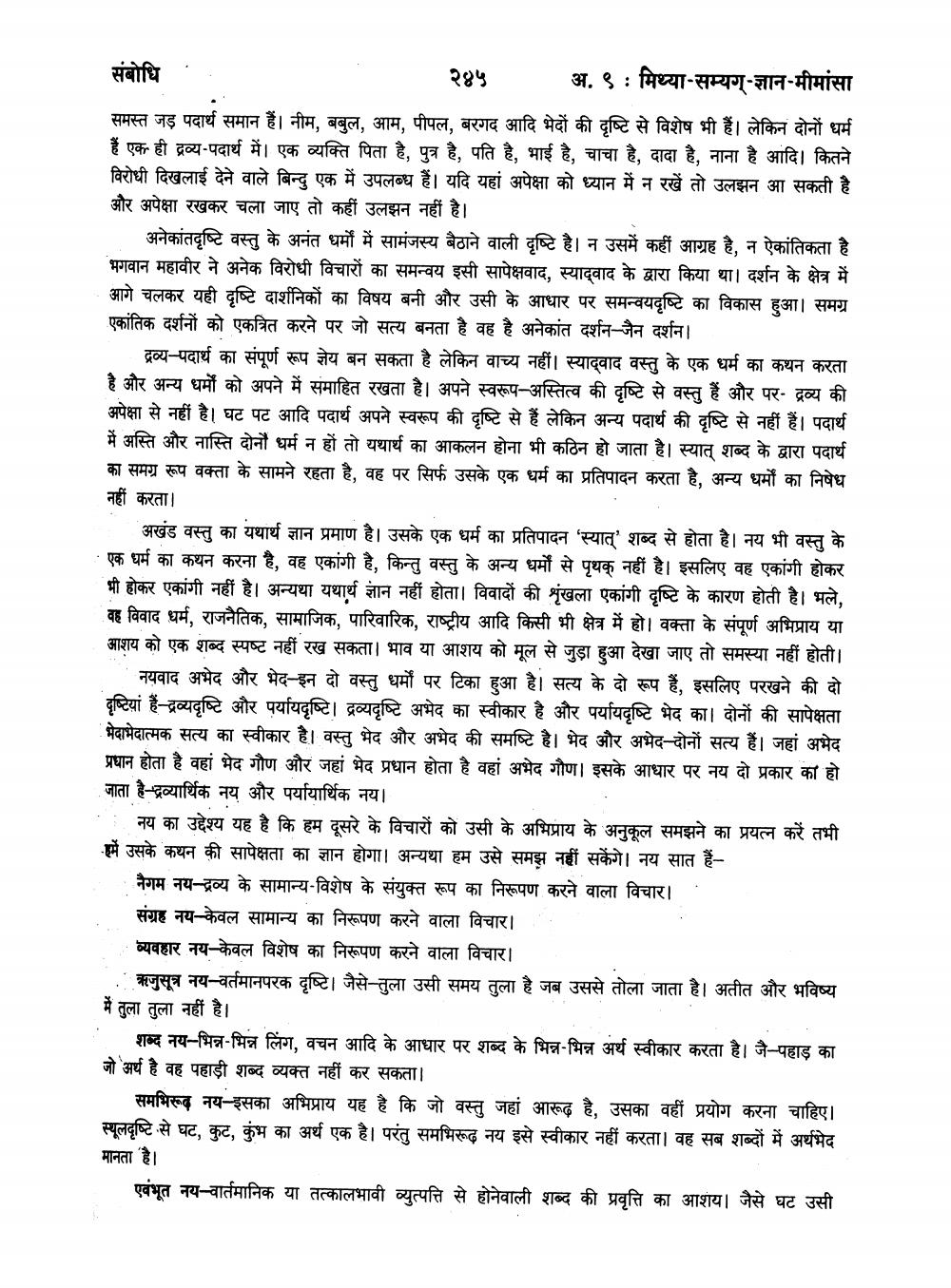________________
संबोधि -
२४५
अ. ९ : मिथ्या-सम्यग्-ज्ञान-मीमांसा
समस्त जड़ पदार्थ समान हैं। नीम, बबुल, आम, पीपल, बरगद आदि भेदों की दृष्टि से विशेष भी हैं। लेकिन दोनों धर्म हैं एक ही द्रव्य-पदार्थ में। एक व्यक्ति पिता है, पुत्र है, पति है, भाई है, चाचा है, दादा है, नाना है आदि। कितने विरोधी दिखलाई देने वाले बिन्दु एक में उपलब्ध हैं। यदि यहां अपेक्षा को ध्यान में न रखें तो उलझन आ सकती है और अपेक्षा रखकर चला जाए तो कहीं उलझन नहीं है।
अनेकांतदृष्टि वस्तु के अनंत धर्मों में सामंजस्य बैठाने वाली दृष्टि है। न उसमें कहीं आग्रह है, न ऐकांतिकता है भगवान महावीर ने अनेक विरोधी विचारों का समन्वय इसी सापेक्षवाद, स्याद्वाद के द्वारा किया था। दर्शन के क्षेत्र में आगे चलकर यही दृष्टि दार्शनिकों का विषय बनी और उसी के आधार पर समन्वयदृष्टि का विकास हुआ। समग्र एकांतिक दर्शनों को एकत्रित करने पर जो सत्य बनता है वह है अनेकांत दर्शन-जैन दर्शन।
द्रव्य-पदार्थ का संपूर्ण रूप ज्ञेय बन सकता है लेकिन वाच्य नहीं। स्याद्वाद वस्तु के एक धर्म का कथन करता है और अन्य धर्मों को अपने में समाहित रखता है। अपने स्वरूप-अस्तित्व की दृष्टि से वस्तु हैं और पर- द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है। घट पट आदि पदार्थ अपने स्वरूप की दृष्टि से हैं लेकिन अन्य पदार्थ की दृष्टि से नहीं हैं। पदार्थ में अस्ति और नास्ति दोनों धर्म न हों तो यथार्थ का आकलन होना भी कठिन हो जाता है। स्यात् शब्द के द्वारा पदार्थ का समग्र रूप वक्ता के सामने रहता है, वह पर सिर्फ उसके एक धर्म का प्रतिपादन करता है, अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता।
अखंड वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्रमाण है। उसके एक धर्म का प्रतिपादन 'स्यात्' शब्द से होता है। नय भी वस्तु के - एक धर्म का कथन करना है, वह एकांगी है, किन्तु वस्तु के अन्य धर्मों से पृथक् नहीं है। इसलिए वह एकांगी होकर भी होकर एकांगी नहीं है। अन्यथा यथार्थ ज्ञान नहीं होता। विवादों की श्रृंखला एकांगी दृष्टि के कारण होती है। भले, वह विवाद धर्म, राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय आदि किसी भी क्षेत्र में हो। वक्ता के संपूर्ण अभिप्राय या आशय को एक शब्द स्पष्ट नहीं रख सकता। भाव या आशय को मूल से जुड़ा हुआ देखा जाए तो समस्या नहीं होती।
'नयवाद अभेद और भेद-इन दो वस्तु धर्मों पर टिका हुआ है। सत्य के दो रूप हैं, इसलिए परखने की दो दृष्टियां हैं-द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि। द्रव्यदृष्टि अभेद का स्वीकार है और पर्यायदृष्टि भेद का। दोनों की सापेक्षता भेदाभेदात्मक सत्य का स्वीकार है। वस्तु भेद और अभेद की समष्टि है। भेद और अभेद-दोनों सत्य हैं। जहां अभेद प्रधान होता है वहां भेद गौण और जहां भेद प्रधान होता है वहां अभेद गौण। इसके आधार पर नय दो प्रकार का हो जाता है-'द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय।
नय का उद्देश्य यह है कि हम दूसरे के विचारों को उसी के अभिप्राय के अनुकूल समझने का प्रयत्न करें तभी -हमें उसके कथन की सापेक्षता का ज्ञान होगा। अन्यथा हम उसे समझ नहीं सकेंगे। नय सात हैं
नैगम नय-द्रव्य के सामान्य-विशेष के संयुक्त रूप का निरूपण करने वाला विचार। संग्रह नय-केवल सामान्य का निरूपण करने वाला विचार। व्यवहार नय-केवल विशेष का निरूपण करने वाला विचार।
ऋजुसूत्र नय-वर्तमानपरक दृष्टि। जैसे-तुला उसी समय तुला है जब उससे तोला जाता है। अतीत और भविष्य में तुला तुला नहीं है।
शब्द नय-भिन्न-भिन्न लिंग, वचन आदि के आधार पर शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। जै-पहाड़ का जो अर्थ है वह पहाड़ी शब्द व्यक्त नहीं कर सकता।
समभिरूद नय-इसका अभिप्राय यह है कि जो वस्तु जहां आरूढ़ है, उसका वहीं प्रयोग करना चाहिए। स्थूलदृष्टि से घट, कुट, कुंभ का अर्थ एक है। परंतु समभिरूढ़ नय इसे स्वीकार नहीं करता। वह सब शब्दों में अर्थभेद मानता है।
एवंभूत नय-वार्तमानिक या तत्कालभावी व्युत्पत्ति से होनेवाली शब्द की प्रवृत्ति का आशय। जैसे घट उसी