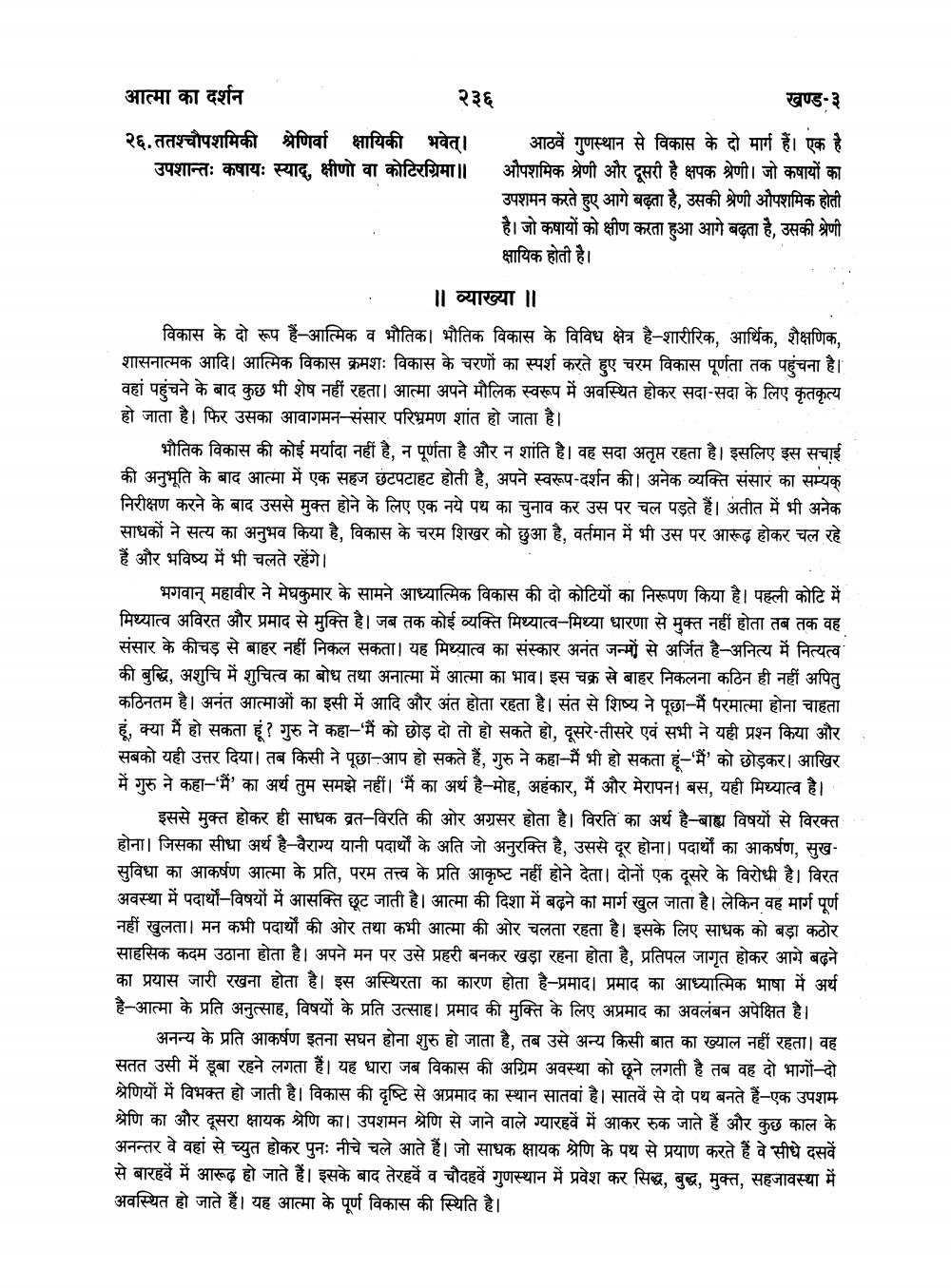________________
आत्मा का दर्शन
२३६
२६. ततश्चौपशमिकी श्रेणिर्वा क्षायिकी भवेत् । उपशान्तः कषायः स्याद्, क्षीणो वा कोटिरग्रिमा ।।
खण्ड - ३
है
आठवें गुणस्थान से विकास के दो मार्ग है। एक औपशमिक श्रेणी और दूसरी है क्षपक श्रेणी। जो कषायों का उपशमन करते हुए आगे बढ़ता है, उसकी श्रेणी औपशमिक होती है जो कषायों को क्षीण करता हुआ आगे बढ़ता है, उसकी श्रेणी क्षायिक होती है।
॥ व्याख्या ||
विकास के दो रूप हैं- आत्मिक व भौतिक । भौतिक विकास के विविध क्षेत्र है- शारीरिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शासनात्मक आदि। आत्मिक विकास क्रमशः विकास के चरणों का स्पर्श करते हुए चरम विकास पूर्णता तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। आत्मा अपने मौलिक स्वरूप में अवस्थित होकर सदा-सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है फिर उसका आवागमन - संसार परिभ्रमण शांत हो जाता है।
भौतिक विकास की कोई मर्यादा नहीं है, न पूर्णता है और न शांति है वह सदा अतृप्त रहता है इसलिए इस सचाई की अनुभूति के बाद आत्मा में एक सहज छटपटाहट होती है, अपने स्वरूप-दर्शन की। अनेक व्यक्ति संसार का सम्यक् निरीक्षण करने के बाद उससे मुक्त होने के लिए एक नये पथ का चुनाव कर उस पर चल पड़ते हैं। अतीत में भी अनेक साधकों ने सत्य का अनुभव किया है, विकास के चरम शिखर को छुआ है, वर्तमान में भी उस पर आरूढ़ होकर चल रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे।
।
भगवान् महावीर ने मेघकुमार के सामने आध्यात्मिक विकास की दो कोटियों का निरूपण किया है। पहली कोटि में मिथ्यात्व अविरत और प्रमाद से मुक्ति है जब तक कोई व्यक्ति मिथ्यात्व मिथ्या धारणा से मुक्त नहीं होता तब तक वह संसार के कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता। यह मिथ्यात्व का संस्कार अनंत जन्मों से अर्जित है-अनित्य में नित्यत्व की बुद्धि, अशुचि में शुचित्व का बोध तथा अनात्मा में आत्मा का भाव। इस चक्र से बाहर निकलना कठिन ही नहीं अपितु कठिनतम है। अनंत आत्माओं का इसी में आदि और अंत होता रहता है। संत से शिष्य ने पूछा- मैं परमात्मा होना चाहता हूं, क्या मैं हो सकता हूं? गुरु ने कहा- 'मैं को छोड़ दो तो हो सकते हो, दूसरे-तीसरे एवं सभी ने यही प्रश्न किया और सबको यही उत्तर दिया। तब किसी ने पूछा- आप हो सकते हैं, गुरु ने कहा- मैं भी हो सकता हूं-'मैं' को छोड़कर । आखिर में गुरु ने कहा- 'मैं' का अर्थ तुम समझे नहीं। 'मैं का अर्थ है - मोह, अहंकार, मैं और मेरापन 1 बस, यही मिथ्यात्व है। इससे मुक्त होकर ही साधक व्रत-विरति की ओर अग्रसर होता है विरति का अर्थ है-बाह्य विषयों से विरक्त होना। जिसका सीधा अर्थ है - वैराग्य यानी पदार्थों के अति जो अनुरक्ति है, उससे दूर होना। पदार्थों का आकर्षण, सुखसुविधा का आकर्षण आत्मा के प्रति, परम तत्त्व के प्रति आकृष्ट नहीं होने देता। दोनों एक दूसरे के विरोधी है। विरत अवस्था में पदार्थों विषयों में आसक्ति छूट जाती है आत्मा की दिशा में बढ़ने का मार्ग खुल जाता है। लेकिन वह मार्ग पूर्ण नहीं खुलता। मन कभी पदार्थों की ओर तथा कभी आत्मा की ओर चलता रहता है। इसके लिए साधक को बड़ा कठोर साहसिक कदम उठाना होता है। अपने मन पर उसे प्रहरी बनकर खड़ा रहना होता है, प्रतिपल जागृत होकर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखना होता है। इस अस्थिरता का कारण होता है-प्रमाद। प्रमाद का आध्यात्मिक भाषा में अर्थ है - आत्मा के प्रति अनुत्साह, विषयों के प्रति उत्साह । प्रमाद की मुक्ति के लिए अप्रमाद का अवलंबन अपेक्षित है।
अनन्य के प्रति आकर्षण इतना सघन होना शुरू हो जाता है, तब उसे अन्य किसी बात का ख्याल नहीं रहता। वह सतत उसी में डूबा रहने लगता है। यह धारा जब विकास की अग्रिम अवस्था को छूने लगती है तब वह दो भागों-दो श्रेणियों में विभक्त हो जाती है। विकास की दृष्टि से अप्रमाद का स्थान सातवां है। सातवें से दो पथ बनते हैं - एक उपशम श्रेणि का और दूसरा क्षायक श्रेणि का। उपशमन श्रेणि से जाने वाले ग्यारहवें में आकर रुक जाते हैं और कुछ काल के अनन्तर वे वहां से च्युत होकर पुनः नीचे चले आते हैं। जो साधक क्षायक श्रेणि के पथ से प्रयाण करते हैं वे सीधे दसवें से बारहवें में आरूढ़ हो जाते हैं। इसके बाद तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान में प्रवेश कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, सहजावस्था में अवस्थित हो जाते हैं। यह आत्मा के पूर्ण विकास की स्थिति है।