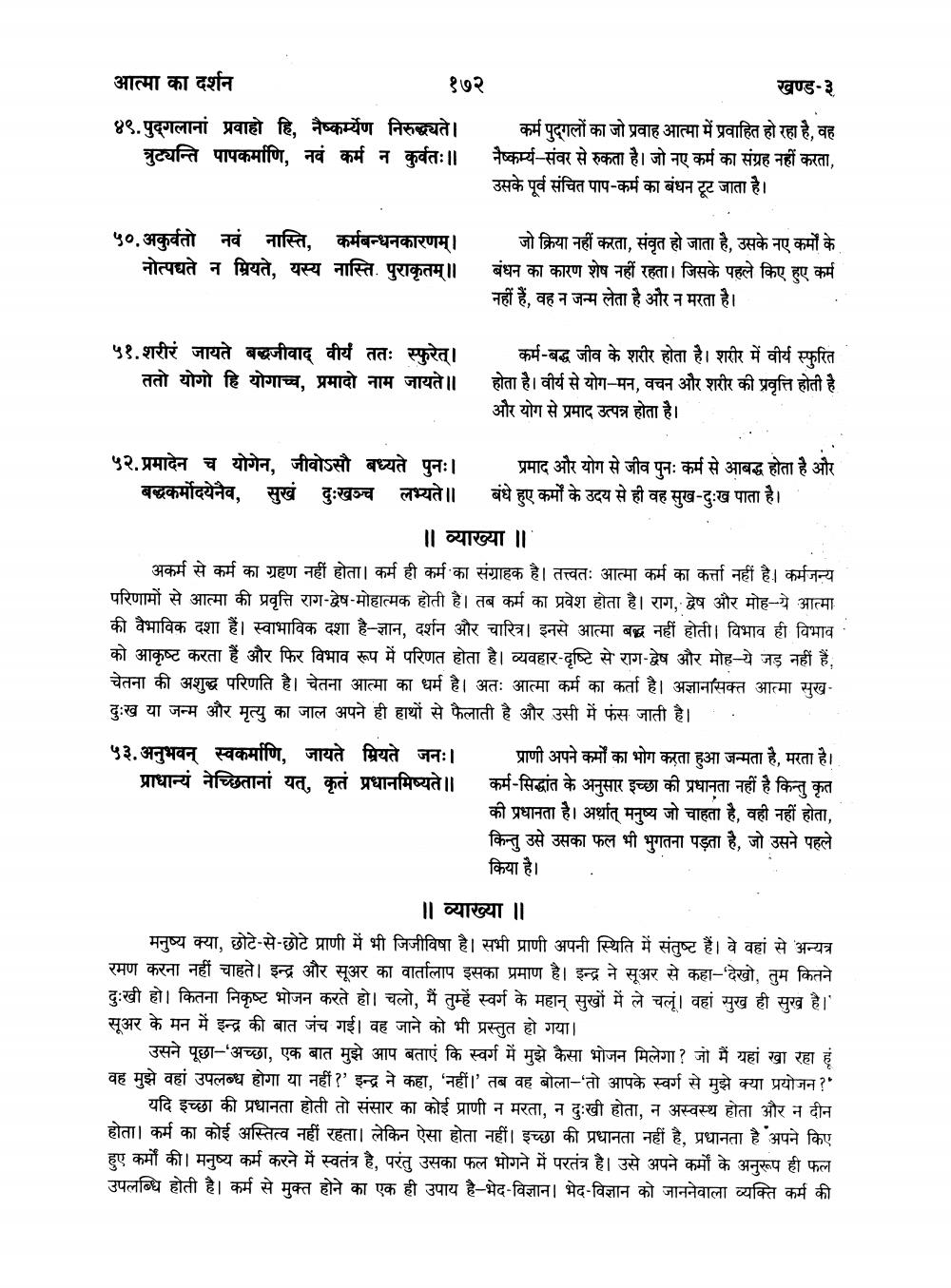________________
आत्मा का दर्शन
१७२
खण्ड-३
४९.पुद्गलानां प्रवाहो हि, नैष्कर्येण निरुक्ष्यते।
त्रुट्यन्ति पापकर्माणि, नवं कर्म न कुर्वतः॥
कर्म पदगलों का जो प्रवाह आत्मा में प्रवाहित हो रहा है, वह नैष्कर्म्य-संवर से रुकता है। जो नए कर्म का संग्रह नहीं करता, उसके पूर्व संचित पाप-कर्म का बंधन टूट जाता है।
५०.अकुर्वतो नवं नास्ति, कर्मबन्धनकारणम्।
नोत्पद्यते न म्रियते, यस्य नास्ति. पुराकृतम्॥
जो क्रिया नहीं करता, संवृत हो जाता है, उसके नए कर्मों के बंधन का कारण शेष नहीं रहता। जिसके पहले किए हुए कर्म नहीं हैं, वह न जन्म लेता है और न मरता है।
५१.शरीरं जायते बद्धजीवाद् वीर्य ततः स्फुरेत्।
ततो योगो हि योगाच्च, प्रमादो नाम जायते॥
कर्म-बद्ध जीव के शरीर होता है। शरीर में वीर्य स्फुरित होता है। वीर्य से योग-मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति होती है और योग से प्रमाद उत्पन्न होता है।
५२. प्रमादेन च योगेन, जीवोऽसौ बध्यते पुनः।
बद्धकर्मोदयेनैव, सुखं दुःखञ्च लभ्यते॥
प्रमाद और योग से जीव पुनः कर्म से आबद्ध होता है और बंधे हुए कर्मों के उदय से ही वह सुख-दुःख पाता है।
॥ व्याख्या ॥ अकर्म से कर्म का ग्रहण नहीं होता। कर्म ही कर्म का संग्राहक है। तत्त्वतः आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। कर्मजन्य परिणामों से आत्मा की प्रवृत्ति राग-द्वेष-मोहात्मक होती है। तब कर्म का प्रवेश होता है। राग, द्वेष और मोह-ये आत्मा की वैभाविक दशा हैं। स्वाभाविक दशा है-ज्ञान, दर्शन और चारित्र। इनसे आत्मा बद्ध नहीं होती। विभाव ही विभाव को आकृष्ट करता हैं और फिर विभाव रूप में परिणत होता है। व्यवहार-दृष्टि से राग-द्वेष और मोह-ये जड़ नहीं हैं, चेतना की अशुद्ध परिणति है। चेतना आत्मा का धर्म है। अतः आत्मा कर्म का कर्ता है। अज्ञानसिक्त आत्मा सुखदुःख या जन्म और मृत्यु का जाल अपने ही हाथों से फैलाती है और उसी में फंस जाती है। ५३. अनुभवन् स्वकर्माणि, जायते म्रियते जनः। प्राणी अपने कर्मों का भोग करता हआ जन्मता है, मरता है। प्राधान्यं नेच्छितानां यत्, कृतं प्रधानमिष्यते॥ कर्म-सिद्धांत के अनुसार इच्छा की प्रधानता नहीं है किन्तु कृत
की प्रधानता है। अर्थात् मनुष्य जो चाहता है, वही नहीं होता, किन्तु उसे उसका फल भी भुगतना पड़ता है, जो उसने पहले किया है।
॥ व्याख्या ॥ मनुष्य क्या, छोटे-से-छोटे प्राणी में भी जिजीविषा है। सभी प्राणी अपनी स्थिति में संतुष्ट हैं। वे वहां से 'अन्यत्र रमण करना नहीं चाहते। इन्द्र और सूअर का वार्तालाप इसका प्रमाण है। इन्द्र ने सूअर से कहा-'देखो, तुम कितने दुःखी हो। कितना निकृष्ट भोजन करते हो। चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग के महान् सुखों में ले चलूं। वहां सुख ही सुख है।' सूअर के मन में इन्द्र की बात जंच गई। वह जाने को भी प्रस्तुत हो गया।
उसने पूछा-'अच्छा, एक बात मुझे आप बताएं कि स्वर्ग में मुझे कैसा भोजन मिलेगा? जो मैं यहां खा रहा हूं वह मुझे वहां उपलब्ध होगा या नहीं?' इन्द्र ने कहा, 'नहीं।' तब वह बोला-'तो आपके स्वर्ग से मुझे क्या प्रयोजन ?'
यदि इच्छा की प्रधानता होती तो संसार का कोई प्राणी न मरता, न दुःखी होता, न अस्वस्थ होता और न दीन होता। कर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन ऐसा होता नहीं। इच्छा की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है अपने किए हुए कर्मों की। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु उसका फल भोगने में परतंत्र है। उसे अपने कर्मों के अनुरूप ही फल उपलब्धि होती है। कर्म से मुक्त होने का एक ही उपाय है-भेद-विज्ञान। भेद-विज्ञान को जाननेवाला व्यक्ति कर्म की