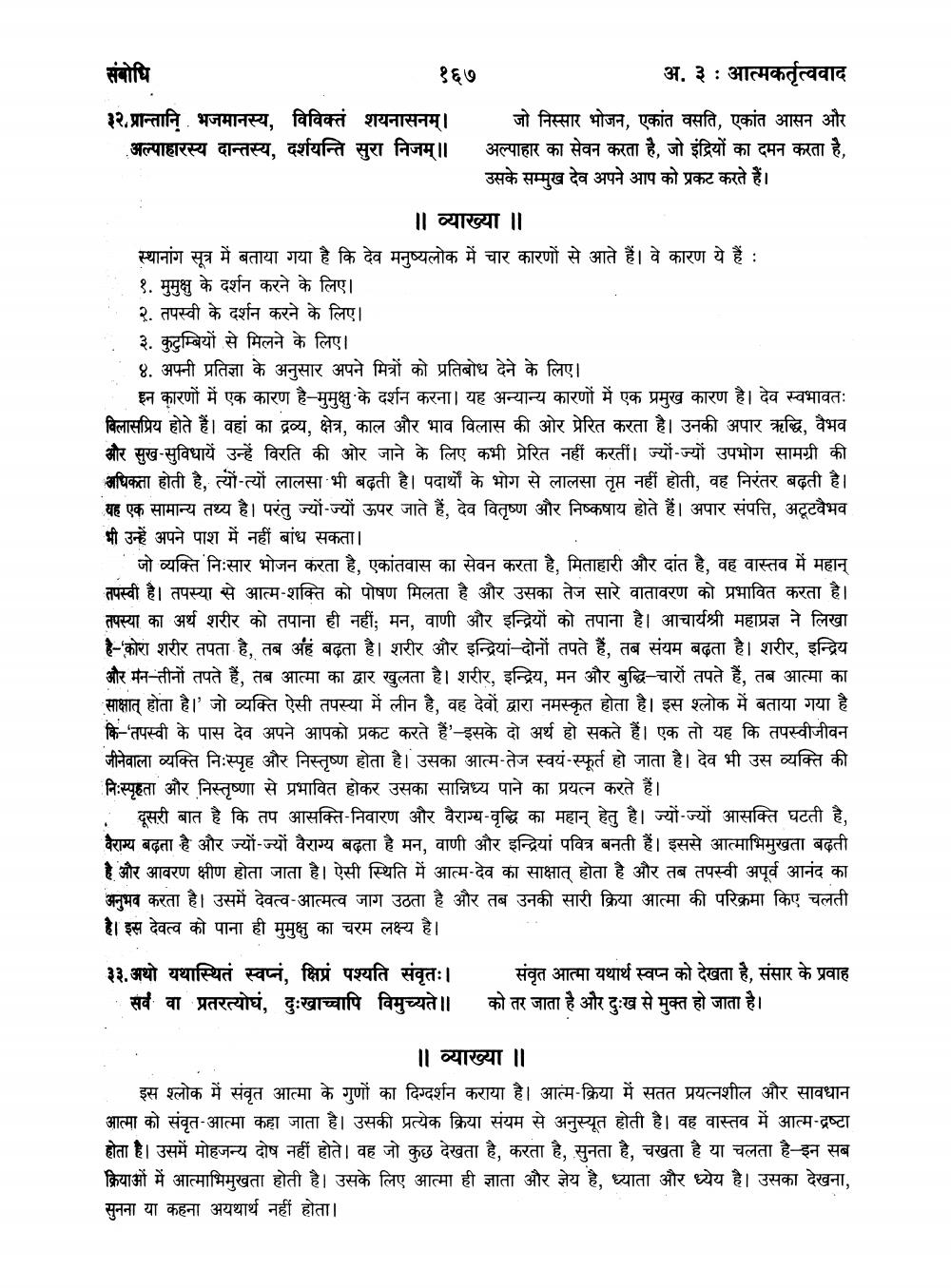________________
संबोधि
१६७
अ. ३ : आत्मकर्तृत्ववाद ३२.प्रान्तानि भजमानस्य, विविक्तं शयनासनम्। जो निस्सार भोजन, एकांत वसति, एकांत आसन और अल्पाहारस्य दान्तस्य, दर्शयन्ति सुरा निजम्॥ अल्पाहार का सेवन करता है, जो इंद्रियों का दमन करता है,
उसके सम्मुख देव अपने आप को प्रकट करते हैं।
॥ व्याख्या ॥ स्थानांग सूत्र में बताया गया है कि देव मनुष्यलोक में चार कारणों से आते हैं। वे कारण ये हैं : १. मुमुक्षु के दर्शन करने के लिए। २. तपस्वी के दर्शन करने के लिए। ३. कुटुम्बियों से मिलने के लिए। ४. अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने मित्रों को प्रतिबोध देने के लिए।
इन कारणों में एक कारण है-मुमुक्षु के दर्शन करना। यह अन्यान्य कारणों में एक प्रमुख कारण है। देव स्वभावतः विलासप्रिय होते हैं। वहां का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव विलास की ओर प्रेरित करता है। उनकी अपार ऋद्धि, वैभव
और सुख-सुविधायें उन्हें विरति की ओर जाने के लिए कभी प्रेरित नहीं करतीं। ज्यों-ज्यों उपभोग सामग्री की अधिकता होती है, त्यों-त्यों लालसा भी बढ़ती है। पदार्थों के भोग से लालसा तृप्त नहीं होती, वह निरंतर बढ़ती है। यह एक सामान्य तथ्य है। परंतु ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं, देव वितृष्ण और निष्कषाय होते हैं। अपार संपत्ति, अटूटवैभव भी उन्हें अपने पाश में नहीं बांध सकता।
जो व्यक्ति निःसार भोजन करता है, एकांतवास का सेवन करता है, मिताहारी और दांत है, वह वास्तव में महान् तपस्वी है। तपस्या से आत्म-शक्ति को पोषण मिलता है और उसका तेज सारे वातावरण को प्रभावित करता है। तपस्या का अर्थ शरीर को तपाना ही नहीं, मन, वाणी और इन्द्रियों को तपाना है। आचार्यश्री महाप्रज्ञ ने लिखा है-कोरा शरीर तपता है, तब अंहं बढ़ता है। शरीर और इन्द्रियां-दोनों तपते हैं, तब संयम बढ़ता है। शरीर, इन्द्रिय और मन-तीनों तपते हैं, तब आत्मा का द्वार खुलता है। शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि-चारों तपते हैं, तब आत्मा का साक्षात् होता है। जो व्यक्ति ऐसी तपस्या में लीन है, वह देवों द्वारा नमस्कृत होता है। इस श्लोक में बताया गया है कि-'तपस्वी के पास देव अपने आपको प्रकट करते हैं'-इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह कि तपस्वीजीवन जीनेवाला व्यक्ति निःस्पृह और निस्तृष्ण होता है। उसका आत्म-तेज स्वयं-स्फूर्त हो जाता है। देव भी उस व्यक्ति की निःस्पृहता और निस्तृष्णा से प्रभावित होकर उसका सान्निध्य पाने का प्रयत्न करते हैं। । दूसरी बात है कि तप आसक्ति-निवारण और वैराग्य-वृद्धि का महान् हेतु है। ज्यों-ज्यों आसक्ति घटती है, वैराग्य बढ़ता है और ज्यों-ज्यों वैराग्य बढ़ता है मन, वाणी और इन्द्रियां पवित्र बनती हैं। इससे आत्माभिमुखता बढ़ती है और आवरण क्षीण होता जाता है। ऐसी स्थिति में आत्म-देव का साक्षात् होता है और तब तपस्वी अपूर्व आनंद का अनुभव करता है। उसमें देवत्व-आत्मत्व जाग उठता है और तब उनकी सारी क्रिया आत्मा की परिक्रमा किए चलती है। इस देवत्व को पाना ही मुमुक्ष का चरम लक्ष्य है।
३३. अथो यथास्थितं स्वप्नं, क्षिप्रं पश्यति संवृतः। - सर्व वा प्रतरत्योघं, दुःखाच्चापि विमुच्यते॥
संवृत आत्मा यथार्थ स्वप्न को देखता है, संसार के प्रवाह को तर जाता है और दुःख से मुक्त हो जाता है।
॥ व्याख्या ॥ _इस श्लोक में संवृत आत्मा के गुणों का दिग्दर्शन कराया है। आत्म-क्रिया में सतत प्रयत्नशील और सावधान आत्मा को संवृत-आत्मा कहा जाता है। उसकी प्रत्येक क्रिया संयम से अनुस्यूत होती है। वह वास्तव में आत्म-द्रष्टा होता है। उसमें मोहजन्य दोष नहीं होते। वह जो कुछ देखता है, करता है, सुनता है, चखता है या चलता है-इन सब क्रियाओं में आत्माभिमुखता होती है। उसके लिए आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञेय है, ध्याता और ध्येय है। उसका देखना, सुनना या कहना अयथार्थ नहीं होता।