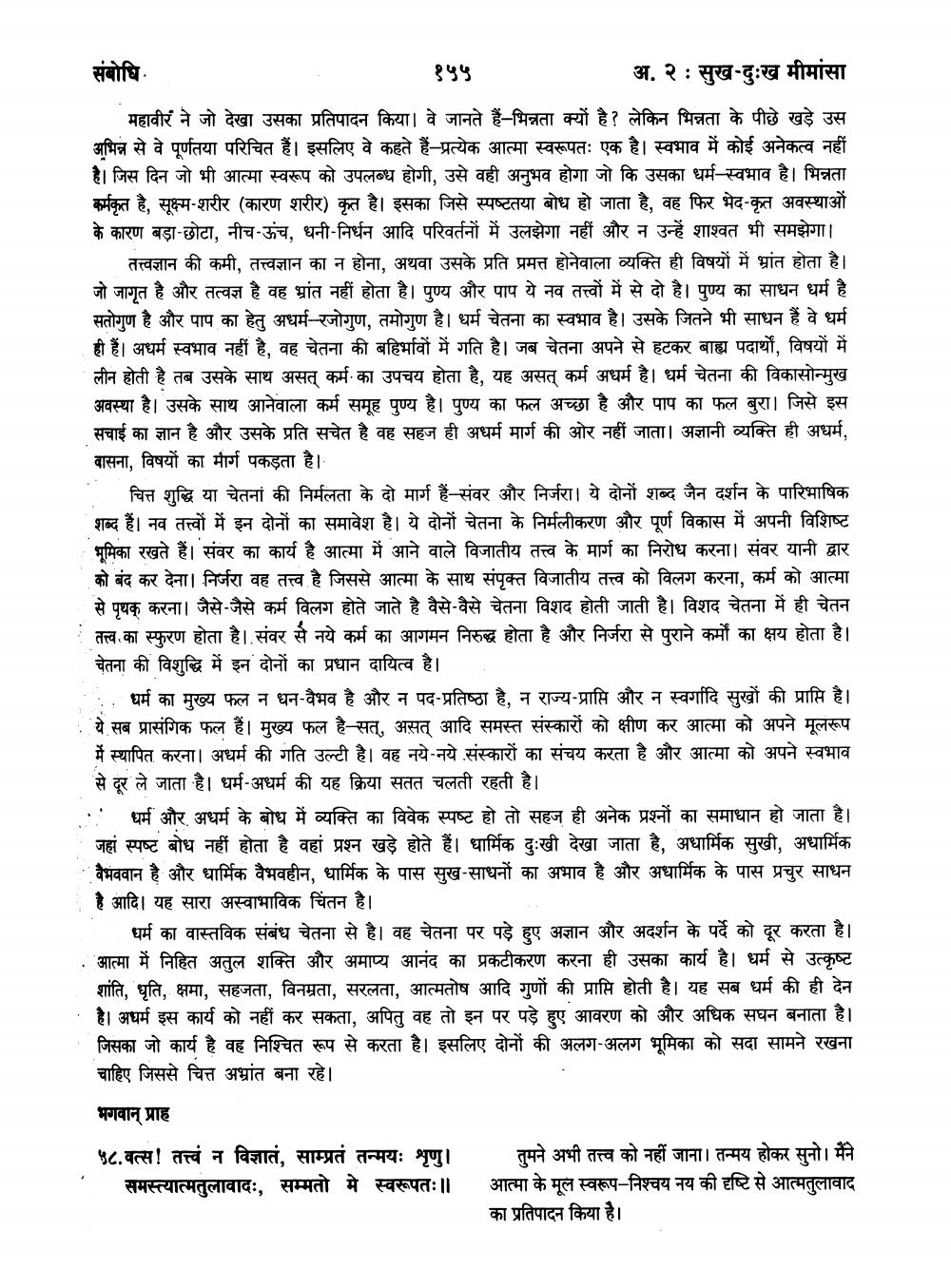________________
संबोधि.
१५५
अ. २ : सुख-दुःख मीमांसा
___ महावीर ने जो देखा उसका प्रतिपादन किया। वे जानते हैं-भिन्नता क्यों है? लेकिन भिन्नता के पीछे खड़े उस अभिन्न से वे पूर्णतया परिचित हैं। इसलिए वे कहते हैं-प्रत्येक आत्मा स्वरूपतः एक है। स्वभाव में कोई अनेकत्व नहीं है। जिस दिन जो भी आत्मा स्वरूप को उपलब्ध होगी, उसे वही अनुभव होगा जो कि उसका धर्म-स्वभाव है। भिन्नता कर्मकृत है, सूक्ष्म-शरीर (कारण शरीर) कृत है। इसका जिसे स्पष्टतया बोध हो जाता है, वह फिर भेद-कृत अवस्थाओं के कारण बड़ा-छोटा, नीच-ऊंच, धनी-निर्धन आदि परिवर्तनों में उलझेगा नहीं और न उन्हें शाश्वत भी समझेगा।
तत्त्वज्ञान की कमी, तत्त्वज्ञान का न होना, अथवा उसके प्रति प्रमत्त होनेवाला व्यक्ति ही विषयों में भ्रांत होता है। जो जागृत है और तत्वज्ञ है वह भ्रांत नहीं होता है। पुण्य और पाप ये नव तत्त्वों में से दो है। पुण्य का साधन धर्म है सतोगुण है और पाप का हेतु अधर्म-रजोगुण, तमोगुण है। धर्म चेतना का स्वभाव है। उसके जितने भी साधन हैं वे धर्म ही हैं। अधर्म स्वभाव नहीं है, वह चेतना की बहिर्भावों में गति है। जब चेतना अपने से हटकर बाह्य पदार्थों, विषयों में लीन होती है तब उसके साथ असत् कर्म का उपचय होता है, यह असत् कर्म अधर्म है। धर्म चेतना की विकासोन्मुख अवस्था है। उसके साथ आनेवाला कर्म समूह पुण्य है। पुण्य का फल अच्छा है और पाप का फल बुरा। जिसे इस सचाई का ज्ञान है और उसके प्रति सचेत है वह सहज ही अधर्म मार्ग की ओर नहीं जाता। अज्ञानी व्यक्ति ही अधर्म, वासना, विषयों का मार्ग पकड़ता है।
चित्त शुद्धि या चेतना की निर्मलता के दो मार्ग हैं-संवर और निर्जरा। ये दोनों शब्द जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्द हैं। नव तत्त्वों में इन दोनों का समावेश है। ये दोनों चेतना के निर्मलीकरण और पूर्ण विकास में अपनी विशिष्ट भूमिका रखते हैं। संवर का कार्य है आत्मा में आने वाले विजातीय तत्त्व के मार्ग का निरोध करना। संवर यानी द्वार को बंद कर देना। निर्जरा वह तत्त्व है जिससे आत्मा के साथ संपृक्त विजातीय तत्त्व को विलग करना, कर्म को आत्मा से पृथक् करना। जैसे-जैसे कर्म विलग होते जाते है वैसे-वैसे चेतना विशद होती जाती है। विशद चेतना में ही चेतन तत्त्व का स्फुरण होता है। संवर से नये कर्म का आगमन निरुद्ध होता है और निर्जरा से पुराने कर्मों का क्षय होता है। चेतना की विशुद्धि में इन दोनों का प्रधान दायित्व है। ., धर्म का मुख्य फल न धन-वैभव है और न पद-प्रतिष्ठा है, न राज्य-प्राप्ति और न स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति है। ये सब प्रासंगिक फल हैं। मुख्य फल है-सत्, असत् आदि समस्त संस्कारों को क्षीण कर आत्मा को अपने मूलरूप में स्थापित करना। अधर्म की गति उल्टी है। वह नये-नये संस्कारों का संचय करता है और आत्मा को अपने स्वभाव
से दूर ले जाता है। धर्म-अधर्म की यह क्रिया सतत चलती रहती है। • धर्म और अधर्म के बोध में व्यक्ति का विवेक स्पष्ट हो तो सहज ही अनेक प्रश्नों का समाधान हो जाता है।
जा स्पष्ट बोध नहीं होता है वहां प्रश्न खड़े होते हैं। धार्मिक दुःखी देखा जाता है, अधार्मिक सुखी, अधार्मिक वैभववान है और धार्मिक वैभवहीन, धार्मिक के पास सुख-साधनों का अभाव है और अधार्मिक के पास प्रचुर साधन है आदि। यह सारा अस्वाभाविक चिंतन है।
धर्म का वास्तविक संबंध चेतना से है। वह चेतना पर पड़े हुए अज्ञान और अदर्शन के पर्दे को दूर करता है। . आत्मा में निहित अतुल शक्ति और अमाप्य आनंद का प्रकटीकरण करना ही उसका कार्य है। धर्म से उत्कृष्ट
शांति, धृति, क्षमा, सहजता, विनम्रता, सरलता, आत्मतोष आदि गुणों की प्राप्ति होती है। यह सब धर्म की ही देन है। अधर्म इस कार्य को नहीं कर सकता, अपितु वह तो इन पर पड़े हुए आवरण को और अधिक सघन बनाता है। जिसका जो कार्य है वह निश्चित रूप से करता है। इसलिए दोनों की अलग-अलग भूमिका को सदा सामने रखना चाहिए जिससे चित्त अभ्रांत बना रहे।
भगवान् प्राह
५८.वत्स! तत्त्वं न विज्ञातं, साम्प्रतं तन्मयः शृणु।
समस्त्यात्मतुलावादः, सम्मतो मे स्वरूपतः॥
तुमने अभी तत्त्व को नहीं जाना। तन्मय होकर सुनो। मैंने आत्मा के मूल स्वरूप-निश्चय नय की दृष्टि से आत्मतुलावाद का प्रतिपादन किया है।