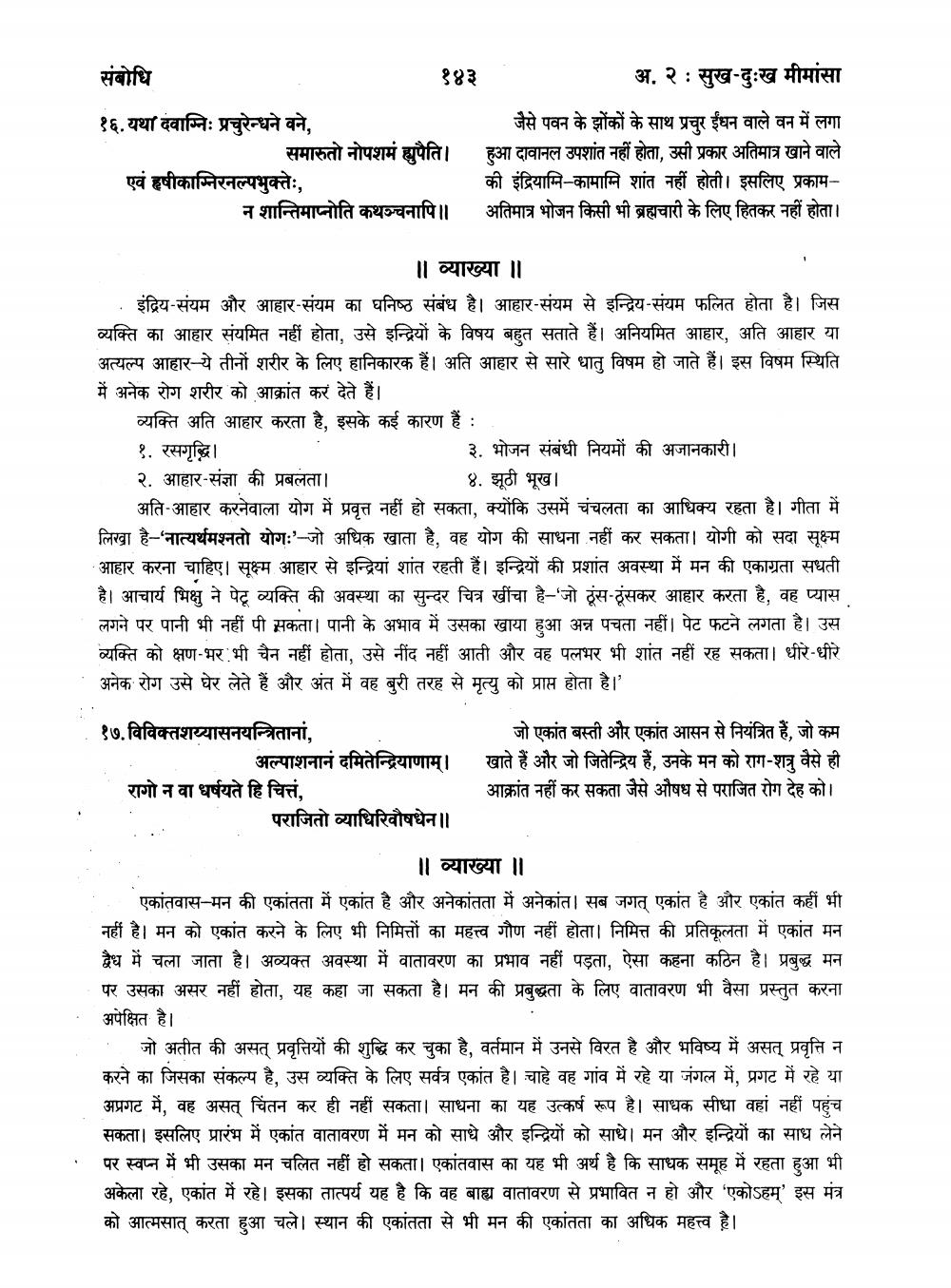________________
संबोधि
१४३
अ. २ : सुख-दुःख मीमांसा १६. यथा दवाग्निः प्रचुरेन्धने वने,
जैसे पवन के झोंकों के साथ प्रचुर ईंधन वाले वन में लगा समारुतो नोपशमं छुपैति। हुआ दावानल उपशांत नहीं होता, उसी प्रकार अतिमात्र खाने वाले एवं हृषीकाग्निरनल्पभुक्तेः,
की इंद्रियाम्मि-कामाग्नि शांत नहीं होती। इसलिए प्रकामन शान्तिमाप्नोति कथञ्चनापि॥ अतिमात्र भोजन किसी भी ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता।
॥ व्याख्या ॥ . इंद्रिय-संयम और आहार-संयम का घनिष्ठ संबंध है। आहार-संयम से इन्द्रिय-संयम फलित होता है। जिस व्यक्ति का आहार संयमित नहीं होता, उसे इन्द्रियों के विषय बहुत सताते हैं। अनियमित आहार, अति आहार या अत्यल्प आहार-ये तीनों शरीर के लिए हानिकारक हैं। अति आहार से सारे धातु विषम हो जाते हैं। इस विषम स्थिति में अनेक रोग शरीर को आक्रांत कर देते हैं।
व्यक्ति अति आहार करता है, इसके कई कारण हैं : १. रसगृद्धि।
३. भोजन संबंधी नियमों की अजानकारी। २. आहार-संज्ञा की प्रबलता।
४. झूठी भूख। अति-आहार करनेवाला योग में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें चंचलता का आधिक्य रहता है। गीता में लिखा है-'नात्यर्थमश्नतो योगः'-जो अधिक खाता है, वह योग की साधना नहीं कर सकता। योगी को सदा सूक्ष्म
आहार करना चाहिए। सूक्ष्म आहार से इन्द्रियां शांत रहती हैं। इन्द्रियों की प्रशांत अवस्था में मन की एकाग्रता सधती है। आचार्य भिक्षु ने पेटू व्यक्ति की अवस्था का सुन्दर चित्र खींचा है-'जो ढूंस-ठूसकर आहार करता है, वह प्यास लगने पर पानी भी नहीं पी सकता। पानी के अभाव में उसका खाया हुआ अन्न पचता नहीं। पेट फटने लगता है। उस
व्यक्ति को क्षण-भर भी चैन नहीं होता, उसे नींद नहीं आती और वह पलभर भी शांत नहीं रह सकता। धीरे-धीरे - अनेक रोग उसे घेर लेते हैं और अंत में वह बुरी तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है।'
. १७.विविक्तशय्यासनयन्त्रितानां,
जो एकांत बस्ती और एकांत आसन से नियंत्रित हैं, जो कम अल्पाशनानं दमितेन्द्रियाणाम्। खाते हैं और जो जितेन्द्रिय हैं, उनके मन को राग-शत्रु वैसे ही रागो न वा धर्षयते हि चित्तं,
आक्रांत नहीं कर सकता जैसे औषध से पराजित रोग देह को। पराजितो व्याधिरिवौषधेन॥
॥ व्याख्या ॥ एकांतवास-मन की एकांतता में एकांत है और अनेकांतता में अनेकांत। सब जगत् एकांत है और एकांत कहीं भी नहीं है। मन को एकांत करने के लिए भी निमित्तों का महत्त्व गौण नहीं होता। निमित्त की प्रतिकूलता में एकांत मन द्वैध में चला जाता है। अव्यक्त अवस्था में वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कहना कठिन है। प्रबुद्ध मन पर उसका असर नहीं होता, यह कहा जा सकता है। मन की प्रबुद्धता के लिए वातावरण भी वैसा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
जो अतीत की असत् प्रवृत्तियों की शुद्धि कर चुका है, वर्तमान में उनसे विरत है और भविष्य में असत् प्रवृत्ति न करने का जिसका संकल्प है, उस व्यक्ति के लिए सर्वत्र एकांत है। चाहे वह गांव में रहे या जंगल में, प्रगट में रहे या अप्रगट में, वह असत् चिंतन कर ही नहीं सकता। साधना का यह उत्कर्ष रूप है। साधक सीधा वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रारंभ में एकांत वातावरण में मन को साधे और इन्द्रियों को साधे। मन और इन्द्रियों का साध लेने पर स्वप्न में भी उसका मन चलित नहीं हो सकता। एकांतवास का यह भी अर्थ है कि साधक समूह में रहता हुआ भी अकेला रहे, एकांत में रहे। इसका तात्पर्य यह है कि वह बाह्य वातावरण से प्रभावित न हो और ‘एकोऽहम्' इस मंत्र को आत्मसात् करता हुआ चले। स्थान की एकांतता से भी मन की एकांतता का अधिक महत्त्व है।