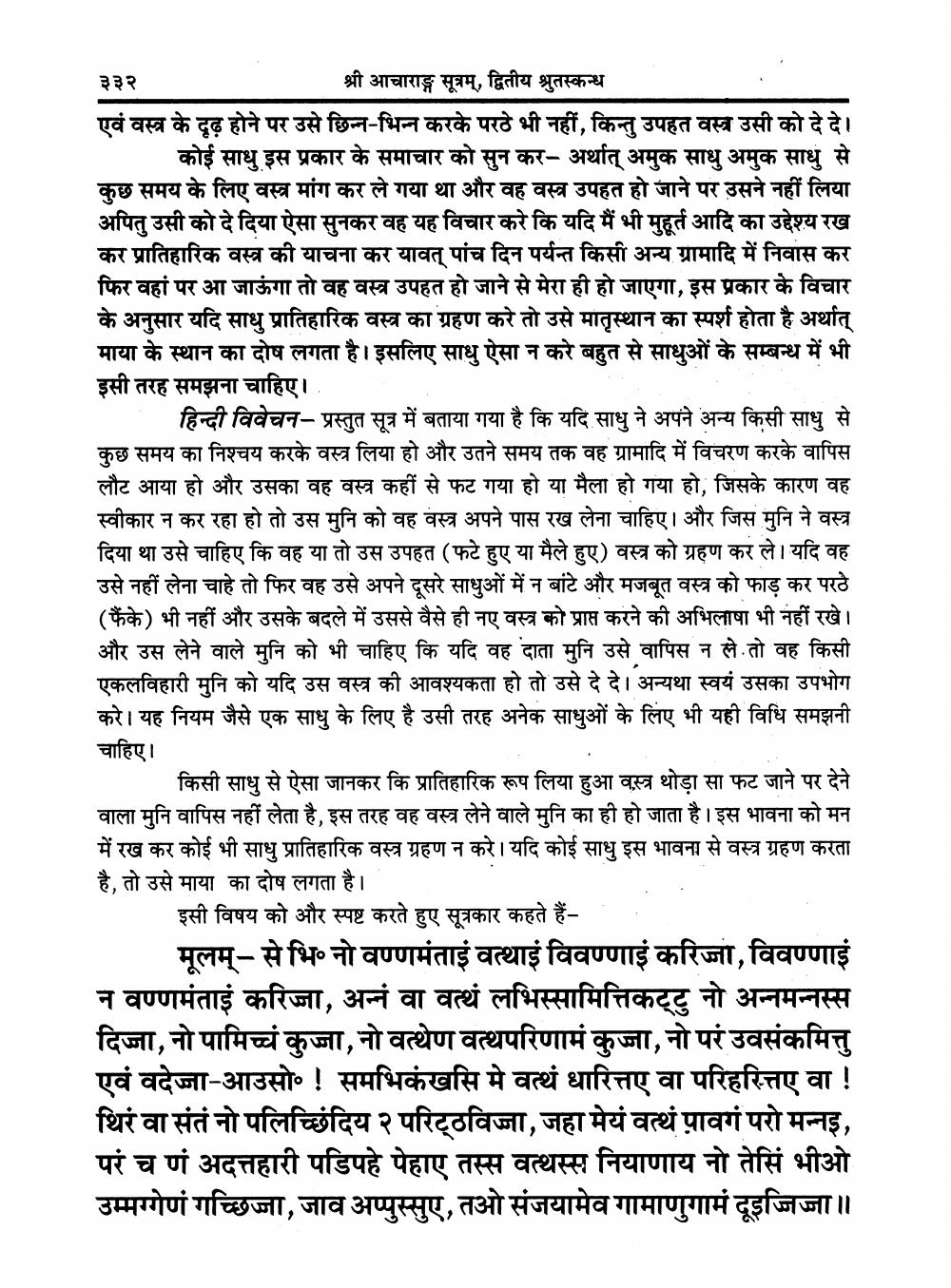________________
३३२
श्री आचाराङ्ग सूत्रम्, द्वितीय श्रुतस्कन्ध एवं वस्त्र के दृढ़ होने पर उसे छिन्न-भिन्न करके परठे भी नहीं, किन्तु उपहत वस्त्र उसी को दे दे।
कोई साधु इस प्रकार के समाचार को सुन कर- अर्थात् अमुक साधु अमुक साधु से कुछ समय के लिए वस्त्र मांग कर ले गया था और वह वस्त्र उपहत हो जाने पर उसने नहीं लिया अपितु उसी को दे दिया ऐसा सुनकर वह यह विचार करे कि यदि मैं भी मुहूर्त आदि का उद्देश्य रख कर प्रातिहारिक वस्त्र की याचना कर यावत् पांच दिन पर्यन्त किसी अन्य ग्रामादि में निवास कर फिर वहां पर आ जाऊंगा तो वह वस्त्र उपहत हो जाने से मेरा ही हो जाएगा, इस प्रकार के विचार के अनुसार यदि साधु प्रातिहारिक वस्त्र का ग्रहण करे तो उसे मातृस्थान का स्पर्श होता है अर्थात् माया के स्थान का दोष लगता है। इसलिए साधु ऐसा न करे बहुत से साधुओं के सम्बन्ध में भी इसी तरह समझना चाहिए।
हिन्दी विवेचन- प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि साधु ने अपने अन्य किसी साधु से कुछ समय का निश्चय करके वस्त्र लिया हो और उतने समय तक वह ग्रामादि में विचरण करके वापिस लौट आया हो और उसका वह वस्त्र कहीं से फट गया हो या मैला हो गया हो, जिसके कारण वह स्वीकार न कर रहा हो तो उस मुनि को वह वस्त्र अपने पास रख लेना चाहिए। और जिस मुनि ने वस्त्र दिया था उसे चाहिए कि वह या तो उस उपहत (फटे हुए या मैले हुए) वस्त्र को ग्रहण कर ले। यदि वह उसे नहीं लेना चाहे तो फिर वह उसे अपने दूसरे साधुओं में न बांटे और मजबूत वस्त्र को फाड़ कर परठे (फैंके) भी नहीं और उसके बदले में उससे वैसे ही नए वस्त्र को प्राप्त करने की अभिलाषा भी नहीं रखे। और उस लेने वाले मुनि को भी चाहिए कि यदि वह दाता मुनि उसे वापिस न ले तो वह किसी एकलविहारी मुनि को यदि उस वस्त्र की आवश्यकता हो तो उसे दे दे। अन्यथा स्वयं उसका उपभोग करे। यह नियम जैसे एक साधु के लिए है उसी तरह अनेक साधुओं के लिए भी यही विधि समझनी चाहिए।
किसी साधु से ऐसा जानकर कि प्रातिहारिक रूप लिया हुआ वस्त्र थोड़ा सा फट जाने पर देने वाला मुनि वापिस नहीं लेता है, इस तरह वह वस्त्र लेने वाले मुनि का ही हो जाता है। इस भावना को मन में रख कर कोई भी साधु प्रातिहारिक वस्त्र ग्रहण न करे। यदि कोई साधु इस भावना से वस्त्र ग्रहण करता है, तो उसे माया का दोष लगता है।
इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं
मूलम्- से भि० नो वण्णमंताई वत्थाई विवण्णाई करिजा, विवण्णाई न वण्णमंताई करिजा, अन्नं वा वत्थं लभिस्सामित्तिक? नो अन्नमन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा, नो वत्थेण वत्थपरिणामं कुज्जा, नो परं उवसंकमित्तु एवं वदेजा-आउसो ! समभिकंखसि मे वत्थं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ! थिरंवा संतं नो पलिच्छिंदिय २ परिट्ठविजा, जहा मेयं वत्थं पावगं परो मन्नइ, परं च णं अदत्तहारी पडिपहे पेहाए तस्स वत्थस्स नियाणाय नो तेसिं भीओ उम्मग्गेणंगच्छिज्जा, जाव अप्पुस्सुए, तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइजिजा॥