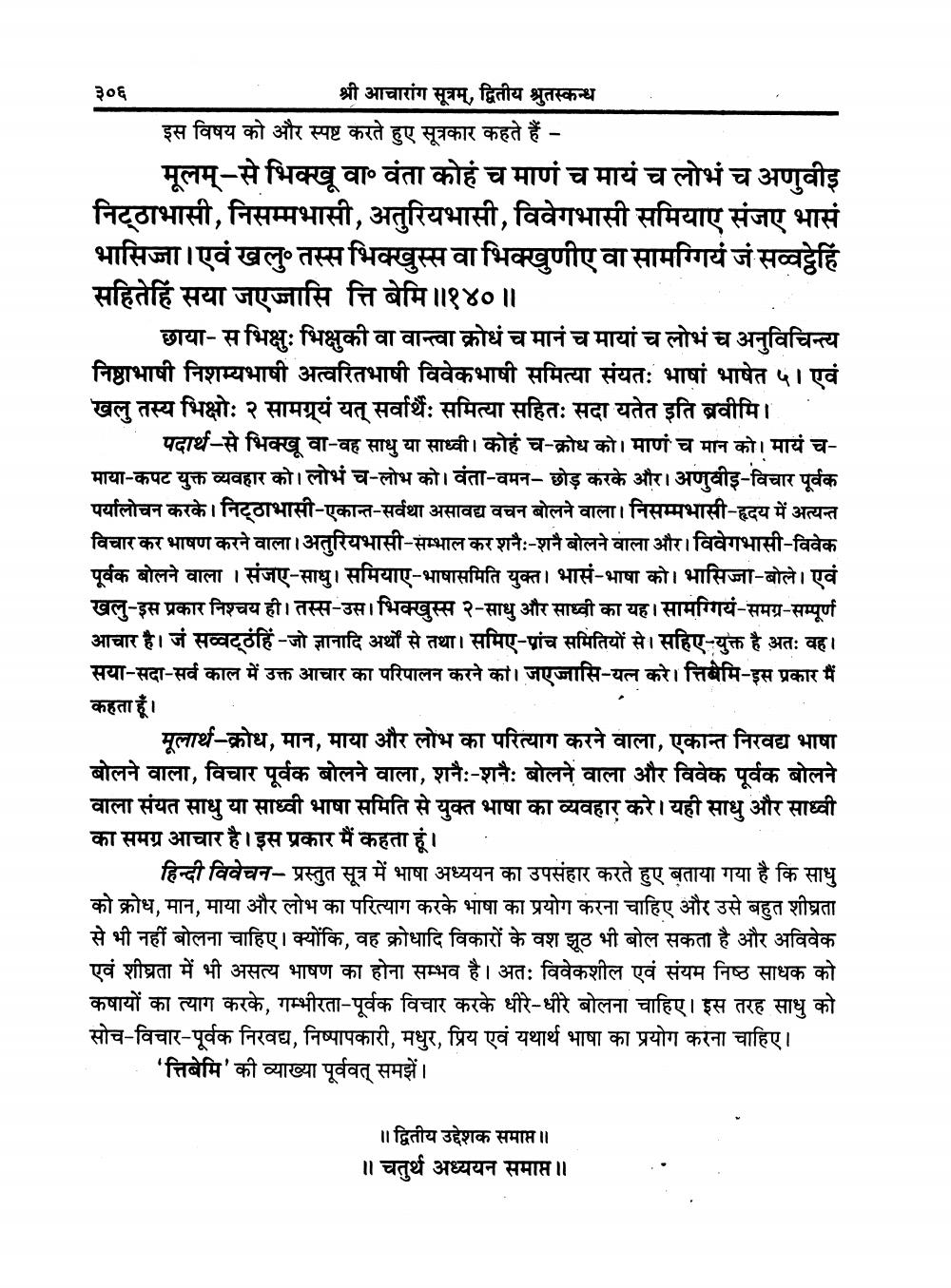________________
३०६
श्री आचारांग सूत्रम्, द्वितीय श्रुतस्कन्ध इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं -
मूलम्-से भिक्खू वा वंता कोहं च माणं च मायं च लोभं च अणुवीइ निट्ठाभासी, निसम्मभासी, अतुरियभासी, विवेगभासी समियाए संजए भासं भासिजा।एवं खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गियं जं सव्व हिं सहितेहिं सया जएजासि त्ति बेमि॥१४०॥
छाया-स भिक्षुः भिक्षुकी वा वान्त्वा क्रोधं च मानं च मायां च लोभं च अनुविचिन्त्य निष्ठाभाषी निशम्यभाषी अत्वरितभाषी विवेकभाषी समित्या संयतः भाषां भाषेत ५। एवं खलु तस्य भिक्षोः २ सामग्र्यं यत् सर्वार्थैः समित्या सहितः सदा यतेत इति ब्रवीमि।
__ पदार्थ-से भिक्खू वा-वह साधु या साध्वी। कोहं च-क्रोध को। माणं च मान को। मायं चमाया-कपट युक्त व्यवहार को। लोभं च-लोभ को। वंता-वमन- छोड़ करके और। अणुवीइ-विचार पूर्वक पर्यालोचन करके। निट्ठाभासी-एकान्त-सर्वथा असावध वचन बोलने वाला। निसम्मभासी-हृदय में अत्यन्त विचार कर भाषण करने वाला।अतुरियभासी-सम्भाल कर शनैः-शनै बोलने वाला और। विवेगभासी-विवेक पूर्वक बोलने वाला । संजए-साधु। समियाए-भाषासमिति युक्त। भासं-भाषा को। भासिज्जा-बोले। एवं खलु-इस प्रकार निश्चय ही। तस्स-उस। भिक्खुस्स २-साधु और साध्वी का यह। सामग्गियं-समग्र-सम्पूर्ण आचार है। जं सव्वळंहि-जो ज्ञानादि अर्थों से तथा। समिए-पांच समितियों से। सहिए-युक्त है अतः वह। सया-सदा-सर्व काल में उक्त आचार का परिपालन करने को। जएजासि-यत्न करे। त्तिबेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ।
मूलार्थ-क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करने वाला, एकान्त निरवद्य भाषा बोलने वाला, विचार पूर्वक बोलने वाला, शनैः-शनैः बोलने वाला और विवेक पूर्वक बोलने वाला संयत साधु या साध्वी भाषा समिति से युक्त भाषा का व्यवहार करे। यही साधु और साध्वी का समग्र आचार है। इस प्रकार मैं कहता हूं।
हिन्दी विवेचन- प्रस्तुत सूत्र में भाषा अध्ययन का उपसंहार करते हुए बताया गया है कि साधु को क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करके भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उसे बहुत शीघ्रता से भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि, वह क्रोधादि विकारों के वश झूठ भी बोल सकता है और अविवेक एवं शीघ्रता में भी असत्य भाषण का होना सम्भव है। अतः विवेकशील एवं संयम निष्ठ साधक को कषायों का त्याग करके, गम्भीरता-पूर्वक विचार करके धीरे-धीरे बोलना चाहिए। इस तरह साधु को सोच-विचार-पूर्वक निरवद्य, निष्पापकारी, मधुर, प्रिय एवं यथार्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
'त्तिबेमि' की व्याख्या पूर्ववत् समझें।
॥द्वितीय उद्देशक समाप्त॥ ॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त॥