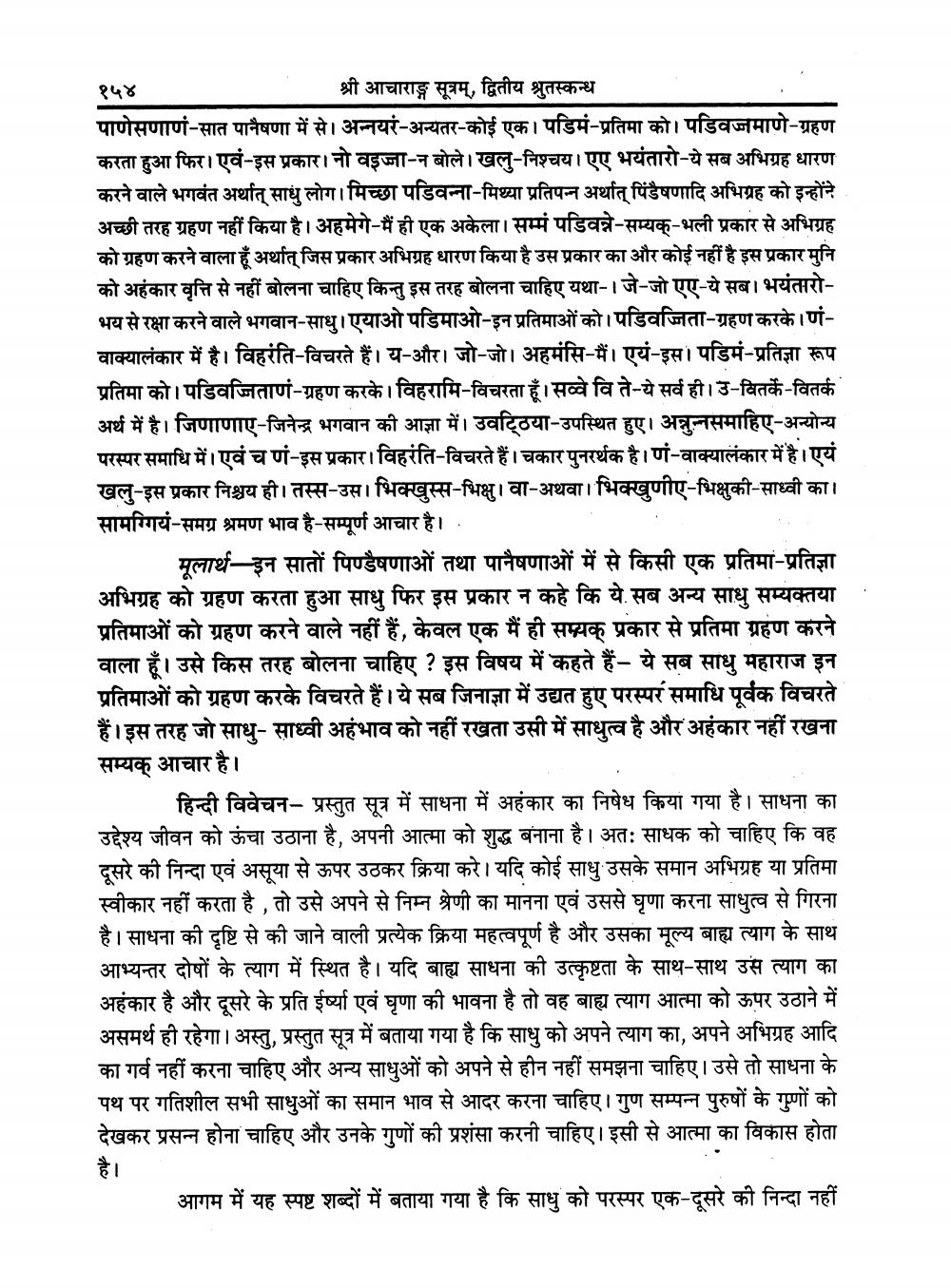________________
१५४
श्री आचाराङ्ग सूत्रम्, द्वितीय श्रुतस्कन्ध पाणेसणाणं-सात पानैषणा में से। अन्नयर-अन्यतर-कोई एक। पडिम-प्रतिमा को। पडिवजमाणे-ग्रहण करता हुआ फिर। एवं-इस प्रकार। नो वइज्जा-न बोले। खलु-निश्चय। एए भयंतारो-ये सब अभिग्रह धारण करने वाले भगवंत अर्थात् साधु लोग। मिच्छा पडिवन्ना-मिथ्या प्रतिपन्न अर्थात् पिंडैषणादि अभिग्रह को इन्होंने अच्छी तरह ग्रहण नहीं किया है। अहमेगे-मैं ही एक अकेला। सम्मं पडिवन्ने-सम्यक्-भली प्रकार से अभिग्रह को ग्रहण करने वाला हूँ अर्थात् जिस प्रकार अभिग्रह धारण किया है उस प्रकार का और कोई नहीं है इस प्रकार मुनि को अहंकार वृत्ति से नहीं बोलना चाहिए किन्तु इस तरह बोलना चाहिए यथा-। जे-जो एए-ये सब। भयंतारोभय से रक्षा करने वाले भगवान-साधु। एयाओ पडिमाओ-इन प्रतिमाओं को।पडिवजिता-ग्रहण करके।णंवाक्यालंकार में है। विहरंति-विचरते हैं। य-और। जो-जो। अहमंसि-मैं। एयं-इस। पडिम-प्रतिज्ञा रूप प्रतिमा को। पडिवज्जिताणं-ग्रहण करके। विहरामि-विचरता हूँ। सव्वे वि ते-ये सर्व ही। उ-वितर्क-वितर्क अर्थ में है। जिणाणाए-जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में। उवट्ठिया-उपस्थित हुए। अनुन्नसमाहिए-अन्योन्य परस्पर समाधि में। एवं च णं-इस प्रकार। विहरंति-विचरते हैं। चकार पुनरर्थक है। णं-वाक्यालंकार में है। एयं खलु-इस प्रकार निश्चय ही। तस्स-उस। भिक्खुस्स-भिक्षु। वा-अथवा। भिक्खुणीए-भिक्षुकी-साध्वी का। सामग्गियं-समग्र श्रमण भाव है-सम्पूर्ण आचार है। ..
मूलार्थ-इन सातों पिण्डैषणाओं तथा पानैषणाओं में से किसी एक प्रतिमा-प्रतिज्ञा अभिग्रह को ग्रहण करता हुआ साधु फिर इस प्रकार न कहे कि ये सब अन्य साधु सम्यक्तया प्रतिमाओं को ग्रहण करने वाले नहीं हैं, केवल एक मैं ही सम्यक् प्रकार से प्रतिमा ग्रहण करने वाला हूँ। उसे किस तरह बोलना चाहिए ? इस विषय में कहते हैं- ये सब साधु महाराज इन प्रतिमाओं को ग्रहण करके विचरते हैं। ये सब जिनाज्ञा में उद्यत हुए परस्परं समाधि पूर्वक विचरते हैं। इस तरह जो साधु- साध्वी अहंभाव को नहीं रखता उसी में साधुत्व है और अहंकार नहीं रखना सम्यक् आचार है।
__हिन्दी विवेचन- प्रस्तुत सूत्र में साधना में अहंकार का निषेध किया गया है। साधना का उद्देश्य जीवन को ऊंचा उठाना है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरे की निन्दा एवं असूया से ऊपर उठकर क्रिया करे। यदि कोई साधु उसके समान अभिग्रह या प्रतिमा स्वीकार नहीं करता है , तो उसे अपने से निम्न श्रेणी का मानना एवं उससे घृणा करना साधुत्व से गिरना है। साधना की दृष्टि से की जाने वाली प्रत्येक क्रिया महत्वपूर्ण है और उसका मूल्य बाह्य त्याग के साथ आभ्यन्तर दोषों के त्याग में स्थित है। यदि बाह्य साधना की उत्कृष्टता के साथ-साथ उस त्याग का अहंकार है और दूसरे के प्रति ईर्ष्या एवं घृणा की भावना है तो वह बाह्य त्याग आत्मा को ऊपर उठाने में असमर्थ ही रहेगा। अस्तु, प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को अपने त्याग का, अपने अभिग्रह आदि का गर्व नहीं करना चाहिए और अन्य साधुओं को अपने से हीन नहीं समझना चाहिए। उसे तो साधना के पथ पर गतिशील सभी साधुओं का समान भाव से आदर करना चाहिए। गुण सम्पन्न पुरुषों के गुणों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए और उनके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। इसी से आत्मा का विकास होता
आगम में यह स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि साधु को परस्पर एक-दूसरे की निन्दा नहीं