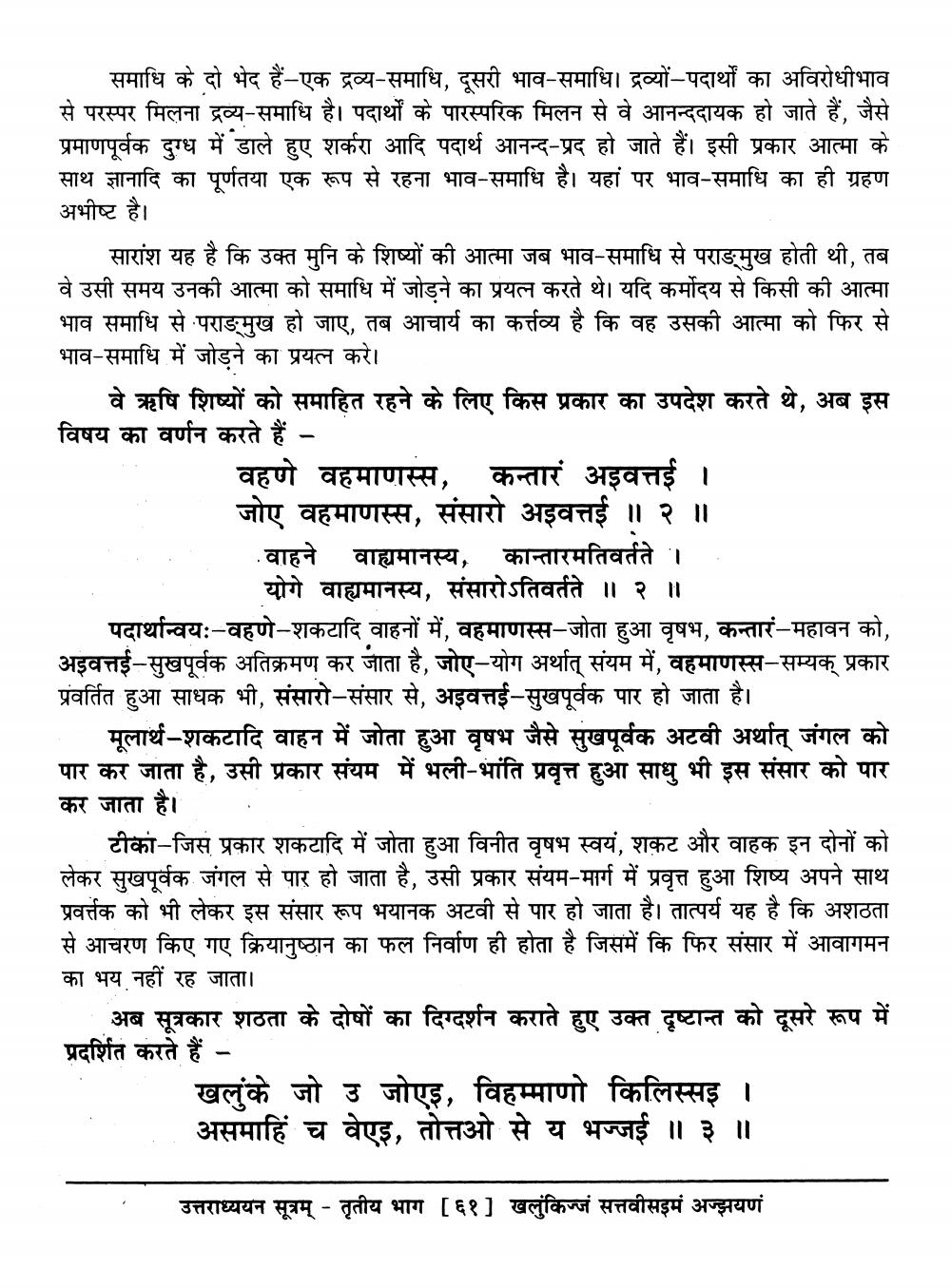________________
समाधि के दो भेद हैं- एक द्रव्य -समाधि, दूसरी भाव -समाधि । द्रव्यों- पदार्थों का अविरोधी भाव से परस्पर मिलना द्रव्य-समाधि है । पदार्थों के पारस्परिक मिलन से वे आनन्ददायक हो जाते हैं, जैसे प्रमाणपूर्वक दुग्ध में डाले हुए शर्करा आदि पदार्थ आनन्द-प्रद हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा के साथ ज्ञानादि का पूर्णतया एक रूप से रहना भाव-समाधि है। यहां पर भाव-समाधि का ही ग्रहण अभीष्ट है।
सारांश यह है कि उक्त मुनि के शिष्यों की आत्मा जब भाव- समाधि से पराङ्मुख होती थी, तब वे उसी समय उनकी आत्मा को समाधि में जोड़ने का प्रयत्न करते थे । यदि कर्मोदय से किसी की आत्मा भाव समाधि से पराङ्मुख हो जाए, तब आचार्य का कर्त्तव्य है कि वह उसकी आत्मा को फिर से भाव - समाधि में जोड़ने का प्रयत्न करे ।
वे ऋषि शिष्यों को समाहित रहने के लिए किस प्रकार का उपदेश करते थे, अब इस विषय का वर्णन करते हैं
-
वहणे वहमाणस्स,
कन्तारं अइवत्तई । जोए वहमाणस्स, संसारो अइवत्तई ॥ २ ॥ वाह्यमानस्य, कान्तारमतिवर्तते ।
. वाहने
योगे वाह्यमानस्य, संसारोऽतिवर्तते ॥ २ ॥
पदार्थान्वयः - वहणे- शकटादि वाहनों में, वहमाणस्स - जोता हुआ वृषभ, कन्तारं - महावन को, अइवत्तई-सुखपूर्वक अतिक्रमण कर जाता है, जोए - योग अर्थात् संयम में, वहमाणस्स - सम्यक् प्रकार प्रवर्तित हुआ साधक भी, संसारो-संसार से, अइवत्तई - सुखपूर्वक पार हो जाता है।
मूलार्थ - शकटादि वाहन में जोता हुआ वृषभ जैसे सुखपूर्वक अटवी अर्थात् जंगल को पार कर जाता है, उसी प्रकार संयम में भली-भांति प्रवृत्त हुआ साधु भी इस संसार को पार कर जाता है।
टीका-जिस प्रकार शकटादि में जोता हुआ विनीत वृषभ स्वयं, शकट और वाहक इन दोनों को लेकर सुखपूर्वक जंगल से पार हो जाता है, उसी प्रकार संयम मार्ग में प्रवृत्त हुआ शिष्य अपने साथ प्रवर्त्तक को भी लेकर इस संसार रूप भयानक अटवी से पार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अशठता से आचरण किए गए क्रियानुष्ठान का फल निर्वाण ही होता है जिसमें कि फिर संसार में आवागमन का भय नहीं रह जाता।
-
अब सूत्रकार शठता के दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए उक्त दृष्टान्त को दूसरे रूप में प्रदर्शित करते हैं
खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सइ । असमाहिं च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जई ॥ ३ ॥
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [६१] खलुंकिज्जं सत्तवीसइमं अज्झयणं