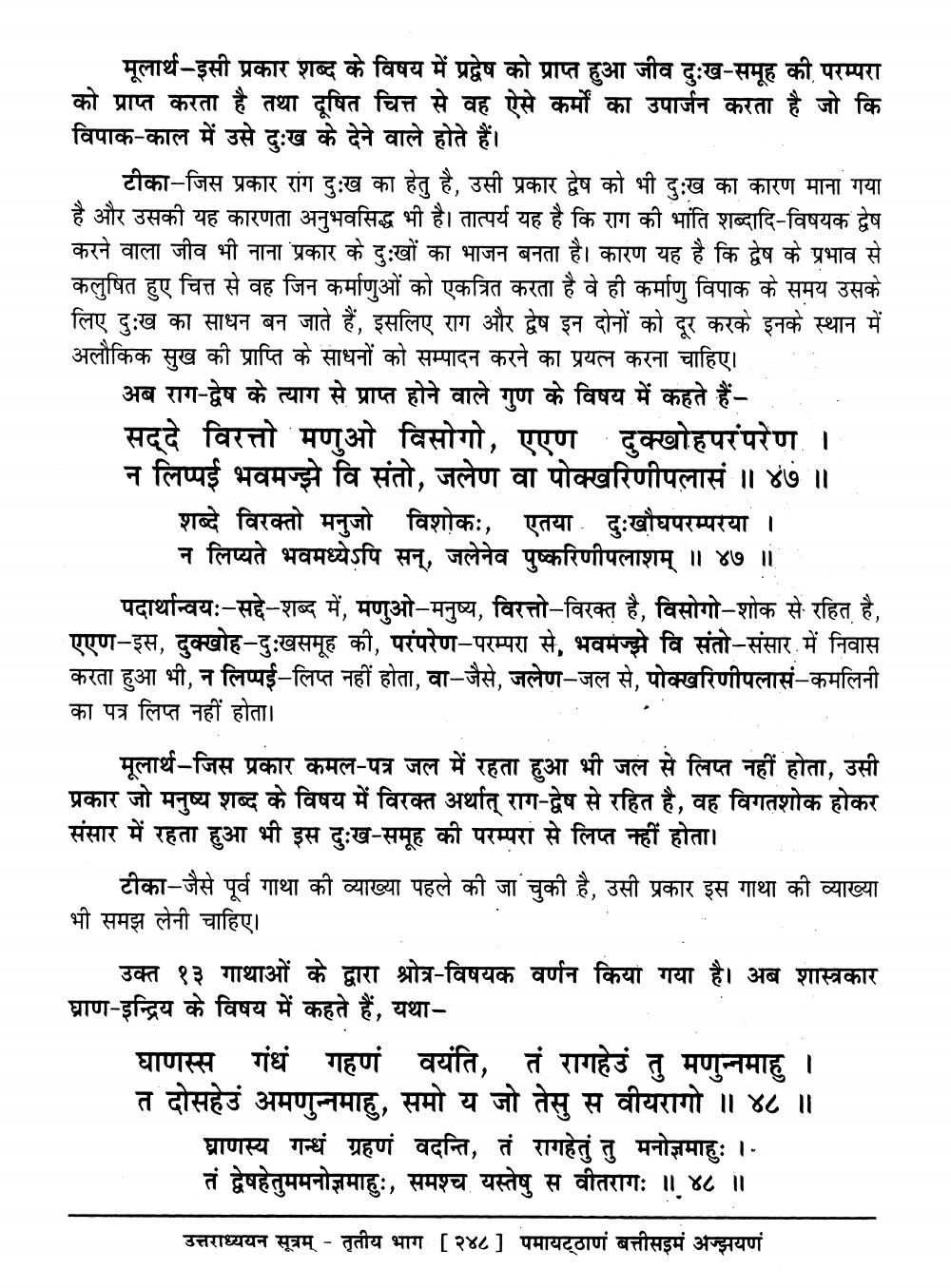________________
मूलार्थ-इसी प्रकार शब्द के विषय में प्रद्वेष को प्राप्त हुआ जीव दुःख-समूह की परम्परा को प्राप्त करता है तथा दूषित चित्त से वह ऐसे कर्मों का उपार्जन करता है जो कि विपाक-काल में उसे दुःख के देने वाले होते हैं।
टीका-जिस प्रकार रांग दुख का हेतु है, उसी प्रकार द्वेष को भी दुःख का कारण माना गया है और उसकी यह कारणता अनुभवसिद्ध भी है। तात्पर्य यह है कि राग की भांति शब्दादि-विषयक द्वेष करने वाला जीव भी नाना प्रकार के दु:खों का भाजन बनता है। कारण यह है कि द्वेष के प्रभाव से कलुषित हुए चित्त से वह जिन कर्माणुओं को एकत्रित करता है वे ही कर्माणु विपाक के समय उसके लिए दु:ख का साधन बन जाते हैं, इसलिए राग और द्वेष इन दोनों को दूर करके इनके स्थान में अलौकिक सुख की प्राप्ति के साधनों को सम्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिए।
अब राग-द्वेष के त्याग से प्राप्त होने वाले गुण के विषय में कहते हैंसद्दे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पई भवमझे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ ४७ ॥
शब्दे विरक्तो मनुजो विशोकः, एतया. दुःखौघपरम्परया ।
न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्, जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥ ४७ ॥ पदार्थान्वयः-सद्दे-शब्द में, मणुओ-मनुष्य, विरत्तो-विरक्त है, विसोगो-शोक से रहित है, एएण-इस, दुक्खोह-दुःखसमूह की, परंपरेण-परम्परा से, भवमझे वि संतो-संसार में निवास करता हुआ भी, न लिप्पई-लिप्त नहीं होता, वा-जैसे, जलेण-जल से, पोक्खरिणीपलासं-कमलिनी का पत्र लिप्त नहीं होता।
मूलार्थ-जिस प्रकार कमल-पत्र जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य शब्द के विषय में विरक्त अर्थात् राग-द्वेष से रहित है, वह विगतशोक होकर संसार में रहता हुआ भी इस दुःख-समूह की परम्परा से लिप्त नहीं होता।
टीका-जैसे पूर्व गाथा की व्याख्या पहले की जा चुकी है, उसी प्रकार इस गाथा की व्याख्या भी समझ लेनी चाहिए।
उक्त १३ गाथाओं के द्वारा श्रोत्र-विषयक वर्णन किया गया है। अब शास्त्रकार घ्राण-इन्द्रिय के विषय में कहते हैं, यथा
घाणस्स गंधं गहणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु । त दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ ४८ ॥
घ्राणस्य गन्धं ग्रहणं वदन्ति, तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।। तं द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः, समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥ ४८ ॥
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ २४८ ] पमायट्ठाणं बत्तीसइमं अज्झयणं