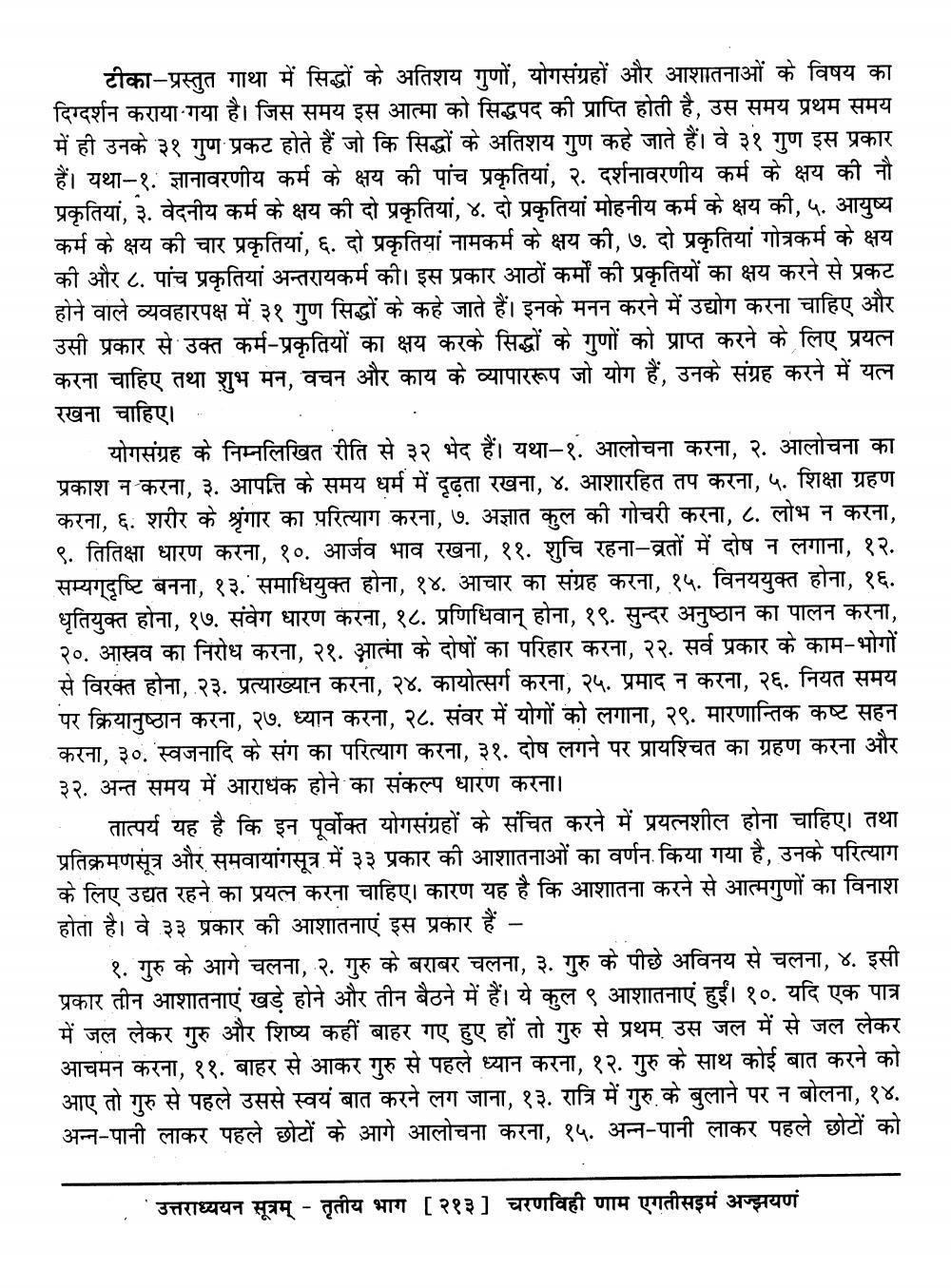________________
टीका-प्रस्तुत गाथा में सिद्धों के अतिशय गुणों, योगसंग्रहों और आशातनाओं के विषय का दिग्दर्शन कराया गया है। जिस समय इस आत्मा को सिद्धपद की प्राप्ति होती है, उस समय प्रथम समय में ही उनके ३१ गुण प्रकट होते हैं जो कि सिद्धों के अतिशय गुण कहे जाते हैं। वे ३१ गुण इस प्रकार हैं। यथा-१. ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय की पांच प्रकृतियां, २. दर्शनावरणीय कर्म के क्षय की नौ प्रकृतियां, ३. वेदनीय कर्म के क्षय की दो प्रकृतियां, ४. दो प्रकृतियां मोहनीय कर्म के क्षय की, ५. आयुष्य कर्म के क्षय की चार प्रकृतियां, ६. दो प्रकृतियां नामकर्म के क्षय की, ७. दो प्रकृतियां गोत्रकर्म के क्षय की और ८. पांच प्रकृतियां अन्तरायकर्म की। इस प्रकार आठों कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करने से प्रकट होने वाले व्यवहारपक्ष में ३१ गुण सिद्धों के कहे जाते हैं। इनके मनन करने में उद्योग करना चाहिए और उसी प्रकार से उक्त कर्म-प्रकृतियों का क्षय करके सिद्धों के गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा शुभ मन, वचन और काय के व्यापाररूप जो योग हैं, उनके संग्रह करने में यत्न रखना चाहिए। .
योगसंग्रह के निम्नलिखित रीति से ३२ भेद हैं। यथा-१. आलोचना करना, २. आलोचना का प्रकाश न करना, ३. आपत्ति के समय धर्म में दृढ़ता रखना, ४. आशारहित तप करना, ५. शिक्षा ग्रहण करना, ६. शरीर के श्रृंगार का परित्याग करना, ७. अज्ञात कुल की गोचरी करना, ८. लोभ न करना, ९. तितिक्षा धारण करना, १०. आर्जव भाव रखना, ११. शुचि रहना-व्रतों में दोष न लगाना, १२. सम्यग्दृष्टि बनना, १३. समाधियुक्त होना, १४. आचार का संग्रह करना, १५. विनययुक्त होना, १६. धृतियुक्त होना, १७. संवेग धारण करना, १८. प्रणिधिवान् होना, १९. सुन्दर अनुष्ठान का पालन करना. २०. आस्रव का निरोध करना, २१. आत्मा के दोषों का परिहार करना, २२. सर्व प्रकार के काम-भोगों से विरक्त होना, २३. प्रत्याख्यान करना, २४. कायोत्सर्ग करना, २५. प्रमाद न करना, २६. नियत समय पर क्रियानुष्ठान करना, २७. ध्यान करना, २८. संवर में योगों को लगाना, २९. मारणान्तिक कष्ट सहन करना, ३०. स्वजनादि के संग का परित्याग करना, ३१. दोष लगने पर प्रायश्चित का ग्रहण करना और ३२. अन्त समय में आराधक होने का संकल्प धारण करना।
तात्पर्य यह है कि इन पूर्वोक्त योगसंग्रहों के संचित करने में प्रयत्नशील होना चाहिए। तथा प्रतिक्रमणसूत्र और समवायांगसूत्र में ३३ प्रकार की आशातनाओं का वर्णन किया गया है, उनके परित्याग के लिए उद्यत रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कारण यह है कि आशातना करने से आत्मगुणों का विनाश होता है। वे ३३ प्रकार की आशातनाएं इस प्रकार हैं -
१. गुरु के आगे चलना, २. गुरु के बराबर चलना, ३. गुरु के पीछे अविनय से चलना, ४. इसी प्रकार तीन आशातनाएं खड़े होने और तीन बैठने में हैं। ये कुल ९ आशातनाएं हुईं। १०. यदि एक पात्र में जल लेकर गुरु और शिष्य कहीं बाहर गए हुए हों तो गुरु से प्रथम उस जल में से जल लेकर आचमन करना, ११. बाहर से आकर गुरु से पहले ध्यान करना, १२. गुरु के साथ कोई बात करने को आए तो गुरु से पहले उससे स्वयं बात करने लग जाना, १३. रात्रि में गुरु के बुलाने पर न बोलना, १४. अन्न-पानी लाकर पहले छोटों के आगे आलोचना करना, १५. अन्न-पानी लाकर पहले छोटों को
, 'उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ २१३] चरणविही णाम एगतीसइमं अज्झयणं