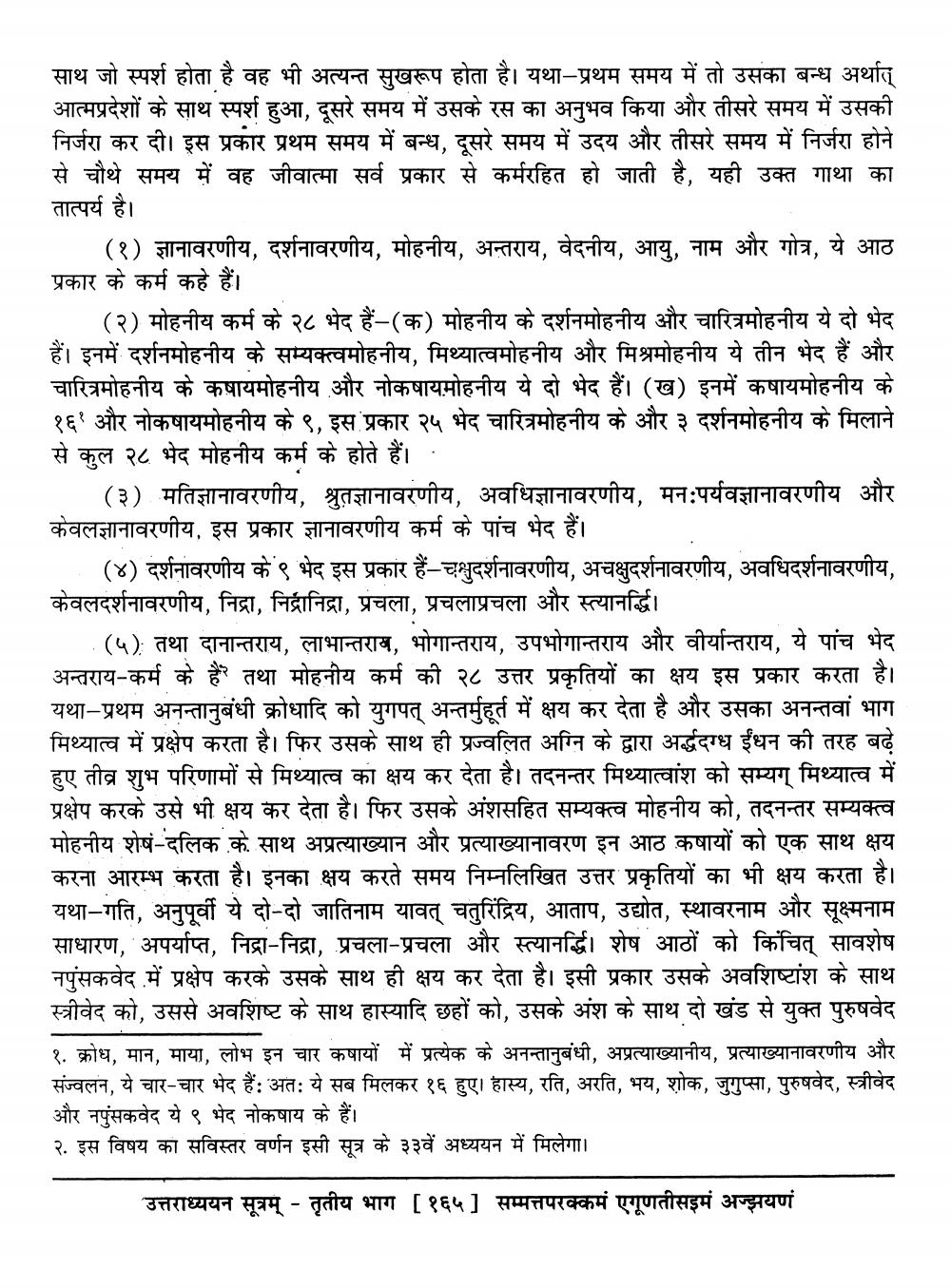________________
साथ जो स्पर्श होता है वह भी अत्यन्त सुखरूप होता है । यथा - प्रथम समय में तो उसका बन्ध अर्थात् आत्मप्रदेशों के साथ स्पर्श हुआ, दूसरे समय में उसके रस का अनुभव किया और तीसरे समय में उसकी निर्जरा कर दी। इस प्रकार प्रथम समय में बन्ध, दूसरे समय में उदय और तीसरे समय में निर्जरा होने से चौथे समय में वह जीवात्मा सर्व प्रकार से कर्मरहित हो जाती है, यही उक्त गाथा का तात्पर्य है।
(१) ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये आठ प्रकार के कर्म कहे हैं।
(२) मोहनीय कर्म के २८ भेद हैं- (क) मोहनीय के दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ये दो भेद हैं। इनमें दर्शनमोहनीय के सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय ये तीन भेद हैं और चारित्रमोहनीय के कषायमोहनीय और नोकषायमोहनीय ये दो भेद हैं। (ख) इनमें कषायमोहनीय के १६' और नोकषायमोहनीय के ९, इस प्रकार २५ भेद चारित्रमोहनीय के और ३ दर्शनमोहनीय के मिलाने से कुल २८ भेद मोहनीय कर्म के होते हैं।
(३) मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनः पर्यवज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय, इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के पांच भेद हैं।
(४) दर्शनावरणीय के ९ भेद इस प्रकार हैं-चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, केवलदर्शनावरणीय, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्द्धि ।
(५) तथा दानान्तराय, लाभान्तराम, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय, ये पांच भेद अन्तराय-कर्म के हैं तथा मोहनीय कर्म की २८ उत्तर प्रकृतियों का क्षय इस प्रकार करता है। यथा - प्रथम अनन्तानुबंधी क्रोधादि को युगपत् अन्तर्मुहूर्त में क्षय कर देता है और उसका अनन्तवां भाग मिथ्यात्व में प्रक्षेप करता है। फिर उसके साथ ही प्रज्वलित अग्नि के द्वारा अर्द्धदग्ध ईंधन की तरह बढ़े हुए तीव्र शुभ परिणामों से मिथ्यात्व का क्षय कर देता है । तदनन्तर मिथ्यात्वांश को सम्यग् मिथ्यात्व में प्रक्षेप करके उसे भी क्षय कर देता है। फिर उसके अंशसहित सम्यक्त्व मोहनीय को, तदनन्तर सम्यक्त्व मोहनीय शेषं - दलिक के साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण इन आठ कषायों को एक साथ क्षय करना आरम्भ करता है। इनका क्षय करते समय निम्नलिखित उत्तर प्रकृतियों का भी क्षय करता है। यथा-गति, अनुपूर्वी ये दो-दो जातिनाम यावत् चतुरिंद्रिय, आताप, उद्योत, स्थावरनाम और सूक्ष्मनाम साधारण, अपर्याप्त, निद्रा-निद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्द्धि । शेष आठों को किंचित् सावशेष नपुंसकवेद में प्रक्षेप करके उसके साथ ही क्षय कर देता है। इसी प्रकार उसके अवशिष्टांश के साथ स्त्रीवेद को, उससे अवशिष्ट के साथ हास्यादि छहों को, उसके अंश के साथ दो खंड से युक्त पुरुषवेद १. क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायों में प्रत्येक के अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानावरणीय और संज्वलन, ये चार - चार भेद हैं: अतः ये सब मिलकर १६ हुए। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद ये ९ भेद नोकषाय के हैं।
२. इस विषय का सविस्तर वर्णन इसी सूत्र के ३३वें अध्ययन में मिलेगा।
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [१६५ ] सम्मत्तपरक्कमं एगूणतीसइमं अज्झयणं