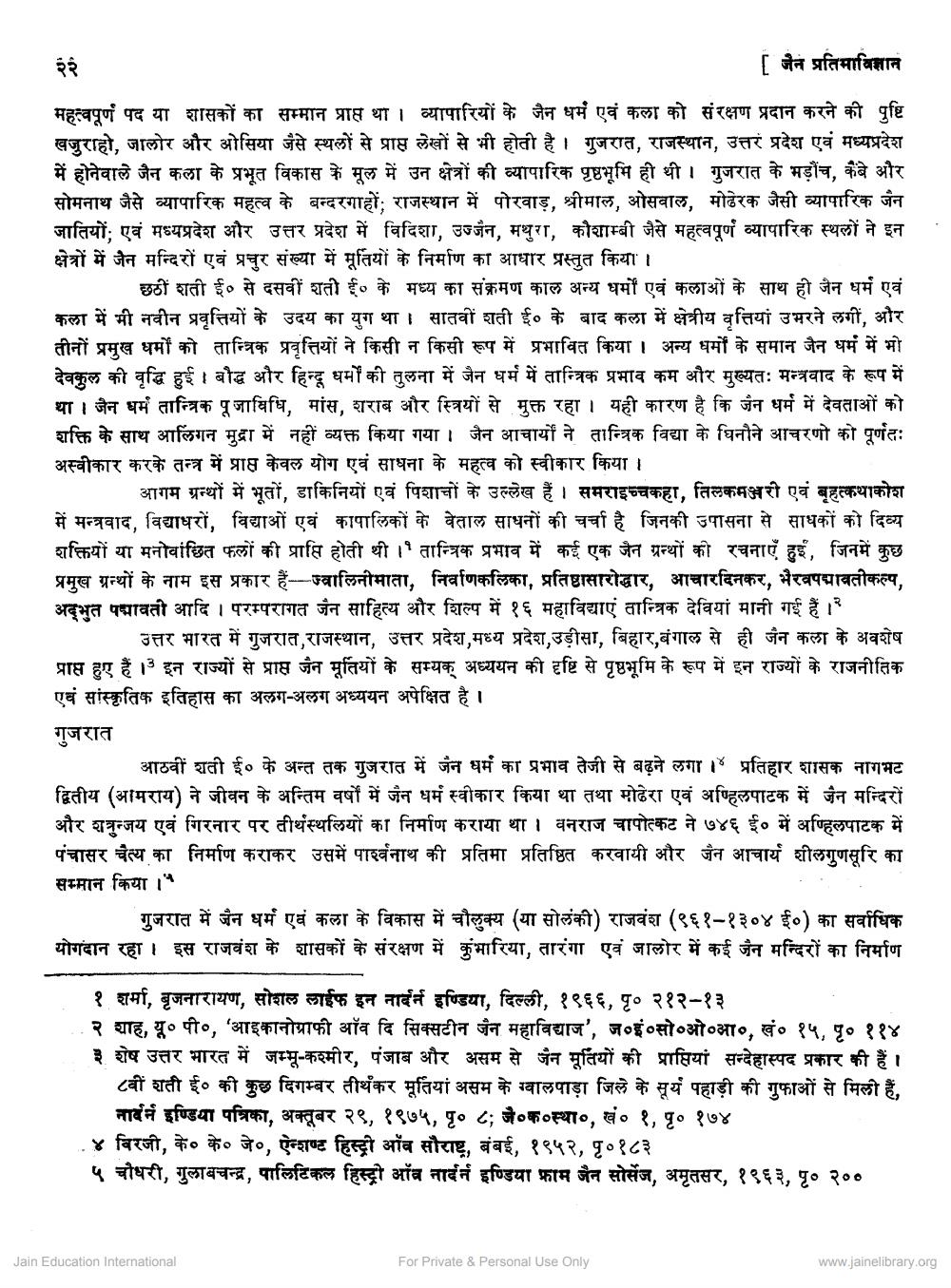________________
२२
[ जैन प्रतिमाविज्ञान
महत्वपूर्ण पद या शासकों का सम्मान प्राप्त था । व्यापारियों के जैन धर्मं एवं कला को संरक्षण प्रदान करने की पुष्टि खजुराहो, जालोर और ओसिया जैसे स्थलों से प्राप्त लेखों से भी होती है । गुजरात, राजस्थान, उत्तरं प्रदेश एवं मध्यप्रदेश में होनेवाले जैन कला के प्रभूत विकास के मूल में उन क्षेत्रों की व्यापारिक पृष्ठभूमि ही थी । गुजरात के मड़ौंच, कैबे और सोमनाथ जैसे व्यापारिक महत्व के बन्दरगाहों; राजस्थान में पोरवाड़, श्रीमाल, ओसवाल, मोढेरक जैसी व्यापारिक जैन जातियों; एवं मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में विदिशा, उज्जैन, मथुरा, कौशाम्बी जैसे महत्वपूर्णं व्यापारिक स्थलों ने इन क्षेत्रों में जैन मन्दिरों एवं प्रचुर संख्या में मूर्तियों के निर्माण का आधार प्रस्तुत किया ।
छठीं शती ई० से दसवीं शती ई० के मध्य का संक्रमण काल अन्य धर्मों एवं कलाओं के साथ ही जैन धर्म एवं कला में मी नवीन प्रवृत्तियों के उदय का युग था । सातवीं शती ई० के बाद कला में क्षेत्रीय वृत्तियां उभरने लगीं, और तीनों प्रमुख धर्मों को तान्त्रिक प्रवृत्तियों ने किसी न किसी रूप में प्रभावित किया । अन्य धर्मों के समान जैन धर्म में भो देवकुल की वृद्धि हुई । बौद्ध और हिन्दू धर्मों की तुलना में जैन धर्म में तान्त्रिक प्रभाव कम और मुख्यतः मन्त्रवाद के रूप में था । जैन धर्मं तान्त्रिक पूजाविधि, मांस, शराब और स्त्रियों से मुक्त रहा। यही कारण है कि जैन धर्म में देवताओं को जैन आचार्यों ने तान्त्रिक विद्या के घिनौने आचरणों को पूर्णतः महत्व को स्वीकार किया ।
शक्ति के साथ आलिंगन मुद्रा में नहीं व्यक्त किया गया। अस्वीकार करके तन्त्र में प्राप्त केवल योग एवं साधना के
आगम ग्रन्थों में भूतों, डाकिनियों एवं पिशाचों के उल्लेख हैं । समराइच्चकहा, तिलकमञ्जरी एवं बृहत्कथाकोश में मन्त्रवाद, विद्याधरों, विद्याओं एवं कापालिकों के वेताल साधनों की चर्चा है जिनकी उपासना से साधकों को दिव्य शक्तियों या मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती थी । तान्त्रिक प्रभाव में कई एक जैन ग्रन्थों की रचनाएँ हुईं, जिनमें कुछ प्रमुख ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-ज्वालिनीमाता, निर्वाणकलिका, प्रतिष्ठासारोद्धार, आचारदिनकर, भैरवपद्मावतीकल्प, अद्भुत पद्मावती आदि । परम्परागत जैन साहित्य और शिल्प में १६ महाविद्याएं तान्त्रिक देवियां मानी गई हैं ।
उत्तर भारत में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल से प्राप्त हुए हैं । इन राज्यों से प्राप्त जैन मूर्तियों के सम्यक् अध्ययन की दृष्टि से पृष्ठभूमि के रूप में एवं सांस्कृतिक इतिहास का अलग-अलग अध्ययन अपेक्षित है ।
गुजरात
आठवीं शती ई० के अन्त तक गुजरात में जैन धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा । प्रतिहार शासक नागभट द्वितीय (आमराय) ने जीवन के अन्तिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार किया था तथा मोढेरा एवं अहिलपाटक में जैन मन्दिरों और शत्रुन्जय एवं गिरनार पर तीर्थस्थलियों का निर्माण कराया था । वनराज चापोत्कट ने ७४६ ई० में अहिलपाटक में पंचासर चैत्य का निर्माण कराकर उसमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवायी और जैन आचार्य शीलगुणसूरि का सम्मान किया।
ही जैन कला के अवशेष इन राज्यों के राजनीतिक
गुजरात में जैन धर्म एवं कला के विकास में चौलुक्य (या सोलंकी ) राजवंश (९६१ - १३०४ ई० ) का सर्वाधिक योगदान रहा । इस राजवंश के शासकों के संरक्षण में कुंभारिया, तारंगा एवं जालोर में कई जैन मन्दिरों का निर्माण
१ शर्मा, बृजनारायण, सोशल लाईफ इन नार्दर्न इण्डिया, दिल्ली, १९६६, पृ० २१२-१३
२ शाह, यू०पी०, 'आइकानोग्राफी ऑव दि सिक्सटीन जैन महाविद्याज', ज०ई०सी०ओ०आ०, खं० १५, पृ० ११४ ३ शेष उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम से जैन मूर्तियों की प्राप्तियां सन्देहास्पद प्रकार की हैं । ८वीं शती ई० की कुछ दिगम्बर तीर्थंकर मूर्तियां असम के ग्वालपाड़ा जिले के सूर्य पहाड़ी की गुफाओं से मिली हैं, नार्दर्न इण्डिया पत्रिका, अक्तूबर २९, १९७५, पृ० ८; जै०क०स्था०, खं० १, पृ० १७४
४ बिरजी, के० के० जे०, ऐन्शष्ट हिस्ट्री ऑव सौराष्ट्र, बंबई, १९५२, पृ०१८३
५ चौधरी, गुलाबचन्द्र, पालिटिकल हिस्ट्री ऑव नार्दर्न इण्डिया फ्राम जैन सोर्सेज, अमृतसर, १९६३, पृ० २००
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org