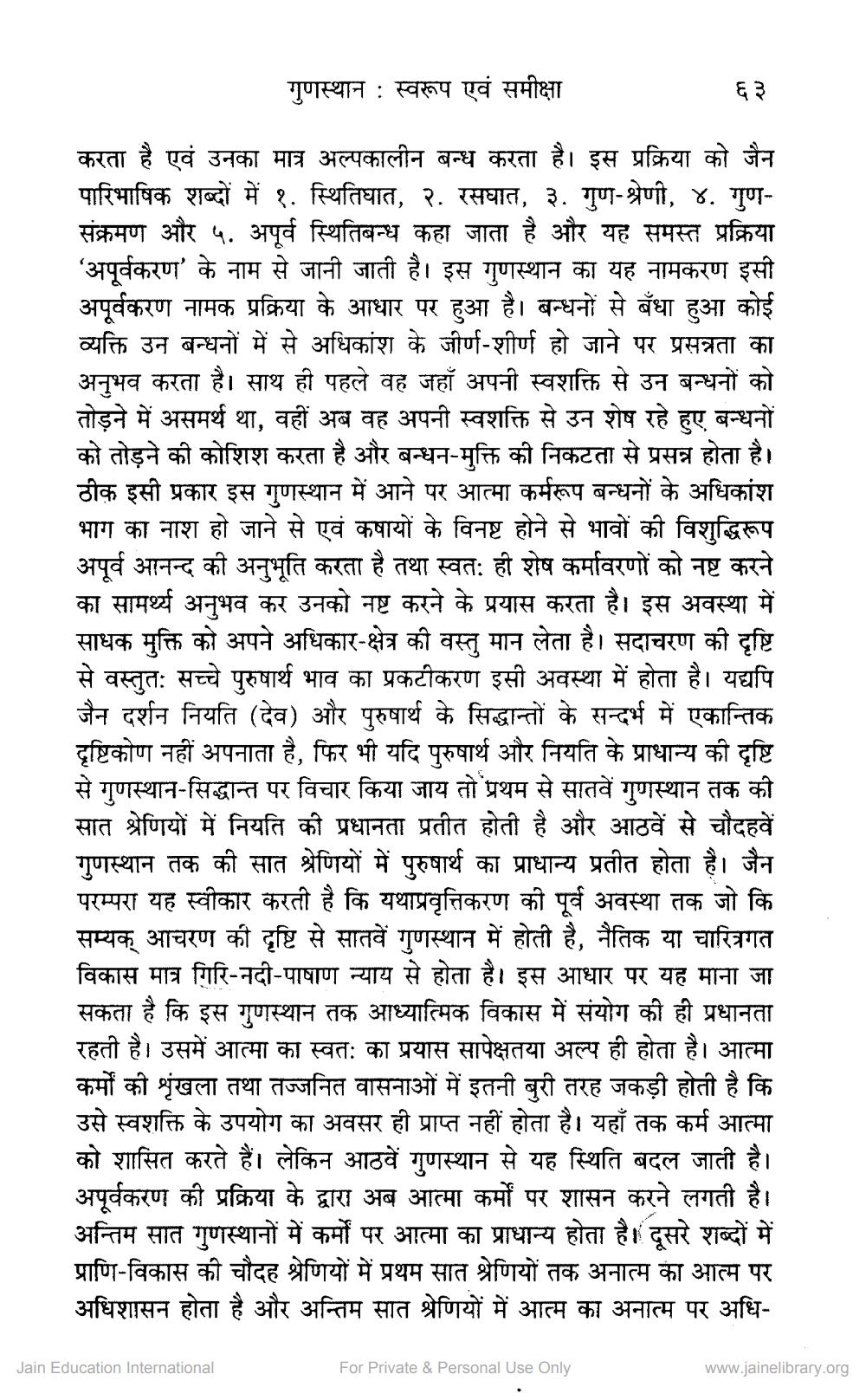________________
गुणस्थान : स्वरूप एवं समीक्षा
६३
करता है एवं उनका मात्र अल्पकालीन बन्ध करता है। इस प्रक्रिया को जैन पारिभाषिक शब्दों में १. स्थितिघात, २. रसघात, ३. गुण-श्रेणी, ४. गुणसंक्रमण और ५. अपर्व स्थितिबन्ध कहा जाता है और यह समस्त प्रक्रिया 'अपूर्वकरण' के नाम से जानी जाती है। इस गुणस्थान का यह नामकरण इसी अपूर्वकरण नामक प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। बन्धनों से बँधा हुआ कोई व्यक्ति उन बन्धनों में से अधिकांश के जीर्ण-शीर्ण हो जाने पर प्रसन्नता का अनुभव करता है। साथ ही पहले वह जहाँ अपनी स्वशक्ति से उन बन्धनों को तोड़ने में असमर्थ था, वहीं अब वह अपनी स्वशक्ति से उन शेष रहे हए बन्धनों को तोड़ने की कोशिश करता है और बन्धन-मुक्ति की निकटता से प्रसन्न होता है। ठीक इसी प्रकार इस गुणस्थान में आने पर आत्मा कर्मरूप बन्धनों के अधिकांश भाग का नाश हो जाने से एवं कषायों के विनष्ट होने से भावों की विशुद्धिरूप अपूर्व आनन्द की अनुभूति करता है तथा स्वत: ही शेष कर्मावरणों को नष्ट करने का सामर्थ्य अनुभव कर उनको नष्ट करने के प्रयास करता है। इस अवस्था में साधक मुक्ति को अपने अधिकार-क्षेत्र की वस्तु मान लेता है। सदाचरण की दृष्टि से वस्तुत: सच्चे पुरुषार्थ भाव का प्रकटीकरण इसी अवस्था में होता है। यद्यपि जैन दर्शन नियति (देव) और पुरुषार्थ के सिद्धान्तों के सन्दर्भ में एकान्तिक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है, फिर भी यदि पुरुषार्थ और नियति के प्राधान्य की दृष्टि से गुणस्थान-सिद्धान्त पर विचार किया जाय तो प्रथम से सातवें गुणस्थान तक की सात श्रेणियों में नियति की प्रधानता प्रतीत होती है और आठवें से चौदहवें गुणस्थान तक की सात श्रेणियों में पुरुषार्थ का प्राधान्य प्रतीत होता है। जैन परम्परा यह स्वीकार करती है कि यथाप्रवृत्तिकरण की पूर्व अवस्था तक जो कि सम्यक् आचरण की दृष्टि से सातवें गुणस्थान में होती है, नैतिक या चारित्रगत विकास मात्र गिरि-नदी-पाषाण न्याय से होता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि इस गुणस्थान तक आध्यात्मिक विकास में संयोग की ही प्रधानता रहती है। उसमें आत्मा का स्वत: का प्रयास सापेक्षतया अल्प ही होता है। आत्मा कर्मों की श्रृंखला तथा तज्जनित वासनाओं में इतनी बुरी तरह जकड़ी होती है कि उसे स्वशक्ति के उपयोग का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कर्म आत्मा को शासित करते हैं। लेकिन आठवें गुणस्थान से यह स्थिति बदल जाती है। अपूर्वकरण की प्रक्रिया के द्वारा अब आत्मा कर्मों पर शासन करने लगती है। अन्तिम सात गुणस्थानों में कर्मों पर आत्मा का प्राधान्य होता है। दूसरे शब्दों में प्राणि-विकास की चौदह श्रेणियों में प्रथम सात श्रेणियों तक अनात्म का आत्म पर अधिशासन होता है और अन्तिम सात श्रेणियों में आत्म का अनात्म पर अधि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org