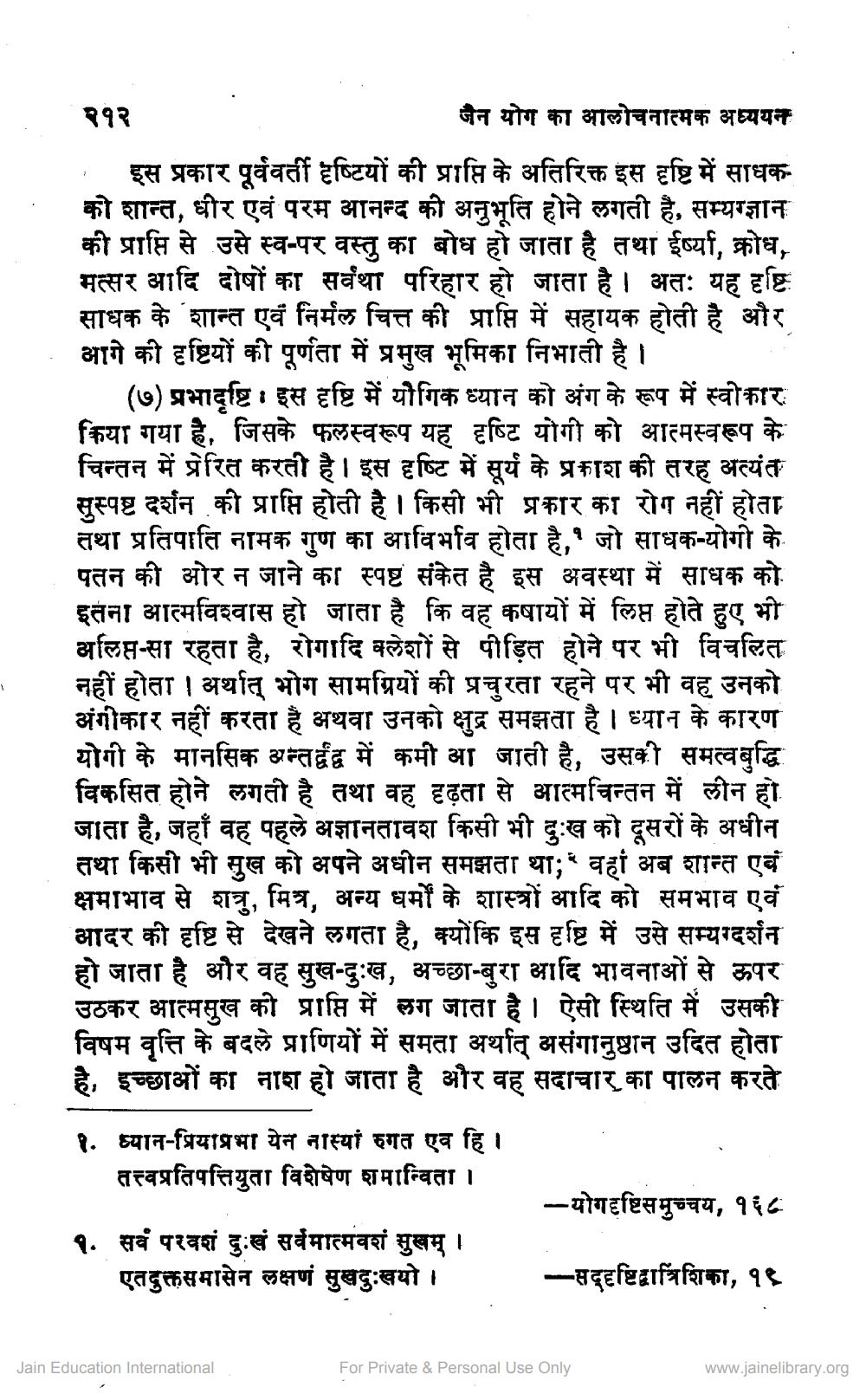________________
२१२
जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन । इस प्रकार पूर्ववर्ती दृष्टियों की प्राप्ति के अतिरिक्त इस दृष्टि में साधक को शान्त, धीर एवं परम आनन्द की अनुभूति होने लगती है, सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति से उसे स्व-पर वस्तु का बोध हो जाता है तथा ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर आदि दोषों का सर्वथा परिहार हो जाता है। अतः यह दृष्टि साधक के शान्त एवं निर्मल चित्त की प्राप्ति में सहायक होती है और आगे की दृष्टियों की पूर्णता में प्रमुख भूमिका निभाती है।
(७) प्रभादृष्टि । इस दृष्टि में यौगिक ध्यान को अंग के रूप में स्वीकार. किया गया है, जिसके फलस्वरूप यह दृष्टि योगी को आत्मस्वरूप के चिन्तन में प्रेरित करती है। इस दृष्टि में सूर्य के प्रकाश की तरह अत्यंत सुस्पष्ट दर्शन की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता तथा प्रतिपाति नामक गुण का आविर्भाव होता है, जो साधक-योगी के पतन की ओर न जाने का स्पष्ट संकेत है इस अवस्था में साधक को इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि वह कषायों में लिप्त होते हुए भी अलिप्त-सा रहता है, रोगादि क्लेशों से पीड़ित होने पर भी विचलित नहीं होता । अर्थात् भोग सामग्रियों की प्रचुरता रहने पर भी वह उनको अंगीकार नहीं करता है अथवा उनको क्षुद्र समझता है । ध्यान के कारण योगी के मानसिक अन्तर्द्वद्व में कमी आ जाती है, उसकी समत्वबुद्धि विकसित होने लगती है तथा वह दृढ़ता से आत्मचिन्तन में लीन हो जाता है, जहाँ वह पहले अज्ञानतावश किसी भी दुःख को दूसरों के अधीन तथा किसी भी सुख को अपने अधीन समझता था; वहां अब शान्त एवं क्षमाभाव से शत्रु, मित्र, अन्य धर्मों के शास्त्रों आदि को समभाव एवं आदर की दृष्टि से देखने लगता है, क्योंकि इस दृष्टि में उसे सम्यग्दर्शन हो जाता है और वह सुख-दुःख, अच्छा-बुरा आदि भावनाओं से ऊपर उठकर आत्मसुख की प्राप्ति में लग जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी विषम वृत्ति के बदले प्राणियों में समता अर्थात् असंगानुष्ठान उदित होता है, इच्छाओं का नाश हो जाता है और वह सदाचार का पालन करते
१. ध्यान-प्रियाप्रभा येन नास्यां रुगत एव हि ।
तत्त्वप्रतिपत्तियुता विशेषेण शमान्विता ।
-योगदृष्टिसमुच्चय, १६८
१. सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।
एतदुक्तसमासेन लक्षणं सुखदुःखयो।
-सदृष्टिद्वात्रिंशिका, १९
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org