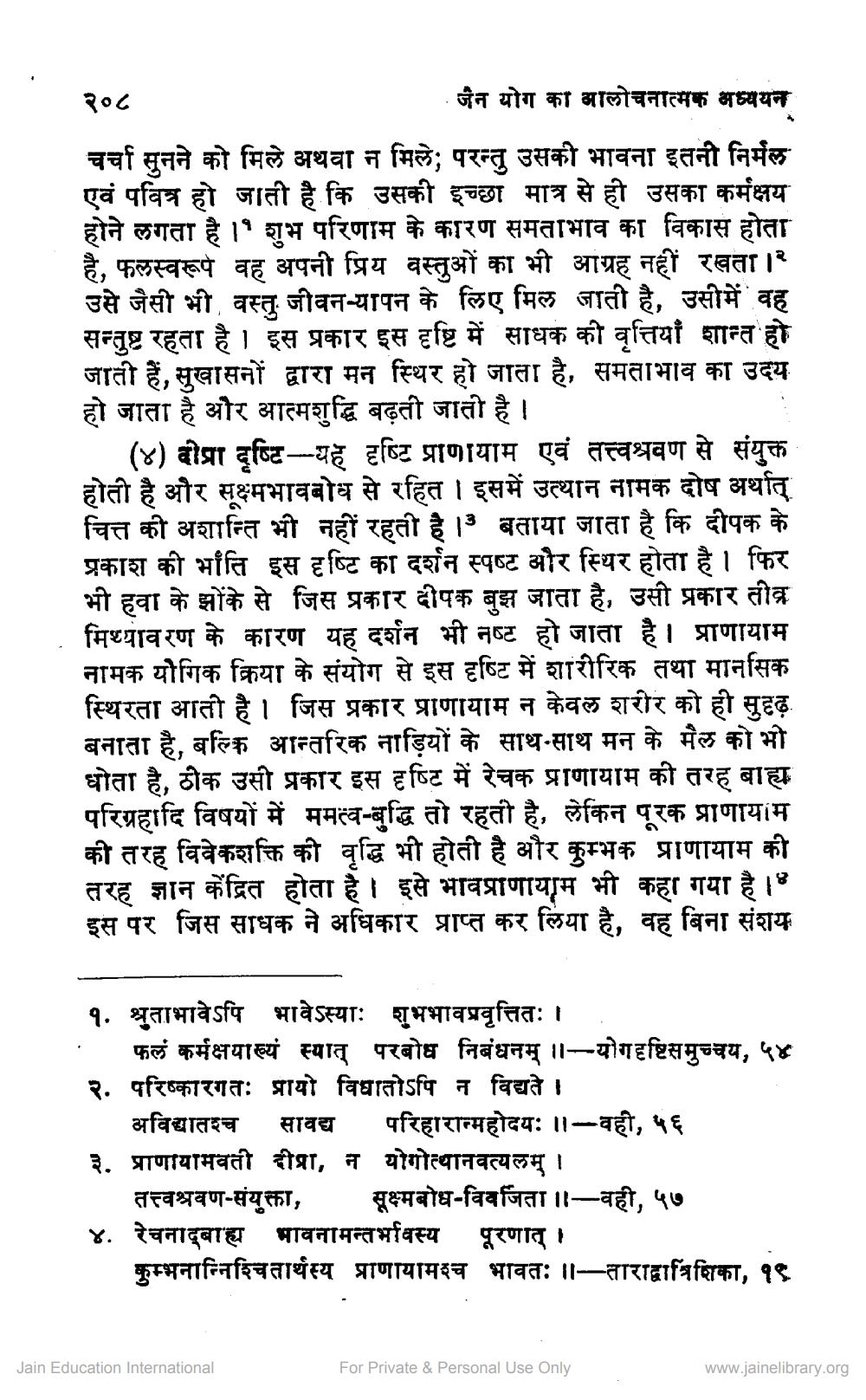________________
२०८
जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन
चर्चा सुनने को मिले अथवा न मिले; परन्तु उसकी भावना इतनी निर्मल एवं पवित्र हो जाती है कि उसकी इच्छा मात्र से ही उसका कर्मक्षय होने लगता है ।" शुभ परिणाम के कारण समताभाव का विकास होता है, फलस्वरूपे वह अपनी प्रिय वस्तुओं का भी आग्रह नहीं रखता । उसे जैसी भी वस्तु जीवन-यापन के लिए मिल जाती है, उसीमें वह सन्तुष्ट रहता है । इस प्रकार इस दृष्टि में साधक की वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं, सुखासनों द्वारा मन स्थिर हो जाता है, समताभाव का उदय हो जाता है और आत्मशुद्धि बढ़ती जाती है ।
(४) वीप्रा दृष्टि - यह दृष्टि प्राणायाम एवं तत्त्वश्रवण से संयुक्त होती है और सूक्ष्मभावबोध से रहित । इसमें उत्थान नामक दोष अर्थात् चित्त की अशान्ति भी नहीं रहती है । बताया जाता है कि दीपक के प्रकाश की भांति इस दृष्टि का दर्शन स्पष्ट और स्थिर होता है । फिर भी हवा के झोंके से जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तीव्र मिथ्यावरण के कारण यह दर्शन भी नष्ट हो जाता है । प्राणायाम नामक यौगिक क्रिया के संयोग से इस दृष्टि में शारीरिक तथा मानसिक स्थिरता आती है । जिस प्रकार प्राणायाम न केवल शरीर को ही सुदृढ़ बनाता है, बल्कि आन्तरिक नाड़ियों के साथ-साथ मन के मैल को भी धोता है, ठीक उसी प्रकार इस दृष्टि में रेचक प्राणायाम की तरह बाह्य परिग्रहादि विषयों में ममत्व-बुद्धि तो रहती है, लेकिन पूरक प्राणायाम की तरह विवेकशक्ति की वृद्धि भी होती है और कुम्भक प्राणायाम की तरह ज्ञान केंद्रित होता है । इसे भावप्राणायाम भी कहा गया है । " इस पर जिस साधक ने अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह बिना संशय
१. श्रुताभावेऽपि भावेऽस्याः शुभभावप्रवृत्तितः ।
फलं कर्मक्षयाख्यं स्यात् परबोध निबंधनम् ॥ -- योग दृष्टिसमुच्चय, ५४ २. परिष्कारगतः प्रायो विधातोऽपि न विद्यते ।
अविद्यातश्च सावद्य परिहारान्महोदयः ॥ - वही, ५६ ३. प्राणायामवती दीप्रा, न योगोत्थानवत्यलम् ।
तत्त्वश्रवण-संयुक्ता, सूक्ष्मबोध - विवर्जिता ॥ - वही,
५७
४. रेचनाद्बाह्य भावनामन्तर्भावस्य पूरणात् ।
कुम्भनान्निश्चितार्थस्य प्राणायामश्च भावतः ॥ - ताराद्वात्रिंशिका, १९
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org