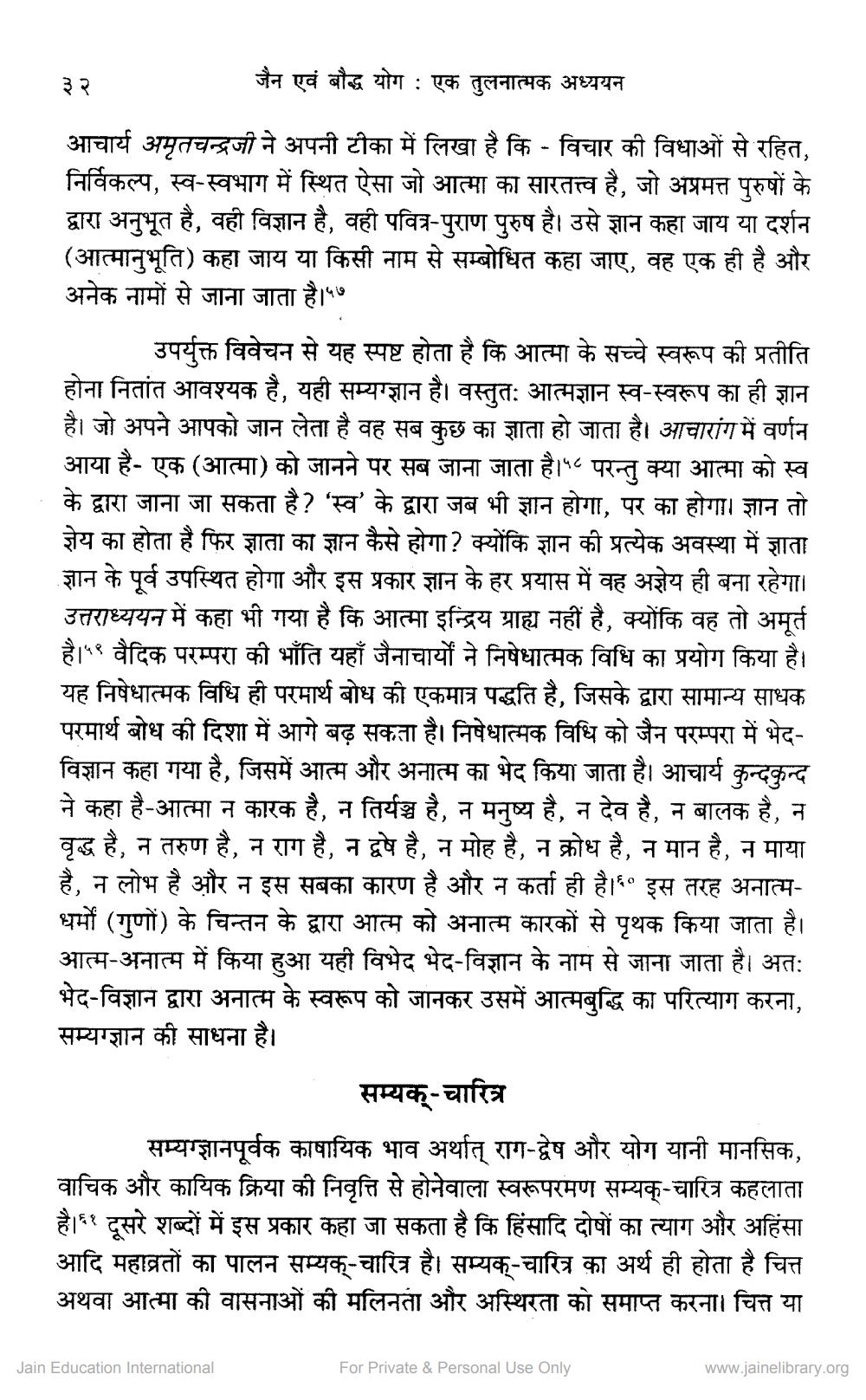________________
३२
जैन एवं बौद्ध योग : एक तुलनात्मक अध्ययन
आचार्य अमृतचन्द्रजी ने अपनी टीका में लिखा है कि - विचार की विधाओं से रहित, निर्विकल्प, स्व-स्वभाग में स्थित ऐसा जो आत्मा का सारतत्त्व है, जो अप्रमत्त पुरुषों के द्वारा अनुभूत है, वही विज्ञान है, वही पवित्र-पुराण पुरुष है। उसे ज्ञान कहा जाय या दर्शन (आत्मानुभूति) कहा जाय या किसी नाम से सम्बोधित कहा जाए, वह एक ही है और अनेक नामों से जाना जाता है।५७
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा के सच्चे स्वरूप की प्रतीति होना नितांत आवश्यक है, यही सम्यग्ज्ञान है। वस्तुत: आत्मज्ञान स्व-स्वरूप का ही ज्ञान है। जो अपने आपको जान लेता है वह सब कुछ का ज्ञाता हो जाता है। आचारांग में वर्णन आया है- एक (आत्मा) को जानने पर सब जाना जाता है।५८ परन्तु क्या आत्मा को स्व के द्वारा जाना जा सकता है? 'स्व' के द्वारा जब भी ज्ञान होगा, पर का होगा। ज्ञान तो ज्ञेय का होता है फिर ज्ञाता का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि ज्ञान की प्रत्येक अवस्था में ज्ञाता ज्ञान के पूर्व उपस्थित होगा और इस प्रकार ज्ञान के हर प्रयास में वह अज्ञेय ही बना रहेगा। उत्तराध्ययन में कहा भी गया है कि आत्मा इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वह तो अमूर्त है।५९ वैदिक परम्परा की भाँति यहाँ जैनाचार्यों ने निषेधात्मक विधि का प्रयोग किया है। यह निषेधात्मक विधि ही परमार्थ बोध की एकमात्र पद्धति है, जिसके द्वारा सामान्य साधक परमार्थ बोध की दिशा में आगे बढ़ सकता है। निषेधात्मक विधि को जैन परम्परा में भेदविज्ञान कहा गया है, जिसमें आत्म और अनात्म का भेद किया जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है-आत्मा न कारक है, न तिर्यञ्च है, न मनुष्य है, न देव है, न बालक है, न वृद्ध है, न तरुण है, न राग है, न द्वष है, न मोह है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है और न इस सबका कारण है और न कर्ता ही है।६० इस तरह अनात्मधर्मों (गुणों) के चिन्तन के द्वारा आत्म को अनात्म कारकों से पृथक किया जाता है। आत्म-अनात्म में किया हुआ यही विभेद भेद-विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अत: भेद-विज्ञान द्वारा अनात्म के स्वरूप को जानकर उसमें आत्मबुद्धि का परित्याग करना, सम्यग्ज्ञान की साधना है।
सम्यक्-चारित्र सम्यग्ज्ञानपूर्वक काषायिक भाव अर्थात् राग-द्वेष और योग यानी मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया की निवृत्ति से होनेवाला स्वरूपरमण सम्यक्-चारित्र कहलाता है।६१ दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंसादि दोषों का त्याग और अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन सम्यक्-चारित्र है। सम्यक्-चारित्र का अर्थ ही होता है चित्त अथवा आत्मा की वासनाओं की मलिनता और अस्थिरता को समाप्त करना। चित्त या
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org