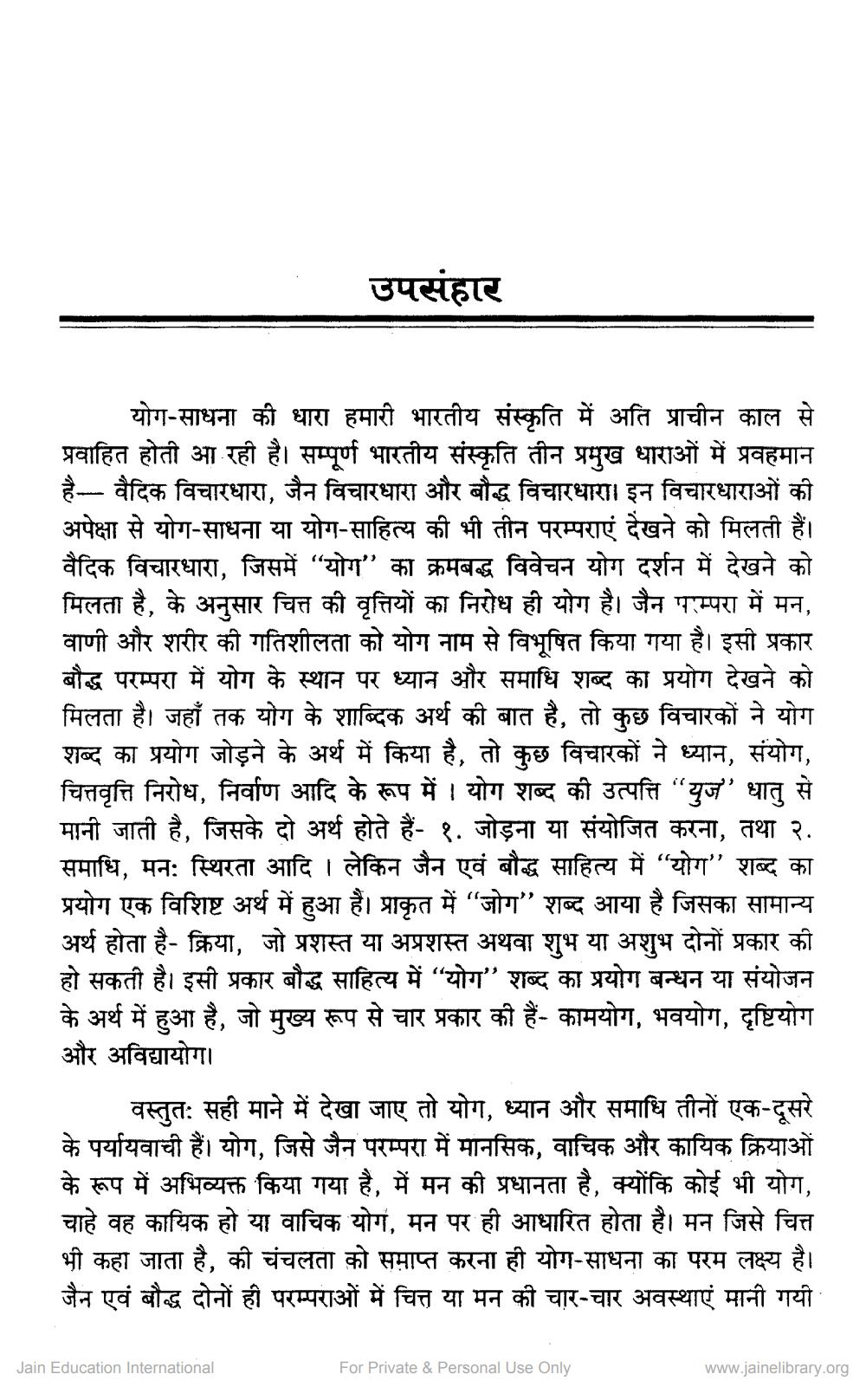________________
उपसंहार
योग-साधना की धारा हमारी भारतीय संस्कृति में अति प्राचीन काल से प्रवाहित होती आ रही है। सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति तीन प्रमुख धाराओं में प्रवहमान है— वैदिक विचारधारा, जैन विचारधारा और बौद्ध विचारधारा। इन विचारधाराओं की अपेक्षा से योग-साधना या योग - साहित्य की भी तीन परम्पराएं देखने को मिलती हैं। वैदिक विचारधारा, जिसमें "योग" का क्रमबद्ध विवेचन योग दर्शन में देखने को मिलता है, के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जैन परम्परा में मन, वाणी और शरीर की गतिशीलता को योग नाम से विभूषित किया गया है। इसी प्रकार बौद्ध परम्परा में योग के स्थान पर ध्यान और समाधि शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। जहाँ तक योग के शाब्दिक अर्थ की बात है, तो कुछ विचारकों ने योग शब्द का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में किया है, तो कुछ विचारकों ने ध्यान, संयोग, चित्तवृत्ति निरोध, निर्वाण आदि के रूप में। योग शब्द की उत्पत्ति " युज' धातु से मानी जाती है, जिसके दो अर्थ होते हैं- १. जोड़ना या संयोजित करना, तथा २. समाधि, मनः स्थिरता आदि । लेकिन जैन एवं बौद्ध साहित्य में "योग" शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में हुआ हैं । प्राकृत में "जोग” शब्द आया है जिसका सामान्य अर्थ होता है - क्रिया, जो प्रशस्त या अप्रशस्त अथवा शुभ या अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती है। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य में "योग" शब्द का प्रयोग बन्धन या संयोजन अर्थ में हुआ है, जो मुख्य रूप से चार प्रकार की हैं- कामयोग, भवयोग, दृष्टियोग और अविद्यायोग |
वस्तुतः सही माने में देखा जाए तो योग, ध्यान और समाधि तीनों एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। योग, जिसे जैन परम्परा में मानसिक, वाचिक और कायिक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, में मन की प्रधानता है, क्योंकि कोई भी योग, चाहे वह कायिक हो या वाचिक योग, मन पर ही आधारित होता है । मन जिसे चित्त भी कहा जाता है, की चंचलता को समाप्त करना ही योग-साधना का परम लक्ष्य है। जैन एवं बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में चित्त या मन की चार-चार अवस्थाएं मानी गयी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org