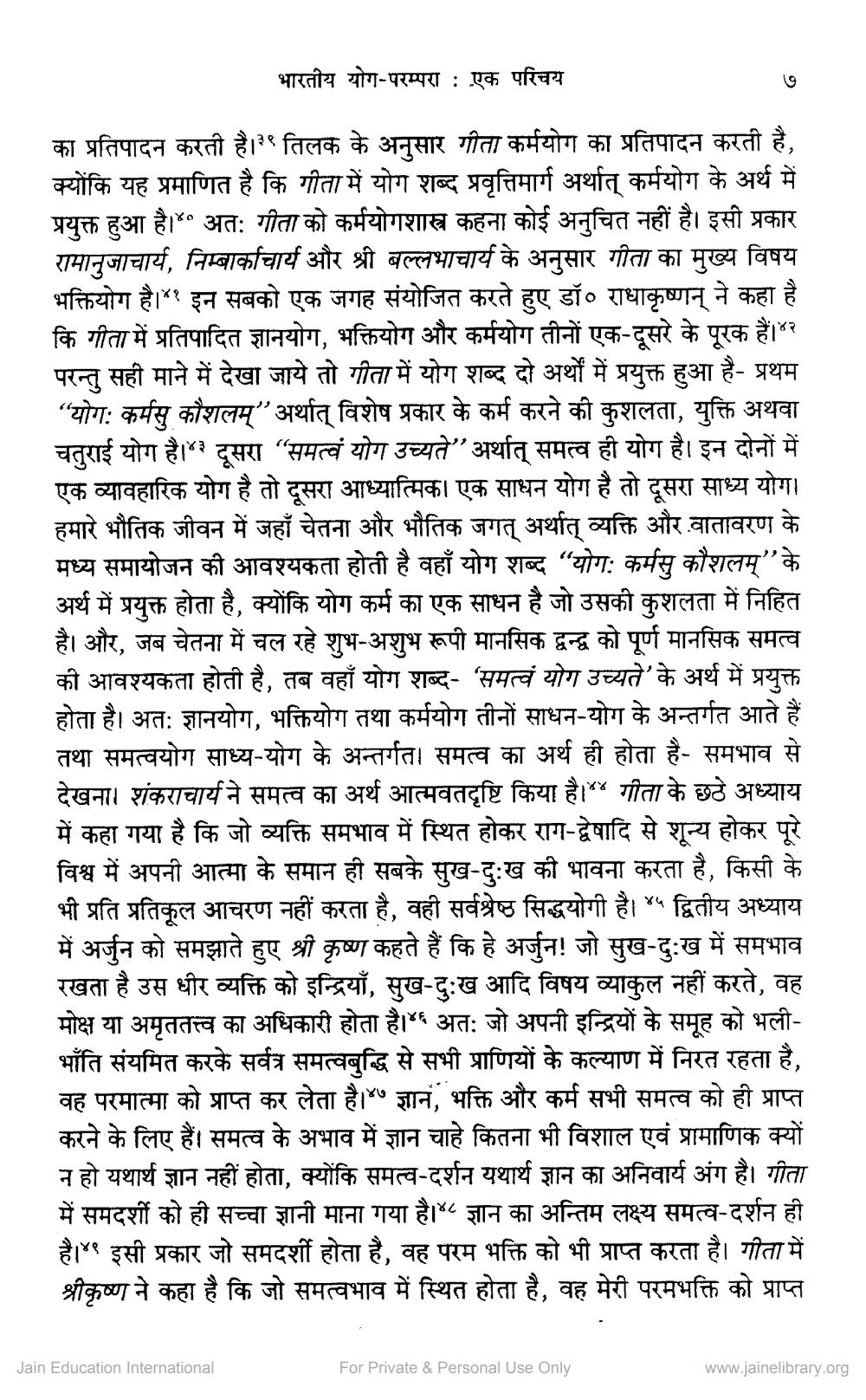________________
भारतीय योग-परम्परा : एक परिचय
का प्रतिपादन करती है।३९ तिलक के अनुसार गीता कर्मयोग का प्रतिपादन करती है, क्योंकि यह प्रमाणित है कि गीता में योग शब्द प्रवृत्तिमार्ग अर्थात् कर्मयोग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अत: गीता को कर्मयोगशास्त्र कहना कोई अनुचित नहीं है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और श्री बल्लभाचार्य के अनुसार गीता का मुख्य विषय भक्तियोग है। इन सबको एक जगह संयोजित करते हुए डॉ० राधाकृष्णन् ने कहा है कि गीता में प्रतिपादित ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं।४२ परन्तु सही माने में देखा जाये तो गीता में योग शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है- प्रथम “योग: कर्मसु कौशलम्' अर्थात् विशेष प्रकार के कर्म करने की कुशलता, युक्ति अथवा चतुराई योग है।३ दूसरा “समत्वं योग उच्यते” अर्थात् समत्व ही योग है। इन दोनों में एक व्यावहारिक योग है तो दूसरा आध्यात्मिक। एक साधन योग है तो दूसरा साध्य योग। हमारे भौतिक जीवन में जहाँ चेतना और भौतिक जगत् अर्थात् व्यक्ति और वातावरण के मध्य समायोजन की आवश्यकता होती है वहाँ योग शब्द “योग: कर्मसु कौशलम्' के अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्योंकि योग कर्म का एक साधन है जो उसकी कुशलता में निहित है। और, जब चेतना में चल रहे शुभ-अशुभ रूपी मानसिक द्वन्द्व को पूर्ण मानसिक समत्व की आवश्यकता होती है, तब वहाँ योग शब्द- 'समत्वं योग उच्यते' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अत: ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा कर्मयोग तीनों साधन-योग के अन्तर्गत आते हैं तथा समत्वयोग साध्य-योग के अन्तर्गत। समत्व का अर्थ ही होता है- समभाव से देखना। शंकराचार्य ने समत्व का अर्थ आत्मवतदृष्टि किया है।४४ गीता के छठे अध्याय में कहा गया है कि जो व्यक्ति समभाव में स्थित होकर राग-द्वेषादि से शून्य होकर पूरे विश्व में अपनी आत्मा के समान ही सबके सुख-दुःख की भावना करता है, किसी के भी प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करता है, वही सर्वश्रेष्ठ सिद्धयोगी है। ४५ द्वितीय अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन! जो सुख-दुःख में समभाव रखता है उस धीर व्यक्ति को इन्द्रियाँ, सुख-दुःख आदि विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष या अमृततत्त्व का अधिकारी होता है। ६ अत: जो अपनी इन्द्रियों के समूह को भलीभाँति संयमित करके सर्वत्र समत्वद्धि से सभी प्राणियों के कल्याण में निरत रहता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म सभी समत्व को ही प्राप्त करने के लिए हैं। समत्व के अभाव में ज्ञान चाहे कितना भी विशाल एवं प्रामाणिक क्यों न हो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि समत्व-दर्शन यथार्थ ज्ञान का अनिवार्य अंग है। गीता में समदर्शी को ही सच्चा ज्ञानी माना गया है। ८ ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य समत्व-दर्शन ही है।४९ इसी प्रकार जो समदर्शी होता है, वह परम भक्ति को भी प्राप्त करता है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि जो समत्वभाव में स्थित होता है, वह मेरी परमभक्ति को प्राप्त
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org