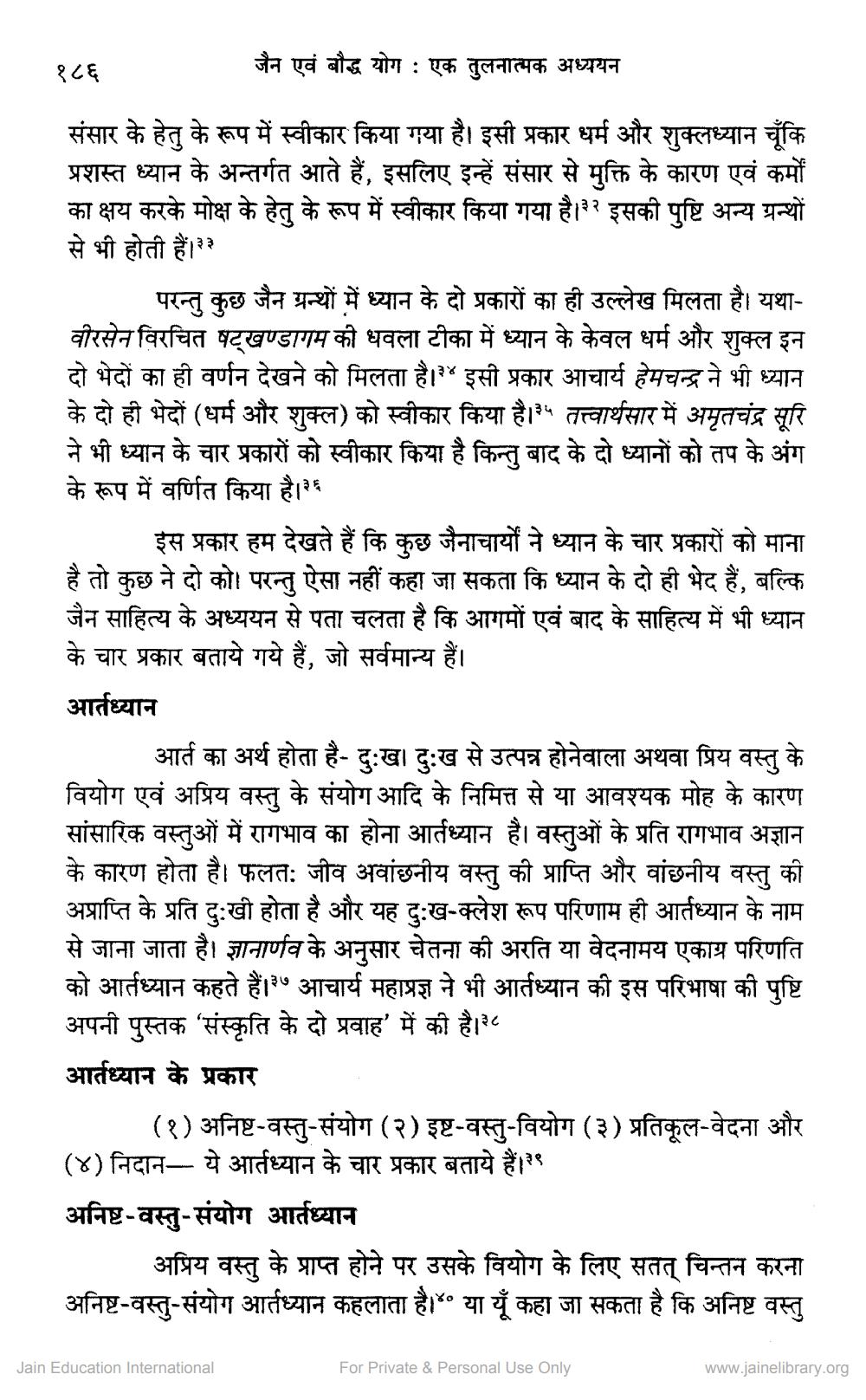________________
१८६
जैन एवं बौद्ध योग : एक तुलनात्मक अध्ययन
संसार के हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार धर्म और शुक्लध्यान चूंकि प्रशस्त ध्यान के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें संसार से मुक्ति के कारण एवं कर्मों का क्षय करके मोक्ष के हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है।३२ इसकी पुष्टि अन्य ग्रन्थों से भी होती हैं।३३
परन्तु कुछ जैन ग्रन्थों में ध्यान के दो प्रकारों का ही उल्लेख मिलता है। यथावीरसेन विरचित षट्खण्डागम की धवला टीका में ध्यान के केवल धर्म और शुक्ल इन दो भेदों का ही वर्णन देखने को मिलता है। इसी प्रकार आचार्य हेमचन्द्र ने भी ध्यान के दो ही भेदों (धर्म और शुक्ल) को स्वीकार किया है।३५ तत्त्वार्थसार में अमृतचंद्र सूरि ने भी ध्यान के चार प्रकारों को स्वीकार किया है किन्तु बाद के दो ध्यानों को तप के अंग के रूप में वर्णित किया है।२६
इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ जैनाचार्यों ने ध्यान के चार प्रकारों को माना है तो कुछ ने दो को। परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ध्यान के दो ही भेद हैं, बल्कि जैन साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि आगमों एवं बाद के साहित्य में भी ध्यान के चार प्रकार बताये गये हैं, जो सर्वमान्य हैं। आर्तध्यान
आर्त का अर्थ होता है- दुःख। दुःख से उत्पन्न होनेवाला अथवा प्रिय वस्तु के वियोग एवं अप्रिय वस्तु के संयोग आदि के निमित्त से या आवश्यक मोह के कारण सांसारिक वस्तुओं में रागभाव का होना आर्तध्यान है। वस्तुओं के प्रति रागभाव अज्ञान के कारण होता है। फलतः जीव अवांछनीय वस्तु की प्राप्ति और वांछनीय वस्तु की अप्राप्ति के प्रति दुःखी होता है और यह दु:ख-क्लेश रूप परिणाम ही आर्तध्यान के नाम से जाना जाता है। ज्ञानार्णव के अनुसार चेतना की अरति या वेदनामय एकाग्र परिणति को आर्तध्यान कहते हैं।३७ आचार्य महाप्रज्ञ ने भी आर्तध्यान की इस परिभाषा की पुष्टि अपनी पुस्तक 'संस्कृति के दो प्रवाह' में की है।२८ आर्तध्यान के प्रकार
(१) अनिष्ट-वस्तु-संयोग (२) इष्ट-वस्तु-वियोग (३) प्रतिकूल-वेदना और (४) निदान- ये आर्तध्यान के चार प्रकार बताये हैं।२९ अनिष्ट-वस्तु-संयोग आर्तध्यान
अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए सतत् चिन्तन करना अनिष्ट-वस्तु-संयोग आर्तध्यान कहलाता है। या यूँ कहा जा सकता है कि अनिष्ट वस्तु
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org