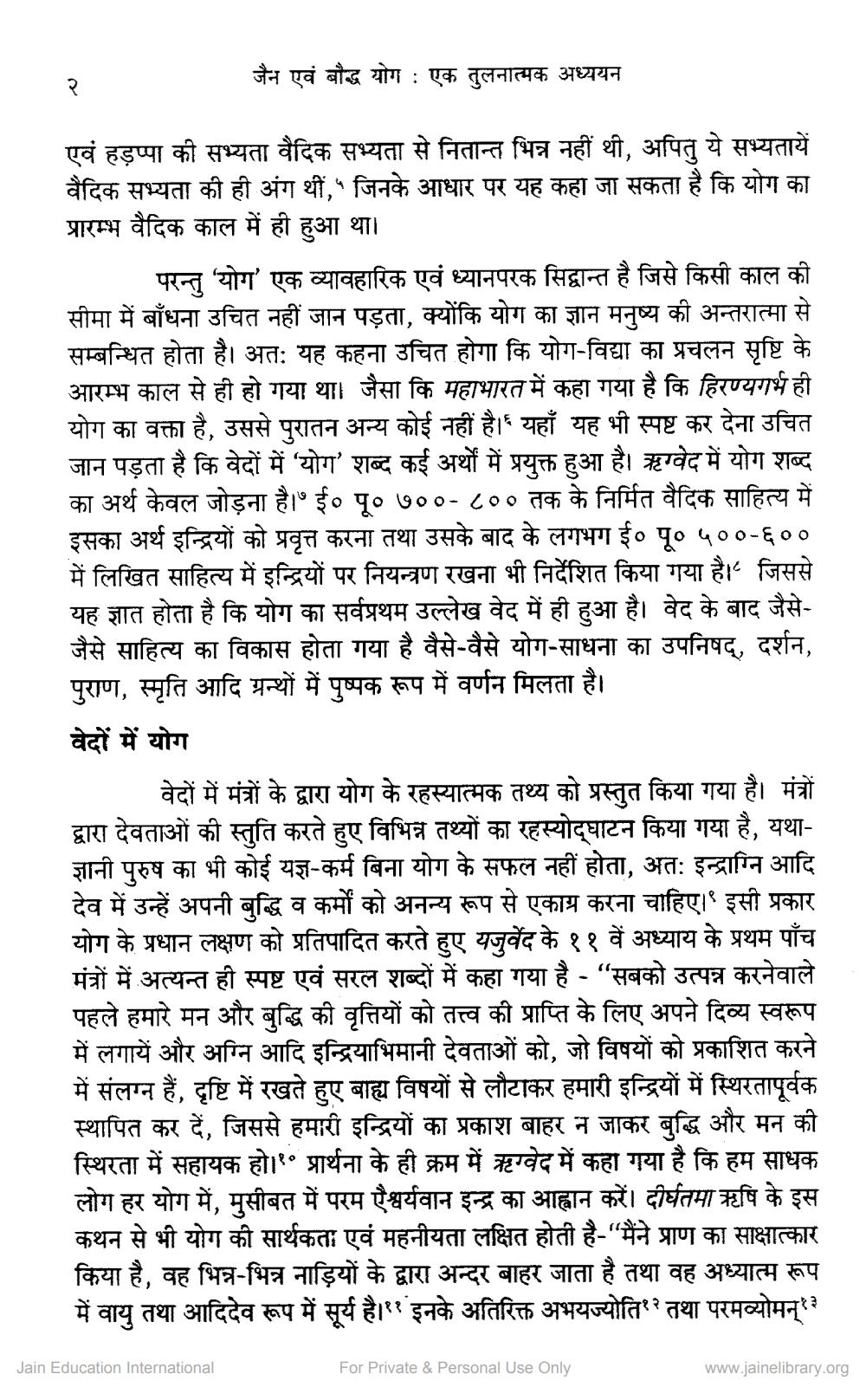________________
जैन एवं बौद्ध योग : एक तुलनात्मक अध्ययन
एवं हड़प्पा की सभ्यता वैदिक सभ्यता से नितान्त भिन्न नहीं थी, अपितु ये सभ्यतायें वैदिक सभ्यता की ही अंग थीं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि योग का प्रारम्भ वैदिक काल में ही हुआ था।
__परन्तु 'योग' एक व्यावहारिक एवं ध्यानपरक सिद्वान्त है जिसे किसी काल की सीमा में बाँधना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि योग का ज्ञान मनुष्य की अन्तरात्मा से सम्बन्धित होता है। अत: यह कहना उचित होगा कि योग-विद्या का प्रचलन सृष्टि के आरम्भ काल से ही हो गया था। जैसा कि महाभारत में कहा गया है कि हिरण्यगर्भ ही योग का वक्ता है, उससे पुरातन अन्य कोई नहीं है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उचित जान पड़ता है कि वेदों में 'योग' शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में योग शब्द का अर्थ केवल जोड़ना है। ई० पू० ७००-८०० तक के निर्मित वैदिक साहित्य में इसका अर्थ इन्द्रियों को प्रवृत्त करना तथा उसके बाद के लगभग ई० पू० ५००-६०० में लिखित साहित्य में इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना भी निर्देशित किया गया है। जिससे यह ज्ञात होता है कि योग का सर्वप्रथम उल्लेख वेद में ही हआ है। वेद के बाद जैसेजैसे साहित्य का विकास होता गया है वैसे-वैसे योग-साधना का उपनिषद्, दर्शन, पुराण, स्मृति आदि ग्रन्थों में पुष्पक रूप में वर्णन मिलता है। वेदों में योग
वेदों में मंत्रों के द्वारा योग के रहस्यात्मक तथ्य को प्रस्तुत किया गया है। मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते हुए विभिन्न तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया गया है, यथाज्ञानी पुरुष का भी कोई यज्ञ-कर्म बिना योग के सफल नहीं होता, अत: इन्द्राग्नि आदि देव में उन्हें अपनी बुद्धि व कर्मों को अनन्य रूप से एकाग्र करना चाहिए। इसी प्रकार योग के प्रधान लक्षण को प्रतिपादित करते हुए यजुर्वेद के ११ वें अध्याय के प्रथम पाँच मंत्रों में अत्यन्त ही स्पष्ट एवं सरल शब्दों में कहा गया है - "सबको उत्पन्न करनेवाले पहले हमारे मन और बुद्धि की वृत्तियों को तत्त्व की प्राप्ति के लिए अपने दिव्य स्वरूप में लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओं को, जो विषयों को प्रकाशित करने में संलग्न हैं, दृष्टि में रखते हए बाह्य विषयों से लौटाकर हमारी इन्द्रियों में स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियों का प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मन की स्थिरता में सहायक हो। प्रार्थना के ही क्रम में ऋग्वेद में कहा गया है कि हम साधक लोग हर योग में, मुसीबत में परम ऐश्वर्यवान इन्द्र का आह्वान करें। दीर्घतमा ऋषि के इस कथन से भी योग की सार्थकता एवं महनीयता लक्षित होती है-“मैंने प्राण का साक्षात्कार किया है, वह भिन्न-भिन्न नाड़ियों के द्वारा अन्दर बाहर जाता है तथा वह अध्यात्म रूप में वायु तथा आदिदेव रूप में सूर्य है।११ इनके अतिरिक्त अभयज्योति'२ तथा परमव्योमन्१३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org