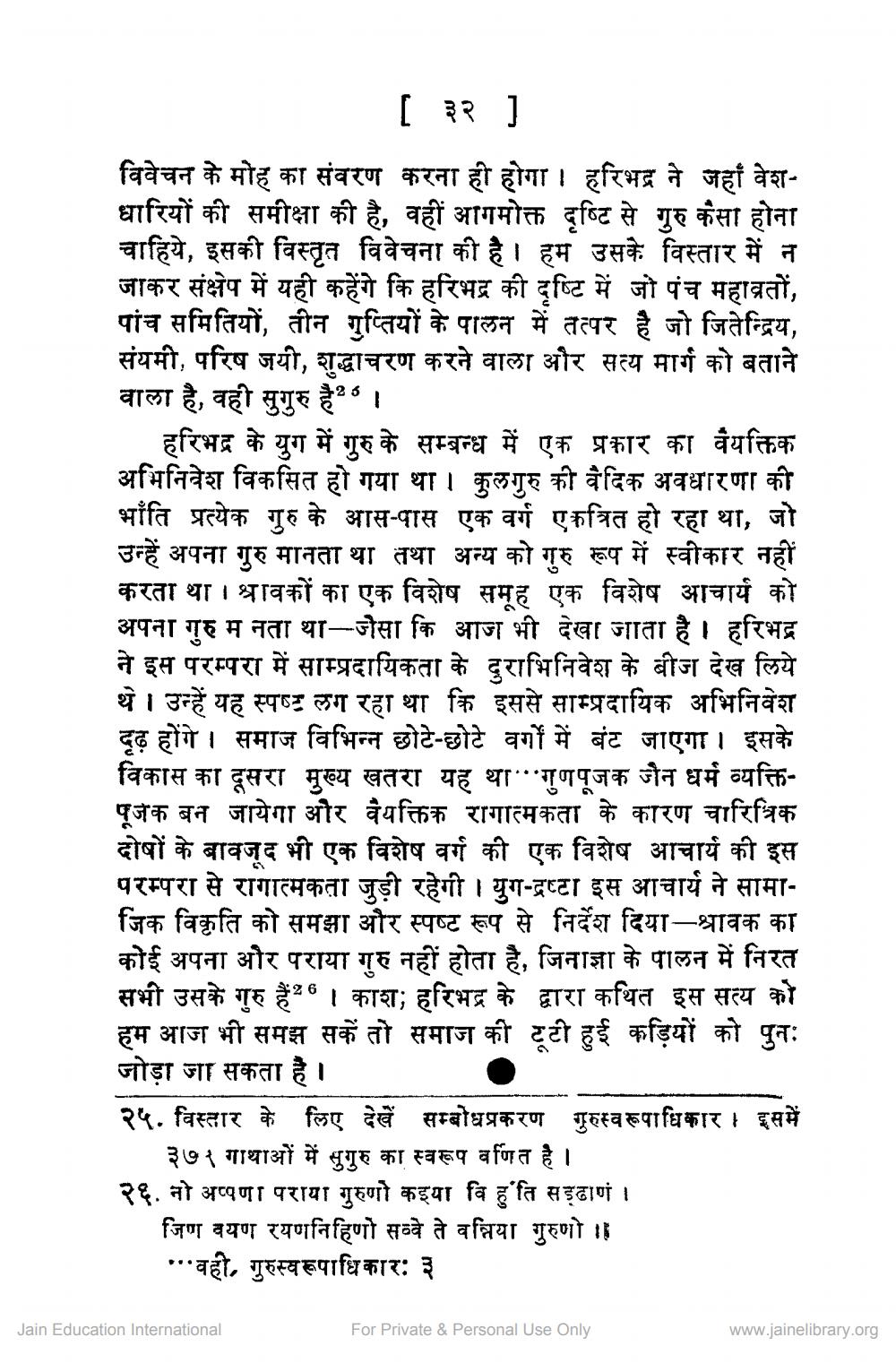________________
[ ३२ ]
विवेचन के मोह का संवरण करना ही होगा । हरिभद्र ने जहाँ वेशधारियों की समीक्षा की है, वहीं आगमोक्त दृष्टि से गुरु कैसा होना चाहिये, इसकी विस्तृत विवेचना की है। हम उसके विस्तार में न जार संक्षेप में यही कहेंगे कि हरिभद्र की दृष्टि में जो पंच महाव्रतों, पांच समितियों, तीन गुप्तियों के पालन में तत्पर है जो जितेन्द्रिय, संयमी, परिष जयी, शुद्धाचरण करने वाला और सत्य मार्ग को बताने वाला है, वही सुगुरु है " ।
26
हरिभद्र के युग में गुरु के सम्बन्ध में एक प्रकार का वैयक्तिक अभिनिवेश विकसित हो गया था। कुलगुरु की वैदिक अवधारणा की भाँति प्रत्येक गुरु के आस-पास एक वर्ग एकत्रित हो रहा था, जो उन्हें अपना गुरु मानता था तथा अन्य को गुरु रूप में स्वीकार नहीं करता था । श्रावकों का एक विशेष समूह एक विशेष आचार्य को अपना गुरु मनता था - जैसा कि आज भी देखा जाता है । हरिभद्र ने इस परम्परा में साम्प्रदायिकता के दुराभिनिवेश के बीज देख लिये थे । उन्हें यह स्पष्ट लग रहा था कि इससे साम्प्रदायिक अभिनिवेश दृढ़ होंगे । समाज विभिन्न छोटे-छोटे वर्गों में बंट जाएगा । इसके विकास का दूसरा मुख्य खतरा यह था गुणपूजक जैन धर्म व्यक्तिपूजक बन जायेगा और वैयक्तिक रागात्मकता के कारण चारित्रिक दोषों के बावजूद भी एक विशेष वर्ग की एक विशेष आचार्य की इस परम्परा से रागात्मकता जुड़ी रहेगी । युग-द्रष्टा इस आचार्य ने सामाजिक विकृति को समझा और स्पष्ट रूप से निर्देश दिया - श्रावक का कोई अपना और पराया गुरु नहीं होता है, जिनाज्ञा के पालन में निरत सभी उसके गुरु हैं । काश; हरिभद्र के द्वारा कथित इस सत्य को हम आज भी समझ सकें तो समाज की टूटी हुई कड़ियों को पुनः जोड़ा जा सकता है ।
२५. विस्तार के लिए देखें सम्बोधप्रकरण गुरुस्वरूपाधिकार । इसमें ३७ २ गाथाओं में सुगुरु का स्वरूप वर्णित है ।
२६. नो अपना पराया गुरुणो कइया विहुति सड्ढाणं ।
जिण वयण रयणनिहिणो सव्वे ते वन्निया गुरुणो | ...वही, गुरुस्वरूपाधिकारः ३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org