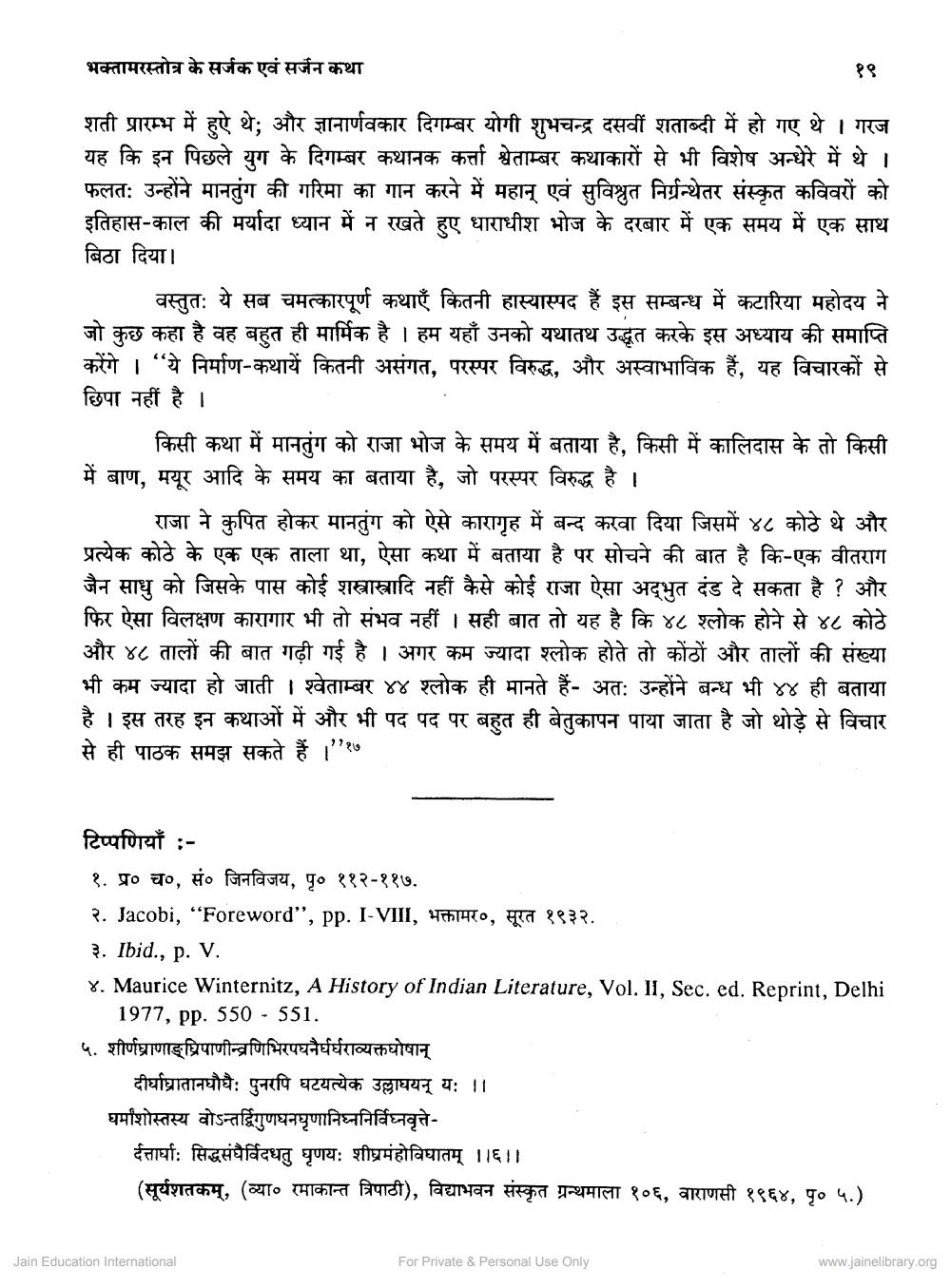________________
भक्तामरस्तोत्र के सर्जक एवं सर्जन कथा
१
शती प्रारम्भ में हुऐ थे; और ज्ञानार्णवकार दिगम्बर योगी शुभचन्द्र दसवीं शताब्दी में हो गए थे । गरज यह कि इन पिछले युग के दिगम्बर कथानक कर्ता श्वेताम्बर कथाकारों से भी विशेष अन्धेरे में थे । फलत: उन्होंने मानतुंग की गरिमा का गान करने में महान् एवं सुविश्रुत निर्ग्रन्थेतर संस्कृत कविवरों को इतिहास-काल की मर्यादा ध्यान में न रखते हुए धाराधीश भोज के दरबार में एक समय में एक साथ बिठा दिया।
वस्तुत: ये सब चमत्कारपूर्ण कथाएँ कितनी हास्यास्पद हैं इस सम्बन्ध में कटारिया महोदय ने जो कुछ कहा है वह बहुत ही मार्मिक है । हम यहाँ उनको यथातथ उद्धृत करके इस अध्याय की समाप्ति करेंगे । “ये निर्माण-कथायें कितनी असंगत, परस्पर विरुद्ध, और अस्वाभाविक हैं, यह विचारकों से छिपा नहीं है ।
किसी कथा में मानतुंग को राजा भोज के समय में बताया है, किसी में कालिदास के तो किसी में बाण, मयूर आदि के समय का बताया है, जो परस्पर विरुद्ध है ।।
राजा ने कुपित होकर मानतुंग को ऐसे कारागृह में बन्द करवा दिया जिसमें ४८ कोठे थे और प्रत्येक कोठे के एक एक ताला था, ऐसा कथा में बताया है पर सोचने की बात है कि-एक वीतराग जैन साधु को जिसके पास कोई शस्त्रास्त्रादि नहीं कैसे कोई राजा ऐसा अद्भुत दंड दे सकता है ? और फिर ऐसा विलक्षण कारागार भी तो संभव नहीं । सही बात तो यह है कि ४८ श्लोक होने से ४८ कोठे
और ४८ तालों की बात गढ़ी गई है । अगर कम ज्यादा श्लोक होते तो कोंठों और तालों की संख्या भी कम ज्यादा हो जाती । श्वेताम्बर ४४ श्लोक ही मानते हैं- अत: उन्होंने बन्ध भी ४४ ही बताया है । इस तरह इन कथाओं में और भी पद पद पर बहुत ही बेतुकापन पाया जाता है जो थोड़े से विचार से ही पाठक समझ सकते हैं ।' १७
टिप्पणियाँ :१. प्र० च०, सं० जिनविजय, पृ० ११२-११७. २. Jacobi, "Foreword", pp. I-VIII, भक्तामर०, सूरत १९३२. ३. Ibid., p. V. ४. Maurice Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. II, Sec. ed. Reprint, Delhi
__1977, pp. 550 - 551. ५. शीर्णघ्राणाध्रिपाणीन्द्रणिभिरपघनैर्घघराव्यक्तघोषान्
दीर्घाघ्रातानघौधैः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन् यः ।। धर्मांशोस्तस्य वोऽन्तर्द्विगुणघनघृणानिघ्ननिर्विघ्नवृत्ते
दत्तार्घा: सिद्धसंधैर्विदधतु घृणयः शीघ्रमहोविघातम् ।।६।। (सूर्यशतकम्, (व्या० रमाकान्त त्रिपाठी), विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला १०६, वाराणसी १९६४, पृ० ५.)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org