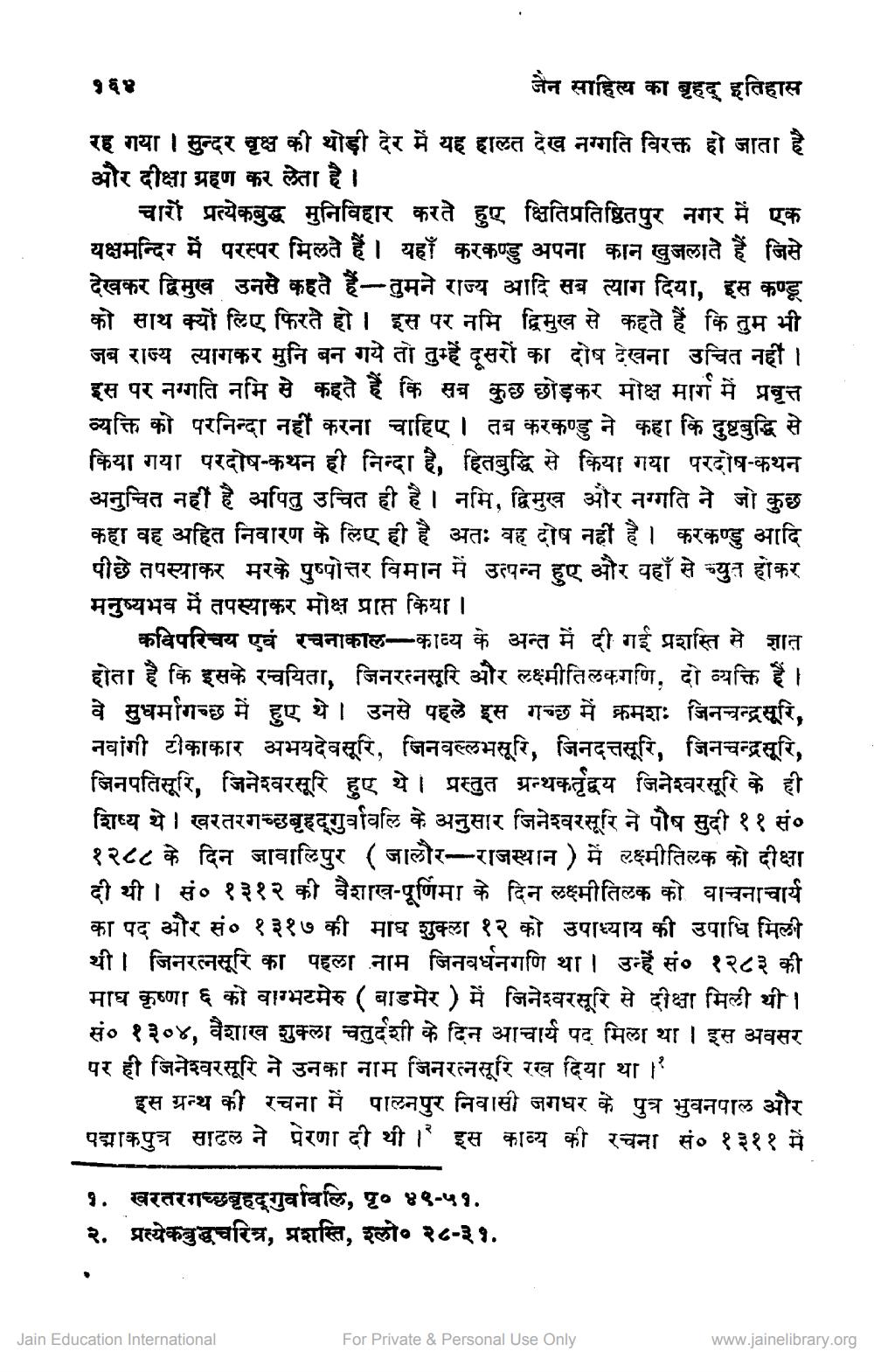________________
१६४
जैन साहित्य का बृहद् इतिहास
रह गया । सुन्दर वृक्ष की थोड़ी देर में यह हालत देख नग्गति विरक्त हो जाता है। और दीक्षा ग्रहण कर लेता है ।
चारों प्रत्येकबुद्ध मुनिविहार करते हुए क्षितिप्रतिष्ठितपुर नगर में एक यक्षमन्दिर में परस्पर मिलते हैं । यहाँ करकण्डु अपना कान खुजलाते हैं जिसे देखकर द्विमुख उनसे कहते हैं - तुमने राज्य आदि सब त्याग दिया, इस कण्डू को साथ क्यों लिए फिरते हो । इस पर नमि द्विमुख से कहते हैं कि तुम भी जब राज्य त्यागकर मुनि बन गये तो तुम्हें दूसरों का दोष देखना उचित नहीं । इस पर नग्गति नमि से कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति को परनिन्दा नहीं करना चाहिए तब करकण्डु ने कहा कि दुष्टबुद्धि से किया गया परदोष कथन ही निन्दा है, हितबुद्धि से किया गया परदोष कथन अनुचित नहीं है अपितु उचित ही है नमि, द्विमुख और नग्गति ने जो कुछ कहा वह अहित निवारण के लिए ही है अतः वह दोष नहीं है । करकण्डु आदि पीछे तपस्याकर मरके पुष्पोत्तर विमान में उत्पन्न हुए और वहाँ से च्युत होकर मनुष्यभव में तपस्याकर मोक्ष प्राप्त किया ।
।
।
कविपरिचय एवं रचनाकाल - काव्य के अन्त में दी गई प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इसके रचयिता, जिनरत्नसूरि और लक्ष्मीतिलकगणि, दो व्यक्ति हैं । वे सुधर्मागच्छ में हुए थे । उनसे पहले इस गच्छ में क्रमशः जिनचन्द्रसूरि, नवांगी टीकाकार अभयदेवसूरि, जिनवल्लभसूरि, जिनदत्तसूरि, जिनचन्द्रसूरि, जिन पतिसूरि, जिनेश्वरसूरि हुए थे । प्रस्तुत ग्रन्थकर्तृद्वय जिनेश्वरसूरि के ही शिष्य थे । खरतरगच्छबृहद्गुर्वावलि के अनुसार जिनेश्वरसूरि ने पौष सुदी ११ सं० १२८८ के दिन जावालिपुर ( जालौर - राजस्थान ) में लक्ष्मीतिलक को दीक्षा दी थी । सं० १३१२ की वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मीतिलक को वाचनाचार्य का पद और सं० १३१७ की माघ शुक्ला १२ को उपाध्याय की उपाधि मिली थी। जिनरत्नसूरि का पहला नाम जिनवर्धन गणि था । उन्हें सं० १२८३ की माघ कृष्णा ६ को वाग्भटमेरु ( बाडमेर ) में जिनेश्वरसूरि से दीक्षा मिली थी । सं० १३०४, वैशाख शुक्ला चतुर्दशी के दिन आचार्य पद मिला था । इस अवसर पर ही जिनेश्वरसूरि ने उनका नाम जिनरत्नसूरि रख दिया था । '
इस ग्रन्थ की रचना में पालनपुर निवासी जगधर के पुत्र भुवनपाल और पद्मा पुत्र साढल ने प्रेरणा दी थी । इस काव्य की रचना सं० १३११ में
१. खरतरगच्छबृहद्गुर्वावलि, पृ० ४९-५१.
२. प्रत्येकबुद्धचरित्र, प्रशस्ति, इलो० २८-३१.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org