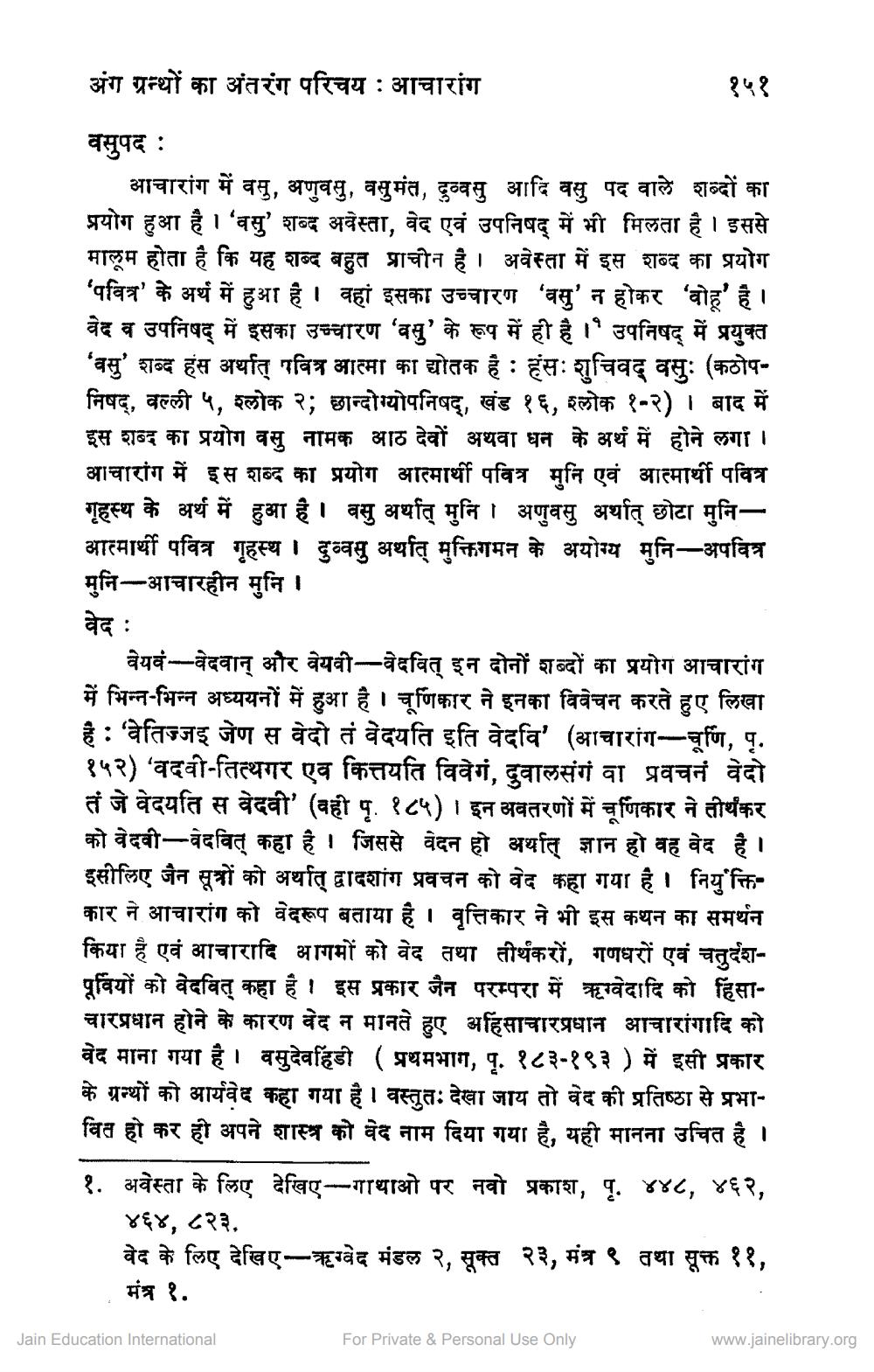________________
अंग ग्रन्थों का अंतरंग परिचय: आचारांग
वसुपद :
आचारांग में वसु, अणुवसु, वसुमंत, दुव्वसु आदि वसु पद वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है । 'वसु' शब्द अवेस्ता, वेद एवं उपनिषद् में भी मिलता है । इससे मालूम होता है कि यह शब्द बहुत प्राचीन है । अवेस्ता में इस शब्द का प्रयोग 'पवित्र' के अर्थ में हुआ है। वहां इसका उच्चारण 'वसु' न होकर 'वोहू' है । वेद व उपनिषद् में इसका उच्चारण 'वसु' के रूप में ही है ।' उपनिषद् में प्रयुक्त 'वसु' शब्द हंस अर्थात् पवित्र आत्मा का द्योतक है : हंसः शुचिवद् वसुः (कठोपनिषद्, वल्ली ५, श्लोक २; छान्दोग्योपनिषद्, खंड १६, श्लोक १-२ ) । बाद में इस शब्द का प्रयोग वसु नामक आठ देवों अथवा धन के अर्थ में होने लगा । आचारांग में इस शब्द का प्रयोग आत्मार्थी पवित्र मुनि एवं आत्मार्थी पवित्र गृहस्थ के अर्थ में हुआ है । वसु अर्थात् मुनि । अणुवसु अर्थात् छोटा मुनिआत्मार्थी पवित्र गृहस्थ । दुब्वसु अर्थात् मुक्तिगमन के अयोग्य मुनि - अपवित्र मुनि - आचारहीन मुनि ।
वेद :
वेrवं - वेदवान् और वेयवी - वेदवित् इन दोनों शब्दों का प्रयोग आचारांग में भिन्न-भिन्न अध्ययनों में हुआ है । चूर्णिकार ने इनका विवेचन करते हुए लिखा है : 'वेतिज्जइ जेण स वेदो तं वेदयति इति वेदवि' (आचारांग - चूर्णि, पृ. १५२) 'वदवी - तित्थगर एव कित्तयति विवेगं, दुवालसंगं वा प्रवचनं वेदो तं जे वेदयति स वेदवी' ( वही पृ. १८५) । इन अवतरणों में चूर्णिकार ने तीर्थंकर को वेदवी - वेदवित् कहा है । जिससे वेदन हो अर्थात् ज्ञान हो वह वेद है । इसीलिए जैन सूत्रों को अर्थात् द्वादशांग प्रवचन को वेद कहा गया है । नियुक्तिकार ने आचारांग को वेदरूप बताया है । वृत्तिकार ने भी इस कथन का समर्थन किया है एवं आचारादि आगमों को वेद तथा तीर्थंकरों, गणधरों एवं चतुर्दशपूर्वियों को वेदवित् कहा है। इस प्रकार जैन परम्परा में ऋग्वेदादि को हिंसाचारप्रधान होने के कारण वेद न मानते हुए अहिंसाचारप्रधान आचारांगादि को वेद माना गया है । वसुदेवहिडी ( प्रथमभाग, पृ. १८३-१९३ ) में इसी प्रकार के ग्रन्थों को आर्यवेद कहा गया है । वस्तुतः देखा जाय तो वेद की प्रतिष्ठा से प्रभावित हो कर ही अपने शास्त्र को वेद नाम दिया गया है, यही मानना उचित है ।
१. अवेस्ता के लिए देखिए -- गाथाओ पर नवो प्रकाश, पृ. ४४८, ४६२,
४६४, ८२३.
वेद के लिए देखिए ॠग्वेद मंडल २, सूक्त २३, मंत्र ९ तथा सूक्त ११,
मंत्र १.
Jain Education International
१५१
-
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org