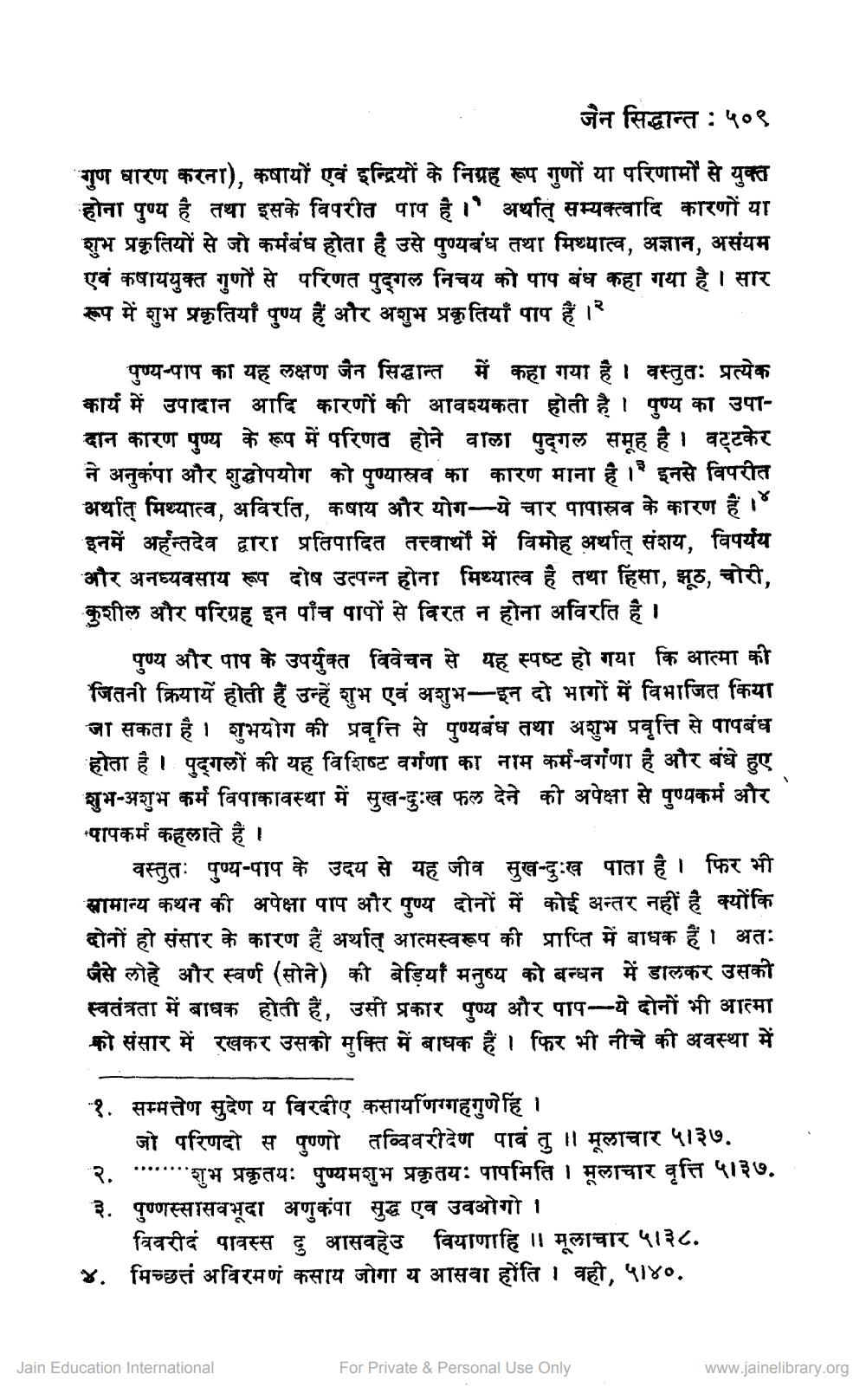________________
जैन सिद्धान्त : ५०९ गुण धारण करना), कषायों एवं इन्द्रियों के निग्रह रूप गुणों या परिणामों से युक्त होना पुण्य है तथा इसके विपरीत पाप है।' अर्थात् सम्यक्त्वादि कारणों या शुभ प्रकृतियों से जो कर्मबंध होता है उसे पुण्यबंध तथा मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम एवं कषाययुक्त गुणों से परिणत पुद्गल निचय को पाप बंध कहा गया है । सार रूप में शुभ प्रकृतियाँ पुण्य हैं और अशुभ प्रकृतियाँ पाप हैं ।
पुण्य-पाप का यह लक्षण जैन सिद्धान्त में कहा गया है। वस्तुतः प्रत्येक कार्य में उपादान आदि कारणों की आवश्यकता होती है। पुण्य का उपादान कारण पुण्य के रूप में परिणत होने वाला पुद्गल समूह है। वट्टकेर ने अनुकंपा और शुद्धोपयोग को पुण्यास्रव का कारण माना है। इनसे विपरीत अर्थात् मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग-ये चार पापास्रव के कारण हैं। इनमें अर्हन्तदेव द्वारा प्रतिपादित तत्त्वार्थों में विमोह अर्थात् संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रूप दोष उत्पन्न होना मिथ्यात्व है तथा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच पापों से विरत न होना अविरति है।
पुण्य और पाप के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा की जितनी क्रियायें होती हैं उन्हें शुभ एवं अशुभ-इन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। शुभयोग की प्रवृत्ति से पुण्यबंध तथा अशुभ प्रवृत्ति से पापबंध होता है। पुद्गलों की यह विशिष्ट वर्गणा का नाम कर्म-वर्गणा है और बंधे हुए शुभ-अशुभ कर्म विपाकावस्था में सुख-दुःख फल देने की अपेक्षा से पुण्यकर्म और 'पापकर्म कहलाते हैं।
वस्तुतः पुण्य-पाप के उदय से यह जीव सुख-दुःख पाता है। फिर भी सामान्य कथन की अपेक्षा पाप और पुण्य दोनों में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों हो संसार के कारण हैं अर्थात् आत्मस्वरूप की प्राप्ति में बाधक हैं । अतः जैसे लोहे और स्वर्ण (सोने) की बेड़ियां मनुष्य को बन्धन में डालकर उसकी स्वतंत्रता में बाधक होती हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप-ये दोनों भी आत्मा को संसार में रखकर उसको मुक्ति में बाधक हैं। फिर भी नीचे की अवस्था में
१. सम्मत्तेण सुदेण य विरदीए कसाणिग्गहगुणेहिं ।
जो परिणदो स पुण्णो तब्दिवरीदेण पावं तु ।। मूलाचार ५।३७. २. ...... शुभ प्रकृतयः पुण्यमशुभ प्रकृतयः पापमिति । मूलाचार वृत्ति ५।३७. ३. पुण्णस्सासवभूदा अणुकंपा सुद्ध एव उवओगो।
विवरीदं पावस्स दु आसवहेउ वियाणाहि ।। मूलाचार ५।३८. ४. मिच्छत्तं अविरमणं कसाय जोगा य आसवा होति । वही, ५४४०.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org