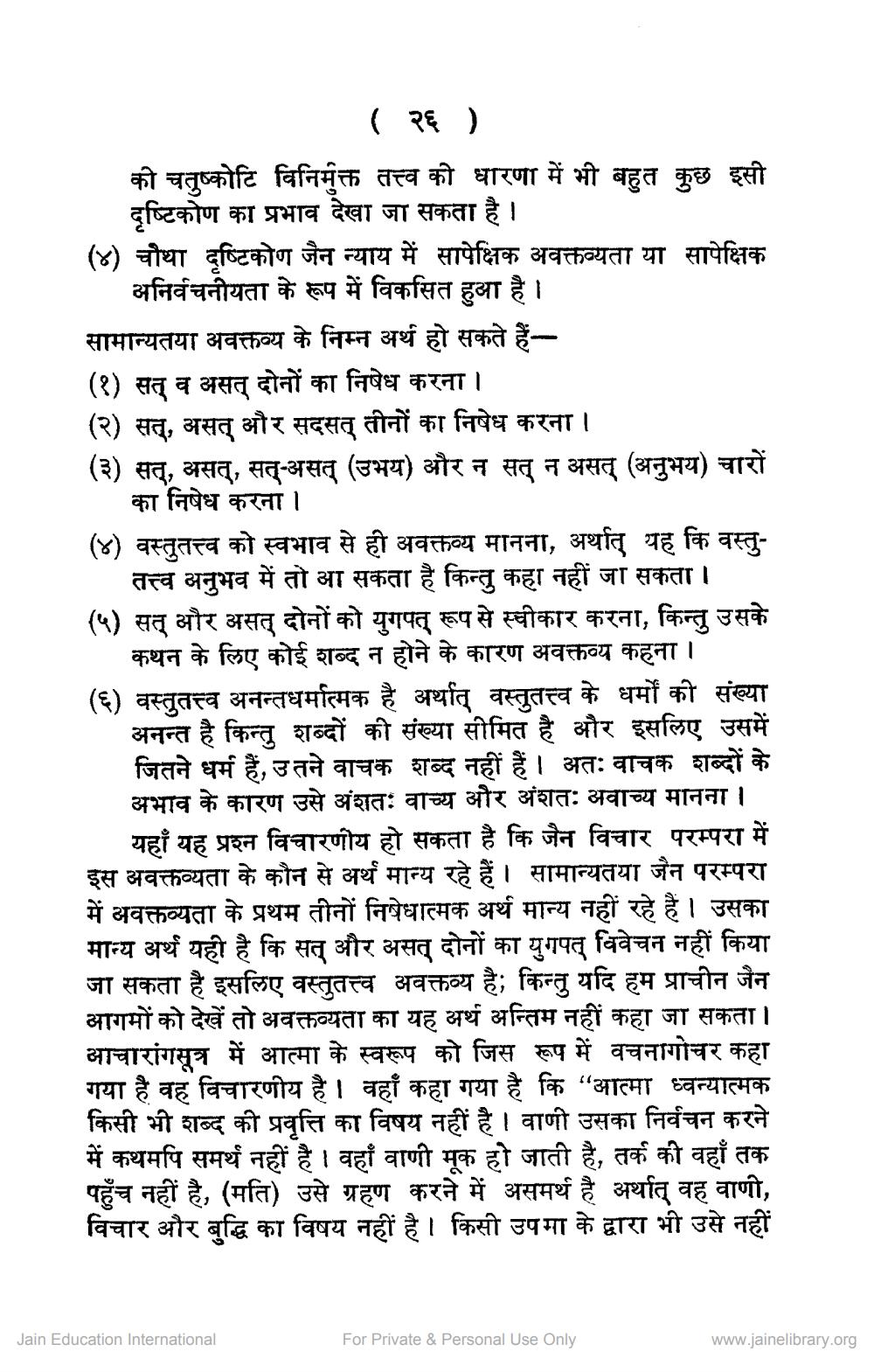________________
( २६ ) की चतुष्कोटि विनिर्मुक्त तत्त्व को धारणा में भी बहुत कुछ इसी
दृष्टिकोण का प्रभाव देखा जा सकता है। (४) चौथा दृष्टिकोण जैन न्याय में सापेक्षिक अवक्तव्यता या सापेक्षिक
अनिर्वचनीयता के रूप में विकसित हुआ है। सामान्यतया अवक्तव्य के निम्न अर्थ हो सकते हैं(१) सत् व असत् दोनों का निषेध करना। (२) सत्, असत् और सदसत् तीनों का निषेध करना । (३) सत्, असत्, सत्-असत् (उभय) और न सत् न असत् (अनुभय) चारों
का निषेध करना। (४) वस्तुतत्त्व को स्वभाव से ही अवक्तव्य मानना, अर्थात् यह कि वस्तु
तत्त्व अनुभव में तो आ सकता है किन्तु कहा नहीं जा सकता। (५) सत् और असत् दोनों को युगपत् रूप से स्वीकार करना, किन्तु उसके
कथन के लिए कोई शब्द न होने के कारण अवक्तव्य कहना । (६) वस्तुतत्त्व अनन्तधर्मात्मक है अर्थात् वस्तुतत्त्व के धर्मों की संख्या
अनन्त है किन्तु शब्दों की संख्या सीमित है और इसलिए उसमें जितने धर्म हैं, उतने वाचक शब्द नहीं हैं। अतः वाचक शब्दों के अभाव के कारण उसे अंशतः वाच्य और अंशतः अवाच्य मानना ।
यहाँ यह प्रश्न विचारणीय हो सकता है कि जैन विचार परम्परा में इस अवक्तव्यता के कौन से अर्थ मान्य रहे हैं। सामान्यतया जैन परम्परा में अवक्तव्यता के प्रथम तीनों निषेधात्मक अर्थ मान्य नहीं रहे हैं। उसका मान्य अर्थ यही है कि सत और असत् दोनों का युगपत् विवेचन नहीं किया जा सकता है इसलिए वस्तुतत्त्व अवक्तव्य है; किन्तु यदि हम प्राचीन जैन आगमों को देखें तो अवक्तव्यता का यह अर्थ अन्तिम नहीं कहा जा सकता। आचारांगसूत्र में आत्मा के स्वरूप को जिस रूप में वचनागोचर कहा गया है वह विचारणीय है। वहाँ कहा गया है कि "आत्मा ध्वन्यात्मक किसी भी शब्द की प्रवृत्ति का विषय नहीं है । वाणी उसका निर्वचन करने में कथमपि समर्थ नहीं है। वहाँ वाणी मूक हो जाती है, तर्क की वहाँ तक पहुँच नहीं है, (मति) उसे ग्रहण करने में असमर्थ है अर्थात् वह वाणी, विचार और बुद्धि का विषय नहीं है। किसी उपमा के द्वारा भी उसे नहीं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org