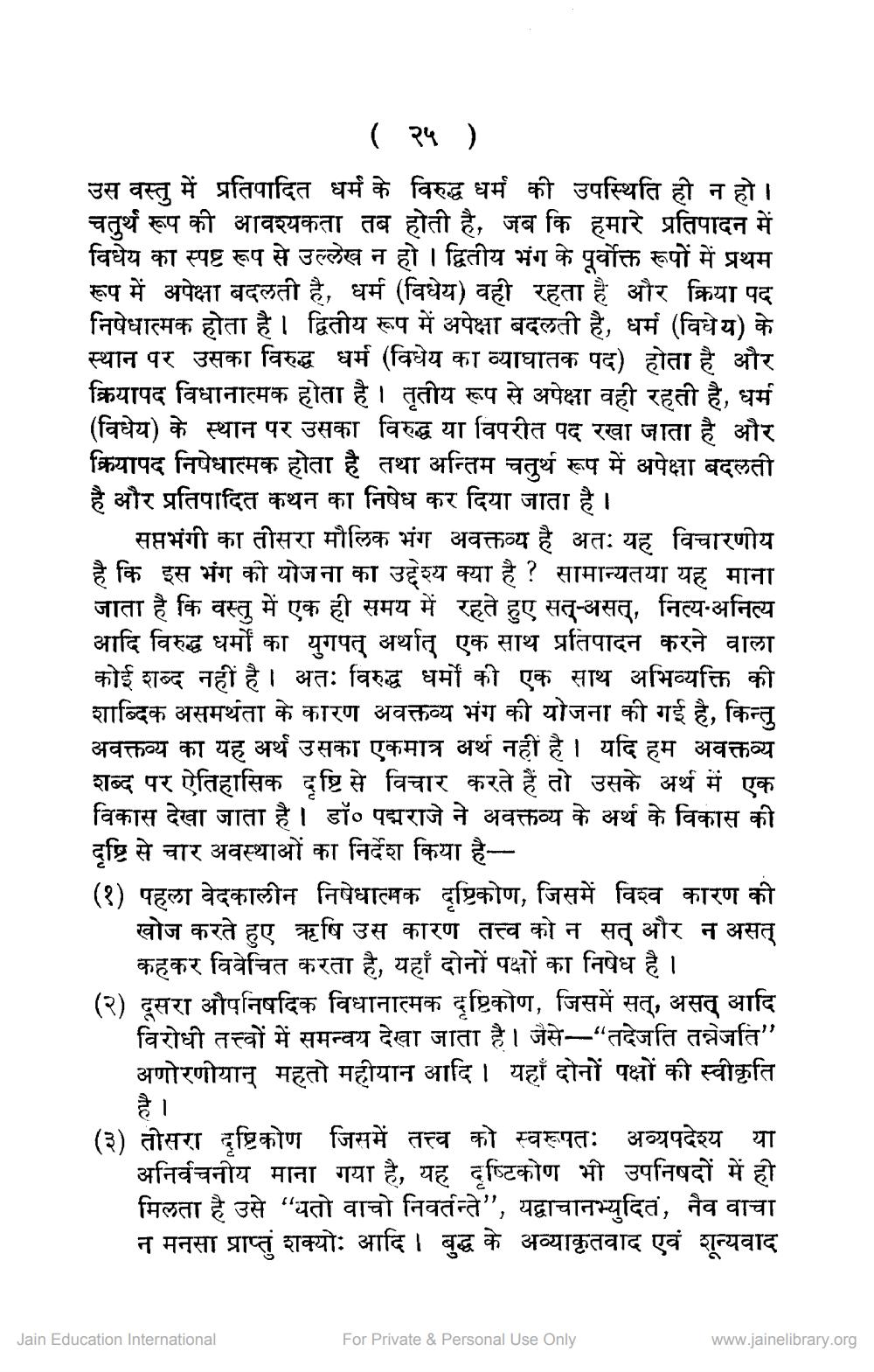________________
( २५ ) उस वस्तु में प्रतिपादित धर्म के विरुद्ध धर्म की उपस्थिति हो न हो। चतुर्थ रूप की आवश्यकता तब होती है, जब कि हमारे प्रतिपादन में विधेय का स्पष्ट रूप से उल्लेख न हो । द्वितीय भंग के पूर्वोक्त रूपों में प्रथम रूप में अपेक्षा बदलती है, धर्म (विधेय) वही रहता है और क्रिया पद निषेधात्मक होता है। द्वितीय रूप में अपेक्षा बदलती है, धर्म (विधेय) के स्थान पर उसका विरुद्ध धर्म (विधेय का व्याघातक पद) होता है और क्रियापद विधानात्मक होता है। तृतीय रूप से अपेक्षा वही रहती है, धर्म (विधेय) के स्थान पर उसका विरुद्ध या विपरीत पद रखा जाता है और क्रियापद निषेधात्मक होता है तथा अन्तिम चतुर्थ रूप में अपेक्षा बदलती है और प्रतिपादित कथन का निषेध कर दिया जाता है।
सप्तभंगी का तीसरा मौलिक भंग अवक्तव्य है अतः यह विचारणीय है कि इस भंग की योजना का उद्देश्य क्या है ? सामान्यतया यह माना जाता है कि वस्तु में एक ही समय में रहते हुए सत्-असत्, नित्य-अनित्य आदि विरुद्ध धर्मों का युगपत् अर्थात् एक साथ प्रतिपादन करने वाला कोई शब्द नहीं है। अतः विरुद्ध धर्मों की एक साथ अभिव्यक्ति की शाब्दिक असमर्थता के कारण अवक्तव्य भंग की योजना की गई है, किन्तु अवक्तव्य का यह अर्थ उसका एकमात्र अर्थ नहीं है। यदि हम अवक्तव्य शब्द पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हैं तो उसके अर्थ में एक विकास देखा जाता है। डॉ० पद्मराजे ने अवक्तव्य के अर्थ के विकास की दृष्टि से चार अवस्थाओं का निर्देश किया है(१) पहला वेदकालीन निषेधात्मक दृष्टिकोण, जिसमें विश्व कारण की
खोज करते हुए ऋषि उस कारण तत्त्व को न सत् और न असत् __ कहकर विवेचित करता है, यहाँ दोनों पक्षों का निषेध है। (२) दूसरा औपनिषदिक विधानात्मक दृष्टिकोण, जिसमें सत्, असत् आदि
विरोधी तत्त्वों में समन्वय देखा जाता है। जैसे-"तदेजति तन्नेजति" अणोरणीयान् महतो महीयान आदि। यहाँ दोनों पक्षों की स्वीकृति
(३) तीसरा दृष्टिकोण जिसमें तत्त्व को स्वरूपतः अव्यपदेश्य या
अनिर्वचनीय माना गया है, यह दृष्टिकोण भी उपनिषदों में ही मिलता है उसे "तो वाचो निवर्तन्ते", यद्वाचानभ्युदितं, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्योः आदि । बुद्ध के अव्याकृतवाद एवं शून्यवाद
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org