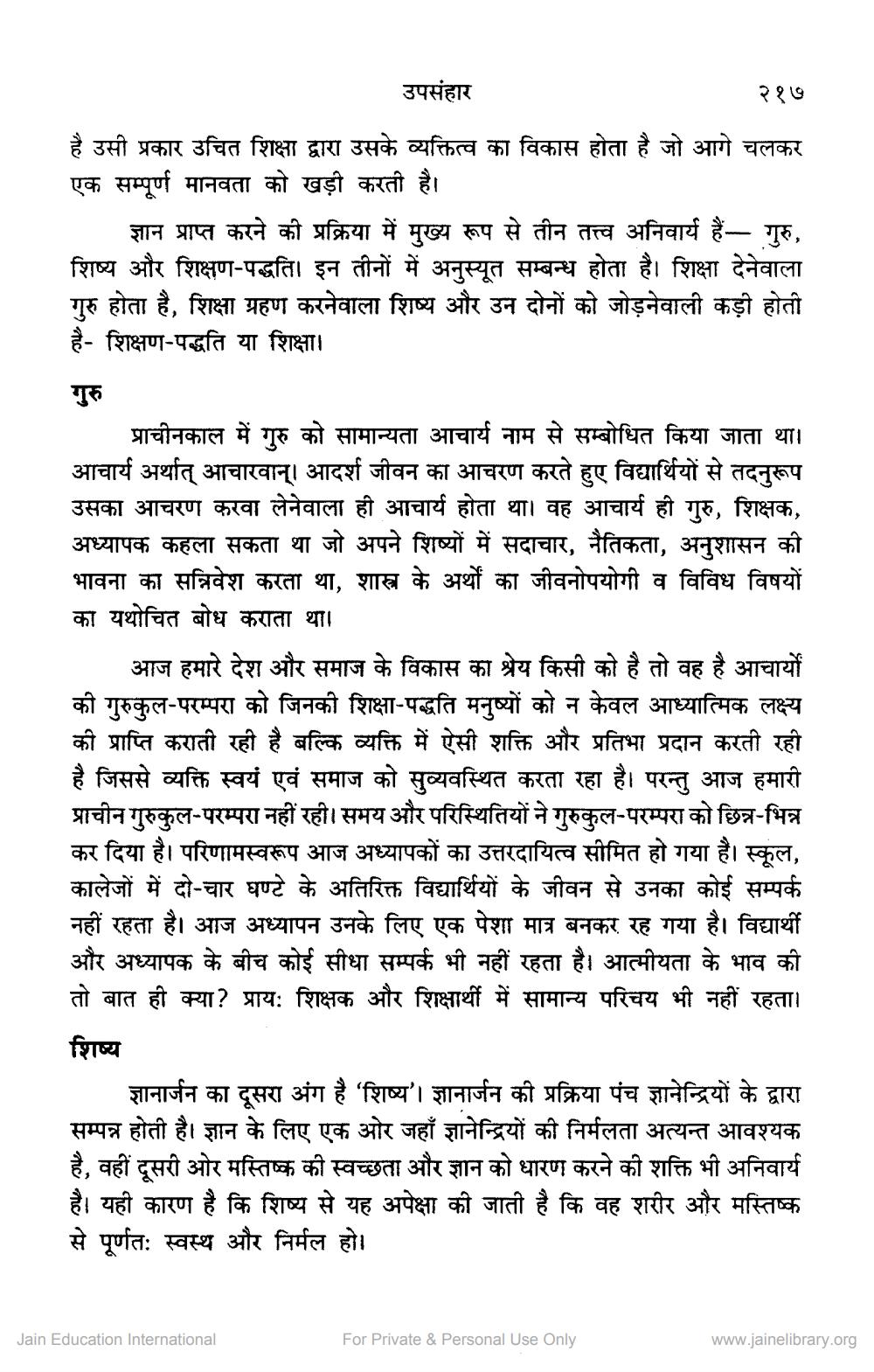________________
उपसंहार
२१७
है उसी प्रकार उचित शिक्षा द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है जो आगे चलकर एक सम्पूर्ण मानवता को खड़ी करती है।
ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन तत्त्व अनिवार्य हैं- गुरु, शिष्य और शिक्षण-पद्धति। इन तीनों में अनुस्यूत सम्बन्ध होता है। शिक्षा देनेवाला गुरु होता है, शिक्षा ग्रहण करनेवाला शिष्य और उन दोनों को जोड़नेवाली कड़ी होती है- शिक्षण-पद्धति या शिक्षा।
प्राचीनकाल में गुरु को सामान्यता आचार्य नाम से सम्बोधित किया जाता था। आचार्य अर्थात् आचारवान्। आदर्श जीवन का आचरण करते हुए विद्यार्थियों से तदनुरूप उसका आचरण करवा लेनेवाला ही आचार्य होता था। वह आचार्य ही गुरु, शिक्षक, अध्यापक कहला सकता था जो अपने शिष्यों में सदाचार, नैतिकता, अनुशासन की भावना का सन्निवेश करता था, शास्त्र के अर्थों का जीवनोपयोगी व विविध विषयों का यथोचित बोध कराता था।
आज हमारे देश और समाज के विकास का श्रेय किसी को है तो वह है आचार्यों की गुरुकुल-परम्परा को जिनकी शिक्षा-पद्धति मनुष्यों को न केवल आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कराती रही है बल्कि व्यक्ति में ऐसी शक्ति और प्रतिभा प्रदान करती रही है जिससे व्यक्ति स्वयं एवं समाज को सुव्यवस्थित करता रहा है। परन्तु आज हमारी प्राचीन गुरुकुल-परम्परा नहीं रही। समय और परिस्थितियों ने गुरुकुल-परम्परा को छिन्न-भिन्न कर दिया है। परिणामस्वरूप आज अध्यापकों का उत्तरदायित्व सीमित हो गया है। स्कूल, कालेजों में दो-चार घण्टे के अतिरिक्त विद्यार्थियों के जीवन से उनका कोई सम्पर्क नहीं रहता है। आज अध्यापन उनके लिए एक पेशा मात्र बनकर रह गया है। विद्यार्थी और अध्यापक के बीच कोई सीधा सम्पर्क भी नहीं रहता है। आत्मीयता के भाव की तो बात ही क्या? प्राय: शिक्षक और शिक्षार्थी में सामान्य परिचय भी नहीं रहता।
शिष्य
ज्ञानार्जन का दूसरा अंग है 'शिष्य'। ज्ञानार्जन की प्रक्रिया पंच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा सम्पन्न होती है। ज्ञान के लिए एक ओर जहाँ ज्ञानेन्द्रियों की निर्मलता अत्यन्त आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर मस्तिष्क की स्वच्छता और ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी अनिवार्य है। यही कारण है कि शिष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शरीर और मस्तिष्क से पूर्णतः स्वस्थ और निर्मल हो।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org