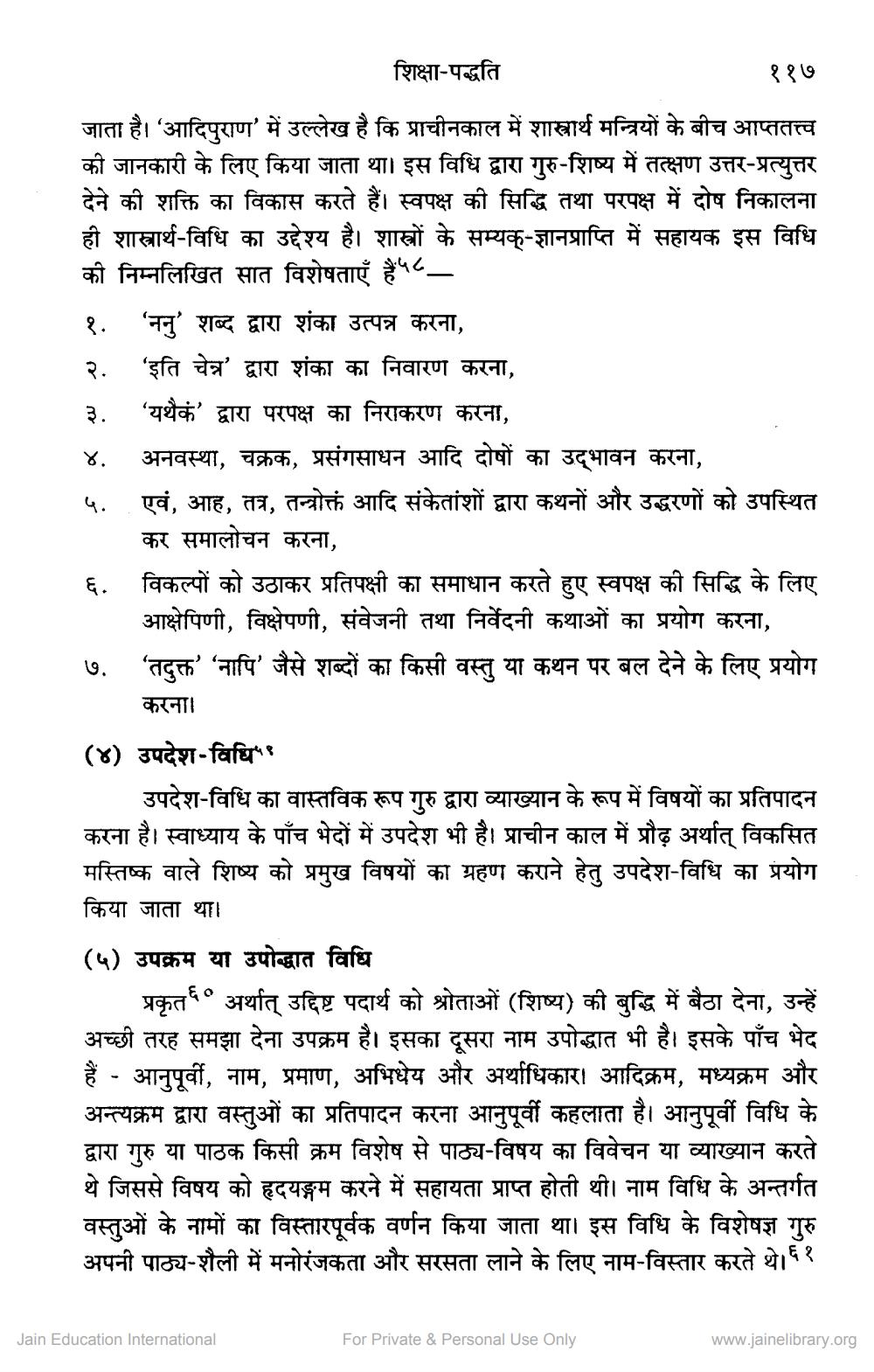________________
शिक्षा-पद्धति
११७
जाता है। 'आदिपुराण' में उल्लेख है कि प्राचीनकाल में शास्त्रार्थ मन्त्रियों के बीच आप्ततत्त्व की जानकारी के लिए किया जाता था । इस विधि द्वारा गुरु-शिष्य में तत्क्षण उत्तर- प्रत्युत्तर देने की शक्ति का विकास करते हैं। स्वपक्ष की सिद्धि तथा परपक्ष में दोष निकालना ही शास्त्रार्थ - विधि का उद्देश्य है। शास्त्रों के सम्यक् - ज्ञानप्राप्ति में सहायक इस विधि की निम्नलिखित सात विशेषताएँ हैं५८
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
'ननु' शब्द द्वारा शंका उत्पन्न करना,
' इति चेत्र' द्वारा शंका का निवारण करना,
'यथैकं' द्वारा परपक्ष का निराकरण करना,
अनवस्था, चक्रक, प्रसंगसाधन आदि दोषों का उद्भावन करना,
एवं, आह, तत्र, तन्त्रोक्तं आदि संकेतांशों द्वारा कथनों और उद्धरणों को उपस्थित कर समालोचन करना,
विकल्पों को उठाकर प्रतिपक्षी का समाधान करते हुए स्वपक्ष की सिद्धि के लिए आक्षेपिणी, विक्षेपणी, संवेजनी तथा निर्वेदनी कथाओं का प्रयोग करना,
'तदुक्त' 'नापि' जैसे शब्दों का किसी वस्तु या कथन पर बल देने के लिए प्रयोग
करना।
(४) उपदेश - विधि ५ ९
उपदेश-विधि का वास्तविक रूप गुरु द्वारा व्याख्यान के रूप में विषयों का प्रतिपादन करना है। स्वाध्याय के पाँच भेदों में उपदेश भी है। प्राचीन काल में प्रौढ़ अर्थात् विकसित मस्तिष्क वाले शिष्य को प्रमुख विषयों का ग्रहण कराने हेतु उपदेश-विधि का प्रयोग किया जाता था।
(५) उपक्रम या उपोद्धात विधि
प्रकृत६० अर्थात् उद्दिष्ट पदार्थ को श्रोताओं (शिष्य) की बुद्धि में बैठा देना, उन्हें अच्छी तरह समझा देना उपक्रम है। इसका दूसरा नाम उपोद्घात भी है। इसके पाँच भेद हैं- आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, अभिधेय और अर्थाधिकार । आदिक्रम, मध्यक्रम और अन्त्यक्रम द्वारा वस्तुओं का प्रतिपादन करना आनुपूर्वी कहलाता है। आनुपूर्वी विधि के द्वारा गुरु या पाठक किसी क्रम विशेष से पाठ्य विषय का विवेचन या व्याख्यान करते थे जिससे विषय को हृदयङ्गम करने में सहायता प्राप्त होती थी । नाम विधि के अन्तर्गत वस्तुओं के नामों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता था। इस विधि के विशेषज्ञ गुरु अपनी पाठ्य-शैली में मनोरंजकता और सरसता लाने के लिए नाम - विस्तार करते थे । ६१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org