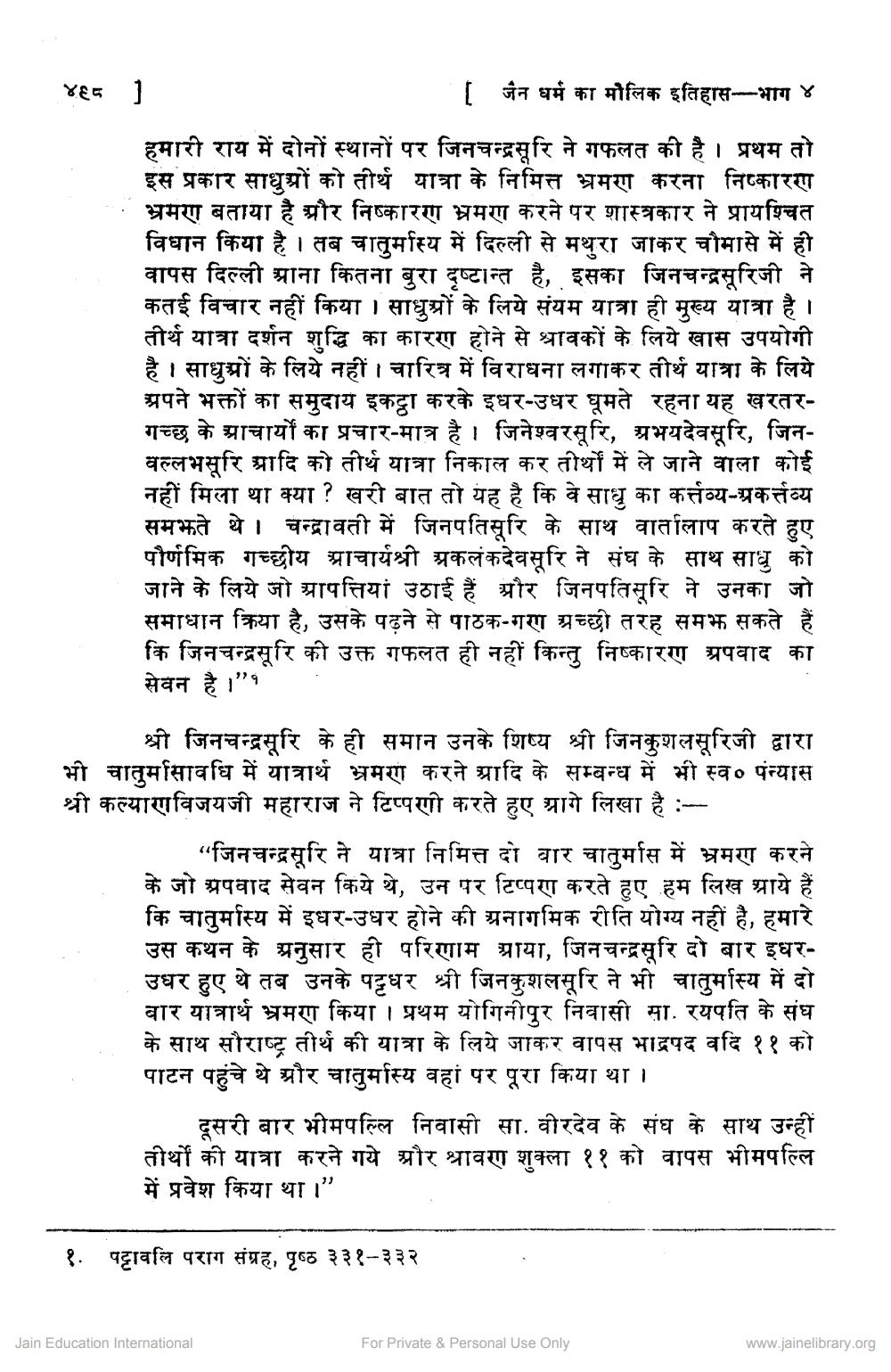________________
४६८
]
[
जैन धर्म का मौलिक इतिहास-भाग ४
हमारी राय में दोनों स्थानों पर जिनचन्द्रसूरि ने गफलत की है। प्रथम तो इस प्रकार साधुनों को तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करना निष्कारण भ्रमण बताया है और निष्कारण भ्रमण करने पर शास्त्रकार ने प्रायश्चित विधान किया है । तब चातुर्मास्य में दिल्ली से मथुरा जाकर चौमासे में ही वापस दिल्ली आना कितना बुरा दृष्टान्त है, इसका जिनचन्द्रसूरिजी ने कतई विचार नहीं किया। साधुओं के लिये संयम यात्रा ही मुख्य यात्रा है । तीर्थ यात्रा दर्शन शुद्धि का कारण होने से श्रावकों के लिये खास उपयोगी है। साधुओं के लिये नहीं। चारित्र में विराधना लगाकर तीर्थ यात्रा के लिये अपने भक्तों का समुदाय इकट्ठा करके इधर-उधर घूमते रहना यह खरतरगच्छ के प्राचार्यों का प्रचार-मात्र है। जिनेश्वरसूरि, अभयदेवसूरि, जिनवल्लभसूरि आदि को तीर्थ यात्रा निकाल कर तीर्थों में ले जाने वाला कोई नहीं मिला था क्या? खरी बात तो यह है कि वे साधु का कर्तव्य-अकर्तव्य समझते थे। चन्द्रावती में जिनपतिसूरि के साथ वार्तालाप करते हुए पौर्णमिक गच्छीय आचार्यश्री अकलंकदेवसूरि ने संघ के साथ साधु को जाने के लिये जो आपत्तियां उठाई हैं और जिनपतिसूरि ने उनका जो समाधान किया है, उसके पढ़ने से पाठक-गरण अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिनचन्द्रसूरि की उक्त गफलत ही नहीं किन्तु निष्कारण अपवाद का सेवन है।"१
श्री जिनचन्द्रसूरि के ही समान उनके शिष्य श्री जिनकुशलसूरिजी द्वारा भी चातुर्मासावधि में यात्रार्थ भ्रमण करने आदि के सम्बन्ध में भी स्व० पंन्यास श्री कल्याणविजयजी महाराज ने टिप्पणी करते हुए आगे लिखा है :
___ "जिनचन्द्रसूरि ने यात्रा निमित्त दो बार चातुर्मास में भ्रमण करने के जो अपवाद सेवन किये थे, उन पर टिप्पण करते हुए हम लिख पाये हैं कि चातुर्मास्य में इधर-उधर होने की अनागमिक रीति योग्य नहीं है, हमारे उस कथन के अनुसार ही परिणाम प्राया, जिनचन्द्रसूरि दो बार इधरउधर हुए थे तब उनके पट्टधर श्री जिनकुशलसूरि ने भी चातुर्मास्य में दो बार यात्रार्थ भ्रमण किया। प्रथम योगिनीपुर निवासी सा. रयपति के संघ के साथ सौराष्ट्र तीर्थ की यात्रा के लिये जाकर वापस भाद्रपद वदि ११ को पाटन पहुंचे थे और चातुर्मास्य वहां पर पूरा किया था।
दूसरी बार भीमपल्लि निवासी सा. वीरदेव के संघ के साथ उन्हीं तीर्थों की यात्रा करने गये और श्रावण शुक्ला ११ को वापस भीमपल्लि में प्रवेश किया था।"
१. पट्टावलि पराग संग्रह, पृष्ठ ३३१-३३२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org