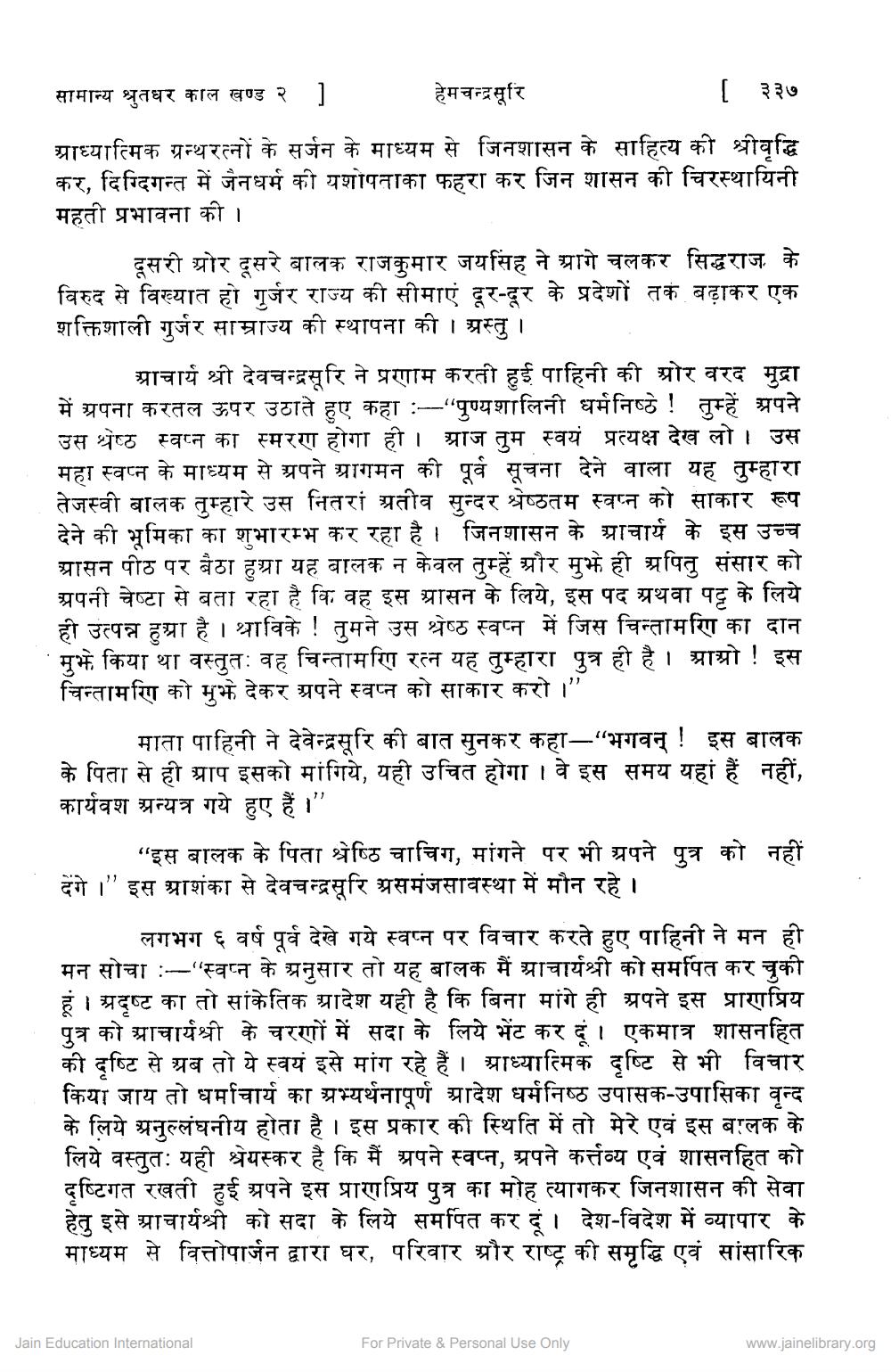________________
सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ]
हेमचन्द्रसूरि
[
३३७
आध्यात्मिक ग्रन्थरत्नों के सर्जन के माध्यम से जिनशासन के साहित्य की श्रीवृद्धि कर, दिग्दिगन्त में जैनधर्म की यशोपताका फहरा कर जिन शासन की चिरस्थायिनी महती प्रभावना की।
दूसरी ओर दूसरे बालक राजकुमार जयसिंह ने आगे चलकर सिद्धराज के विरुद से विख्यात हो गुर्जर राज्य की सीमाएं दूर-दूर के प्रदेशों तक बढ़ाकर एक शक्तिशाली गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की । अस्तु ।।
__ प्राचार्य श्री देवचन्द्रसूरि ने प्रणाम करती हुई पाहिनी की ओर वरद मुद्रा में अपना करतल ऊपर उठाते हुए कहा :- "पुण्यशालिनी धर्मनिष्ठे ! तुम्हें अपने उस श्रेष्ठ स्वप्न का स्मरण होगा ही। आज तुम स्वयं प्रत्यक्ष देख लो। उस महा स्वप्न के माध्यम से अपने प्रागमन की पूर्व सूचना देने वाला यह तुम्हारा तेजस्वी बालक तुम्हारे उस नितरां अतीव सुन्दर श्रेष्ठतम स्वप्न को साकार रूप देने की भूमिका का शभारम्भ कर रहा है। जिनशासन के प्राचार्य के इस उच्च प्रासन पीठ पर बैठा हुया यह बालक न केवल तुम्हें और मुझे ही अपितु संसार को अपनी चेष्टा से बता रहा है कि वह इस अासन के लिये, इस पद अथवा पट्ट के लिये ही उत्पन्न हना है । श्राविके ! तुमने उस श्रेष्ठ स्वप्न में जिस चिन्तामणि का दान मुझे किया था वस्तुतः वह चिन्तामणि रत्न यह तुम्हारा पुत्र ही है। प्रायो ! इस चिन्तामरिण को मुझे देकर अपने स्वप्न को साकार करो।"
माता पाहिनी ने देवेन्द्रसूरि की बात सुनकर कहा- "भगवन् ! इस बालक के पिता से ही आप इसको मांगिये, यही उचित होगा । वे इस समय यहां हैं नहीं, कार्यवश अन्यत्र गये हुए हैं।"
__ "इस बालक के पिता श्रेष्ठ चाचिग, मांगने पर भी अपने पुत्र को नहीं देंगे।" इस आशंका से देवचन्द्रसूरि असमंजसावस्था में मौन रहे ।
लगभग ६ वर्ष पूर्व देखे गये स्वप्न पर विचार करते हुए पाहिनी ने मन ही मन सोचा :- "स्वप्न के अनुसार तो यह बालक मैं आचार्यश्री को समर्पित कर चुकी हूं। अदृष्ट का तो सांकेतिक अादेश यही है कि बिना मांगे ही अपने इस प्राणप्रिय पुत्र को आचार्यश्री के चरणों में सदा के लिये भेंट कर दूं। एकमात्र शासनहित की दृष्टि से अब तो ये स्वयं इसे मांग रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार किया जाय तो धर्माचार्य का अभ्यर्थनापूर्ण आदेश धर्मनिष्ठ उपासक-उपासिका वृन्द के लिये अनुल्लंघनीय होता है । इस प्रकार की स्थिति में तो मेरे एवं इस बालक के लिये वस्तुतः यही श्रेयस्कर है कि मैं अपने स्वप्न, अपने कर्तव्य एवं शासनहित को दृष्टिगत रखती हुई अपने इस प्राणप्रिय पुत्र का मोह त्यागकर जिनशासन की सेवा हेतु इसे प्राचार्यश्री को सदा के लिये समर्पित कर दूं। देश-विदेश में व्यापार के माध्यम से वित्तोपार्जन द्वारा घर, परिवार और राष्ट्र की समृद्धि एवं सांसारिक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org