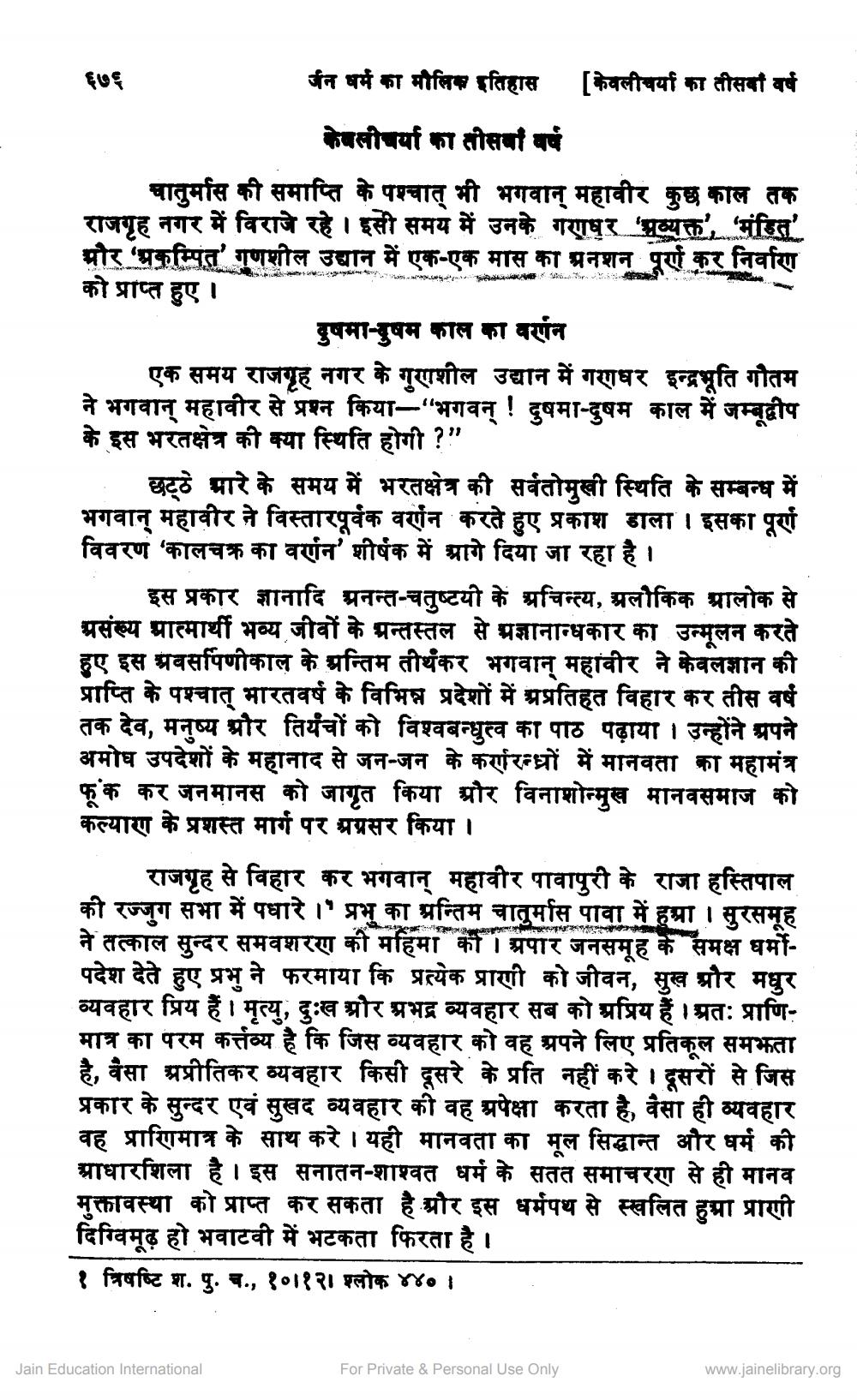________________
६७६
जन धर्म का मौलिक इतिहास [केवलीवर्या का तीसवां वर्ष
केवलीचर्या का तीसवां वर्ष चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात् भी भगवान् महावीर कुछ काल तक राजगृह नगर में विराजे रहे । इसी समय में उनके गणधर 'अव्यक्त', 'मंडित' और 'प्रकृम्पित' गुणशील उद्यान में एक-एक मास का अनशन पूर्ण कर निर्वाण को प्राप्त हुए।
दुषमा-दुषम काल का वर्णन एक समय राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में गणधर इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया-"भगवन् ! दुषमा-दुषम काल में जम्बूद्वीप के इस भरतक्षेत्र की क्या स्थिति होगी ?"
. भारे के समय में भरतक्षेत्र की सर्वतोमुखी स्थिति के सम्बन्ध में भगवान् महावीर ने विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए प्रकाश डाला। इसका पूर्ण विवरण 'कालचक्र का वर्णन' शीर्षक में आगे दिया जा रहा है ।
इस प्रकार ज्ञानादि अनन्त-चतुष्टयो के अचिन्त्य, अलौकिक पालोक से असंख्य मात्मार्थी भव्य जीवों के अन्तस्तल से प्रज्ञानान्धकार का उन्मूलन करते हुए इस अवसर्पिणीकाल के अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर ने केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में अप्रतिहत विहार कर तीस वर्ष तक देव, मनुष्य और तियंचों को विश्वबन्धुत्व का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपने अमोघ उपदेशों के महानाद से जन-जन के कर्णरन्ध्रों में मानवता का महामंत्र फूक कर जनमानस को जागृत किया और विनाशोन्मुख मानवसमाज को कल्याण के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर किया।
राजगृह से विहार कर भगवान् महावीर पावापुरी के राजा हस्तिपाल की रज्जुग सभा में पधारे ।' प्रभु का अन्तिम चातुर्मास पावा में हुप्रा । सुरसमूह ने तत्काल सुन्दर समवशरण की महिमा की। अपार जनसमूह के समक्ष धर्मोपदेश देते हुए प्रभु ने फरमाया कि प्रत्येक प्राणी को जीवन, सुख और मधुर व्यवहार प्रिय हैं। मृत्यु, दुःख और अभद्र व्यवहार सब को अप्रिय हैं। अतः प्राणिमात्र का परम कर्तव्य है कि जिस व्यवहार को वह अपने लिए प्रतिकूल समझता है, वैसा अप्रीतिकर व्यवहार किसी दूसरे के प्रति नहीं करे । दूसरों से जिस प्रकार के सुन्दर एवं सुखद व्यवहार की वह अपेक्षा करता है, वैसा ही व्यवहार वह प्राणिमात्र के साथ करे । यही मानवता का मूल सिद्धान्त और धर्म की आधारशिला है। इस सनातन-शाश्वत धर्म के सतत समाचरण से ही मानव मुक्तावस्था को प्राप्त कर सकता है और इस धर्मपथ से स्खलित हुप्रा प्राणी दिग्विमूढ़ हो भवाटवी में भटकता फिरता है। १ त्रिषष्टि श. पु. च., १०।१२। श्लोक ४४० ।
muni
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org