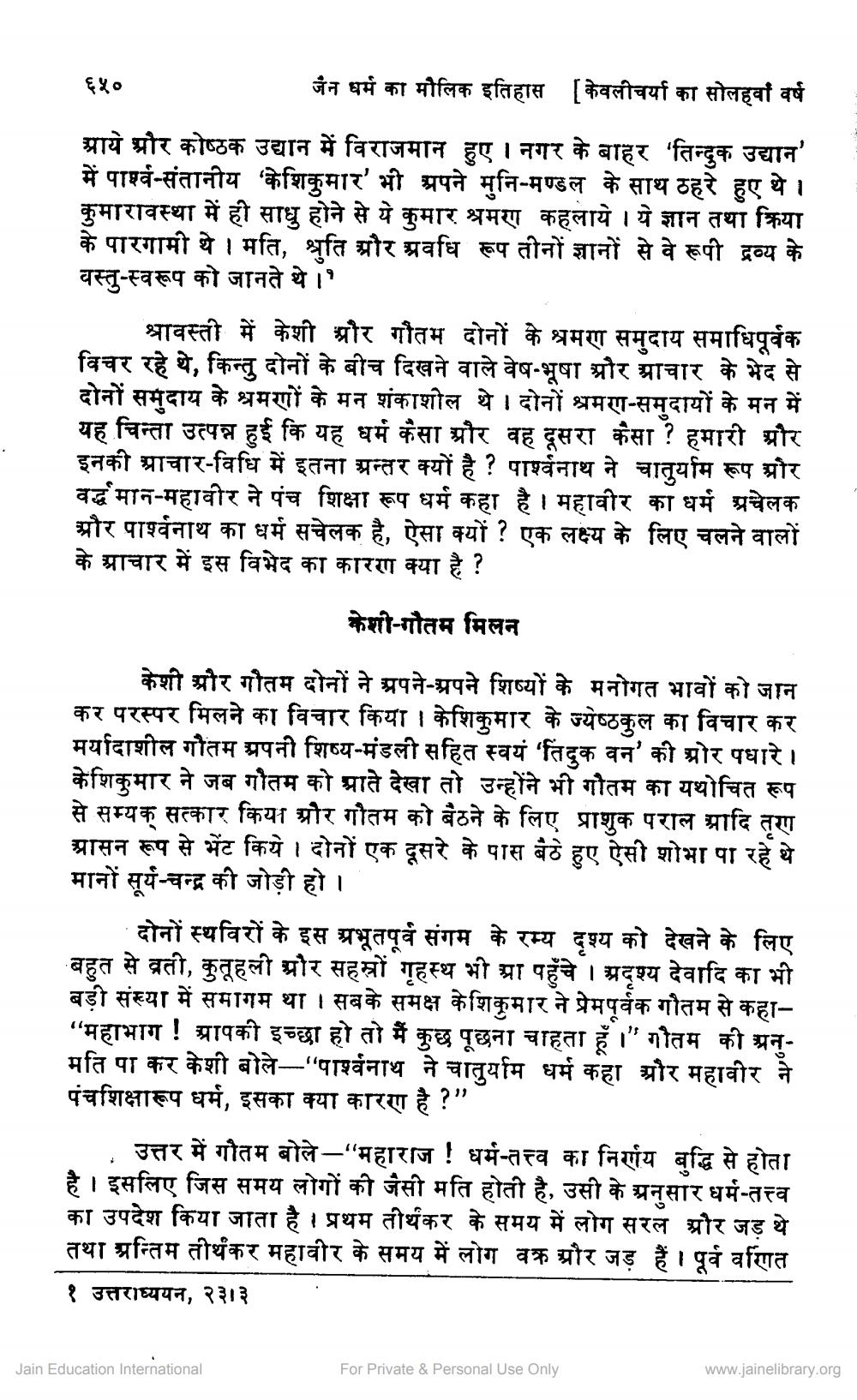________________
६५०
जैन धर्म का मौलिक इतिहास [केवलीचर्या का सोलहवां वर्ष
आये और कोष्ठक उद्यान में विराजमान हुए । नगर के बाहर 'तिन्दुक उद्यान' में पार्श्व-संतानीय 'केशिकुमार' भी अपने मुनि-मण्डल के साथ ठहरे हुए थे। कुमारावस्था में ही साधु होने से ये कुमार श्रमण कहलाये । ये ज्ञान तथा क्रिया के पारगामी थे । मति, श्रुति और अवधि रूप तीनों ज्ञानों से वे रूपी द्रव्य के वस्तु-स्वरूप को जानते थे।'
श्रावस्ती में केशी और गौतम दोनों के श्रमण समुदाय समाधिपूर्वक विचर रहे थे, किन्तु दोनों के बीच दिखने वाले वेष-भूषा और प्राचार के भेद से दोनों समुदाय के श्रमणों के मन शंकाशील थे। दोनों श्रमण-समुदायों के मन में यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि यह धर्म कैसा और वह दूसरा कैसा? हमारी और इनकी प्राचार-विधि में इतना अन्तर क्यों है ? पार्श्वनाथ ने चातुर्याम रूप और वर्द्धमान-महावीर ने पंच शिक्षा रूप धर्म कहा है। महावीर का धर्म अचेलक और पार्श्वनाथ का धर्म सचेलक है, ऐसा क्यों ? एक लक्ष्य के लिए चलने वालों के प्राचार में इस विभेद का कारण क्या है ?
केशी-गौतम मिलन केशी और गौतम दोनों ने अपने-अपने शिष्यों के मनोगत भावों को जान कर परस्पर मिलने का विचार किया । केशिकुमार के ज्येष्ठकुल का विचार कर मर्यादाशील गौतम अपनी शिष्य-मंडली सहित स्वयं 'तिदुक वन' की ओर पधारे। केशिकूमार ने जब गौतम को प्राते देखा तो उन्होंने भी गौतम का यथोचित रूप से सम्यक सत्कार किया और गौतम को बैठने के लिए प्राशुक पराल आदि तण आसन रूप से भेंट किये । दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए ऐसी शोभा पा रहे थे मानों सूर्य-चन्द्र की जोड़ी हो।
दोनों स्थविरों के इस अभूतपूर्व संगम के रम्य दश्य को देखने के लिए बहुत से व्रती, कुतूहली और सहस्रों गृहस्थ भी आ पहुँचे । अदृश्य देवादि का भी बड़ी संख्या में समागम था । सबके समक्ष केशिकुमार ने प्रेमपूर्वक गौतम से कहा"महाभाग ! आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ।" गौतम की अनुमति पा कर केशी बोले-"पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म कहा और महावीर ने पंचशिक्षारूप धर्म, इसका क्या कारण है ?"
उत्तर में गौतम बोले-"महाराज! धर्म-तत्त्व का निर्णय बुद्धि से होता है। इसलिए जिस समय लोगों की जैसी मति होती है, उसी के अनुसार धर्म-तत्त्व का उपदेश किया जाता है । प्रथम तीर्थंकर के समय में लोग सरल और जड़ थे तथा अन्तिम तीर्थंकर महावीर के समय में लोग वक्र और जड़ हैं। पूर्व वरिणत १ उत्तराध्ययन, २३॥३
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org