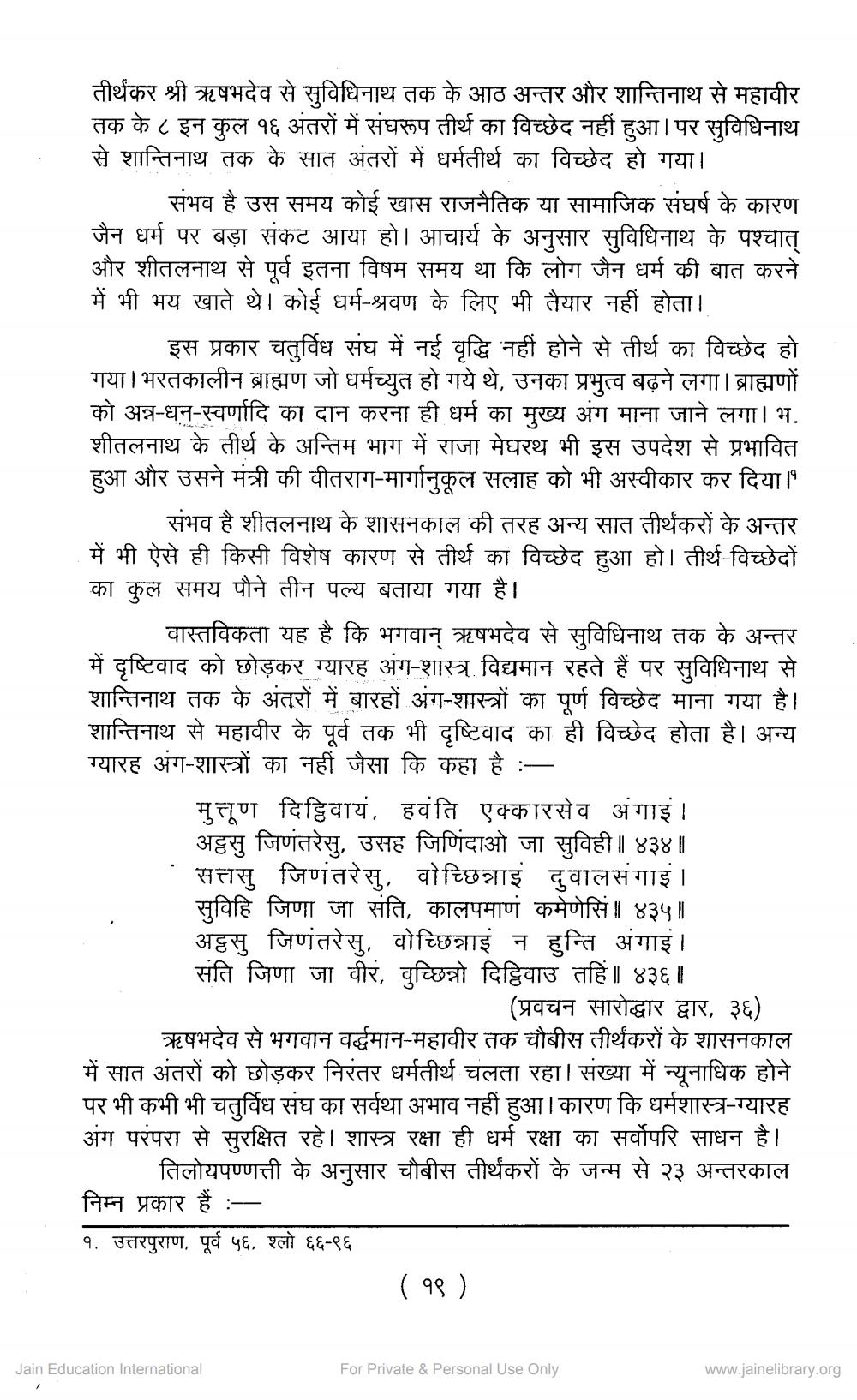________________
तीर्थंकर श्री ऋषभदेव से सुविधिनाथ तक के आठ अन्तर और शान्तिनाथ से महावीर तक के ८ इन कुल १६ अंतरों में संघरूप तीर्थ का विच्छेद नहीं हुआ। पर सुविधिनाथ से शान्तिनाथ तक के सात अंतरों में धर्मतीर्थ का विच्छेद हो गया।
/
संभव है उस समय कोई खास राजनैतिक या सामाजिक संघर्ष के कारण जैन धर्म पर बड़ा संकट आया हो । आचार्य के अनुसार सुविधिनाथ के पश्चात् और शीतलनाथ से पूर्व इतना विषम समय था कि लोग जैन धर्म की बात करने में भी भय खाते थे। कोई धर्म-श्रवण के लिए भी तैयार नहीं होता ।
इस प्रकार चतुर्विध संघ में नई वृद्धि नहीं होने से तीर्थ का विच्छेद हो गया। भरतकालीन ब्राह्मण जो धर्मच्युत हो गये थे, उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा । ब्राह्मणों को अन्न-धन-स्वर्णादि का दान करना ही धर्म का मुख्य अंग माना जाने लगा । भ. शीतलनाथ के तीर्थ के अन्तिम भाग में राजा मेघरथ भी इस उपदेश से प्रभावित हुआ और उसने मंत्री की वीतराग-मार्गानुकूल सलाह को भी अस्वीकार कर दिया । " संभव है शीतलनाथ के शासनकाल की तरह अन्य सात तीर्थंकरों के अन्तर में भी ऐसे ही किसी विशेष कारण से तीर्थ का विच्छेद हुआ हो। तीर्थ-विच्छेदों का कुल समय पौने तीन पल्य बताया गया है ।
वास्तविकता यह है कि भगवान् ऋषभदेव से सुविधिनाथ तक के अन्तर में दृष्टिवाद को छोड़कर ग्यारह अंग- शास्त्र विद्यमान रहते हैं पर सुविधिनाथ से शान्तिनाथ तक के अंतरों में बारहों अंग - शास्त्रों का पूर्ण विच्छेद माना गया है। शान्तिनाथ से महावीर के पूर्व तक भी दृष्टिवाद का ही विच्छेद होता है । अन्य ग्यारह अंग - शास्त्रों का नहीं जैसा कि कहा है :
मुत्तूण दिट्ठिवायं हवंति एक्कारसेव अंगाई । अट्ठसु जिणंतरेसु, उसह जिणिंदाओ जा सुविही ॥ ४३४ ॥ सत्तसु जिणंतरेसु, वोच्छिन्नाइं दुवालसंगाई | सुविहि जिणा जा संति, कालपमाणं कमेणेसिं ॥ ४३५ ॥ अट्ठसु जिणंतरेसु, वोच्छिन्नाई न हुन्ति अंगाई । संति जिणा जा वीरं वुच्छिन्नो दिट्ठिवाउ तहिं ॥ ४३६ ॥ (प्रवचन सारोद्धार द्वार, ३६) ऋषभदेव से भगवान वर्द्धमान महावीर तक चौबीस तीर्थंकरों के शासनकाल में सात अंतरों को छोड़कर निरंतर धर्मतीर्थ चलता रहा । संख्या में न्यूनाधिक होने पर भी कभी भी चतुर्विध संघ का सर्वथा अभाव नहीं हुआ । कारण कि धर्मशास्त्र - ग्यारह अंग परंपरा से सुरक्षित रहे । शास्त्र रक्षा ही धर्म रक्षा का सर्वोपरि साधन है। तिलोयपण्णत्ती के अनुसार चौबीस तीर्थकरों के जन्म से २३ अन्तरकाल निम्न प्रकार हैं : —
१. उत्तरपुराण, पूर्व ५६, श्लो ६६-९६
Jain Education International
( १९ )
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org