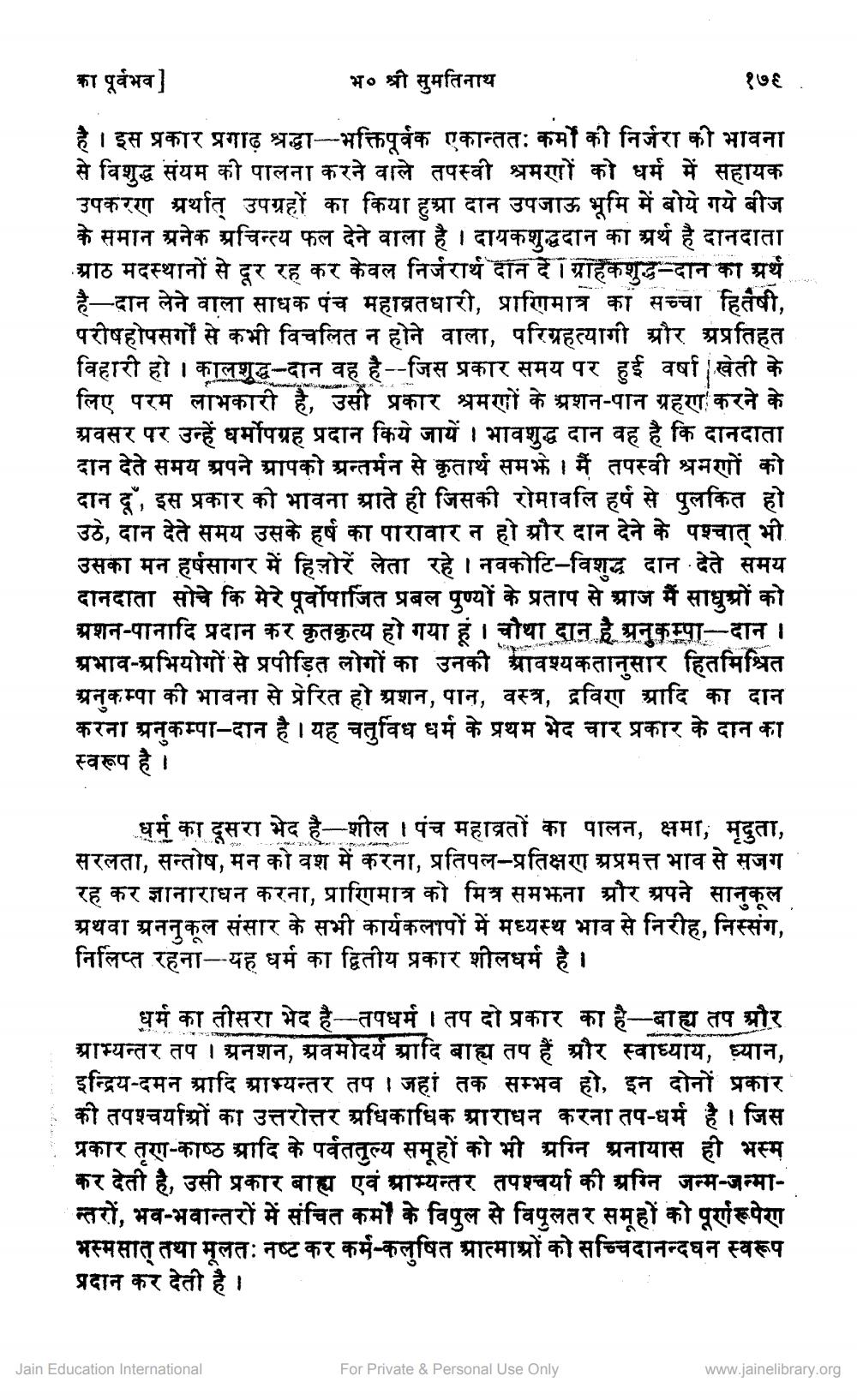________________
का पूर्वभव भ० श्री सुमतिनाथ
१७६ . है । इस प्रकार प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्तिपूर्वक एकान्ततः कर्मों की निर्जरा की भावना से विशुद्ध संयम की पालना करने वाले तपस्वी श्रमणों को धर्म में सहायक उपकरण अर्थात् उपग्रहों का किया हुआ दान उपजाऊ भूमि में बोये गये बीज के समान अनेक अचिन्त्य फल देने वाला है । दायकशुद्धदान का अर्थ है दानदाता आठ मदस्थानों से दूर रह कर केवल निर्जरार्थ दान दें। ग्राहकशुद्ध-दान का अर्थ है-दान लेने वाला साधक पंच महाव्रतधारी, प्राणिमात्र का सच्चा हितैषी, परीषहोपसर्गों से कभी विचलित न होने वाला, परिग्रहत्यागी और अप्रतिहत विहारी हो । कालशुद्ध-दान वह है--जिस प्रकार समय पर हुई वर्षा खेती के लिए परम लाभकारी है, उसी प्रकार श्रमणों के प्रशन-पान ग्रहण करने के अवसर पर उन्हें धर्मोपग्रह प्रदान किये जायें । भावशुद्ध दान वह है कि दानदाता दान देते समय अपने आपको अन्तर्मन से कृतार्थ समझे । मैं तपस्वी श्रमणों को दान दूं, इस प्रकार को भावना पाते ही जिसकी रोमावलि हर्ष से पुलकित हो उठे, दान देते समय उसके हर्ष का पारावार न हो और दान देने के पश्चात् भी उसका मन हर्षसागर में हिलोरें लेता रहे । नवकोटि-विशुद्ध दान देते समय दानदाता सोचे कि मेरे पूर्वोपाजित प्रबल पुण्यों के प्रताप से आज मैं साधुनों को अशन-पानादि प्रदान कर कृतकृत्य हो गया हूं। चौथा दान है. अनुकम्पा-दान । अभाव-अभियोगों से प्रपीड़ित लोगों का उनकी आवश्यकतानुसार हितमिश्रित अनुकम्पा की भावना से प्रेरित हो अशन, पान, वस्त्र, द्रविण आदि का दान करना अनुकम्पा-दान है। यह चतुर्विध धर्म के प्रथम भेद चार प्रकार के दान का स्वरूप है।
धर्म का दूसरा भेद है-शील । पंच महाव्रतों का पालन, क्षमा, मृदुता, सरलता, सन्तोष, मन को वश में करना, प्रतिपल-प्रतिक्षण अप्रमत्त भाव से सजग रह कर ज्ञानाराधन करना, प्राणिमात्र को मित्र समझना और अपने सानुकूल अथवा अननुकूल संसार के सभी कार्यकलापों में मध्यस्थ भाव से निरीह, निस्संग, निलिप्त रहना-यह धर्म का द्वितीय प्रकार शीलधर्म है।
धर्म का तीसरा भेद है-तपधर्म । तप दो प्रकार का है-बाह्य तप और आभ्यन्तर तप । अनशन, अवमोदर्य आदि बाह्य तप हैं और स्वाध्याय, ध्यान, इन्द्रिय-दमन आदि आभ्यन्तर तप । जहां तक सम्भव हो, इन दोनों प्रकार की तपश्चर्याओं का उत्तरोत्तर अधिकाधिक आराधन करना तप-धर्म है। जिस प्रकार तरण-काष्ठ आदि के पर्वततुल्य समूहों को भी अग्नि अनायास ही भस्म कर देती है, उसी प्रकार बाह्य एवं प्राभ्यन्तर तपश्चर्या की अग्नि जन्म-जन्मान्तरों, भव-भवान्तरों में संचित कर्मों के विपुल से विपुलतर समूहों को पूर्णरूपेण भस्मसात् तथा मूलतः नष्ट कर कर्म-कलुषित प्रात्माओं को सच्चिदानन्दघन स्वरूप प्रदान कर देती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org