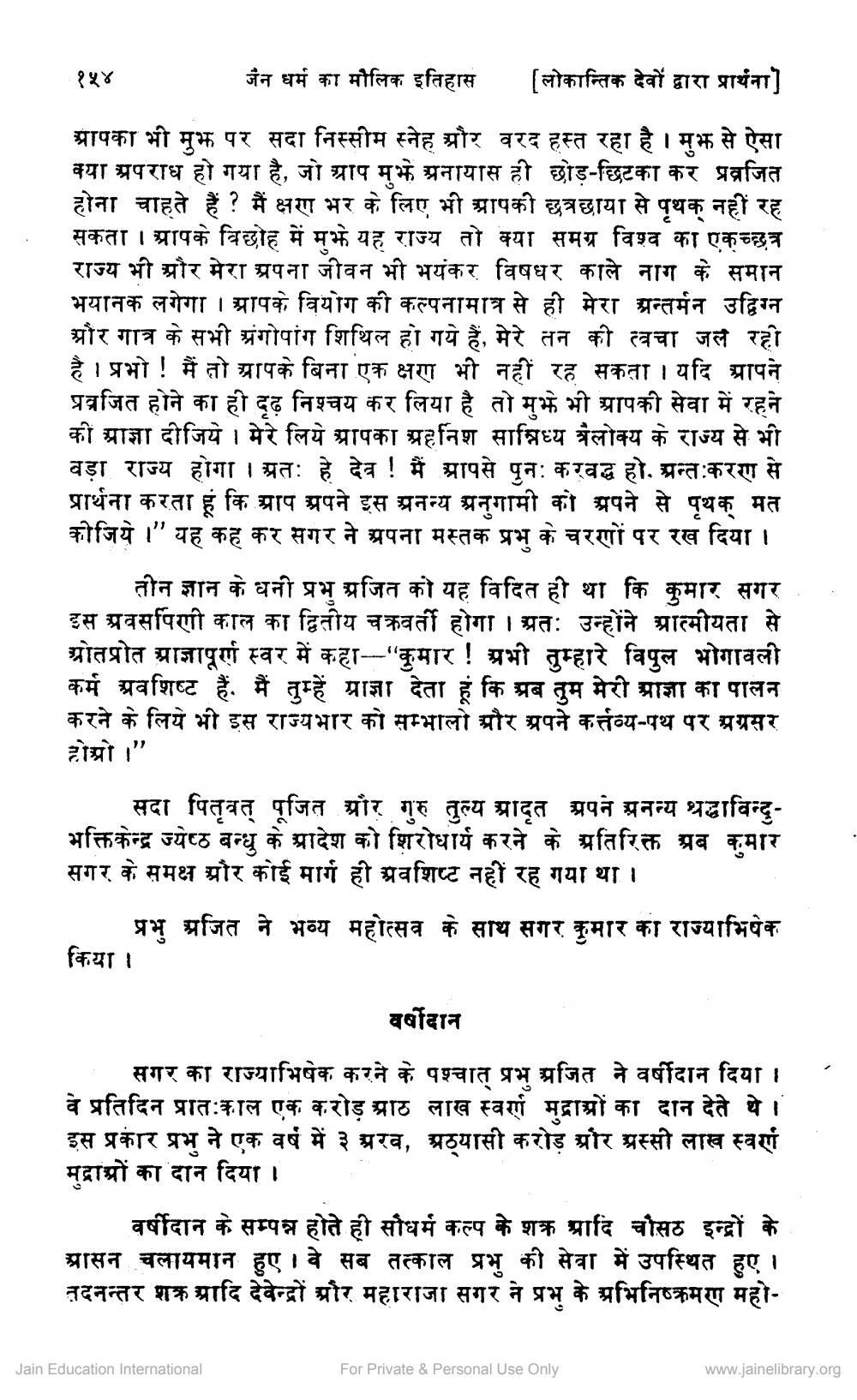________________
१५४
जैन धर्म का मौलिक इतिहास
लोकान्तिक देवों द्वारा प्रार्थना]
आपका भी मुझ पर सदा निस्सीम स्नेह और वरद हस्त रहा है । मुझ से ऐसा क्या अपराध हो गया है, जो पाप मुझे अनायास ही छोड़-छिटका कर प्रवजित होना चाहते हैं ? मैं क्षण भर के लिए भी आपकी छत्रछाया से पृथक नहीं रह सकता । आपके विछोह में मुझे यह राज्य तो क्या समग्र विश्व का एकच्छत्र राज्य भी और मेरा अपना जीवन भी भयंकर विषधर काले नाग के समान भयानक लगेगा । आपके वियोग की कल्पनामात्र से ही मेरा अन्तर्मन उद्विग्न और गात्र के सभी अंगोपांग शिथिल हो गये हैं, मेरे तन की त्वचा जल रही है । प्रभो ! मैं तो आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता । यदि आपने प्रवजित होने का ही दढ़ निश्चय कर लिया है तो मुझे भी आपकी सेवा में रहने की आज्ञा दीजिये । मेरे लिये आपका अहनिश सानिध्य त्रैलोक्य के राज्य से भी बड़ा राज्य होगा । अतः हे देव ! मैं आपसे पुन: करबद्ध हो. अन्तःकरण से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इस अनन्य अनुगामी को अपने से पथक मत कोजिये ।" यह कह कर सगर ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों पर रख दिया।
तीन ज्ञान के धनी प्रभु अजित को यह विदित ही था कि कुमार सगर इस अवसपिणी काल का द्वितीय चक्रवर्ती होगा । अतः उन्होंने आत्मीयता से अोतप्रोत प्राज्ञापूर्ण स्वर में कहा-"कुमार ! अभी तुम्हारे विपुल भोगावली कर्म अवशिष्ट हैं. मैं तुम्हें प्राज्ञा देता हूं कि अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिये भी इस राज्यभार को सम्भालो और अपने कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होयो।"
सदा पितृवत् पूजित और गुरु तुल्य प्रादृत अपने अनन्य श्रद्धाविन्दुभक्तिकेन्द्र ज्येष्ठ बन्ध के आदेश को शिरोधार्य करने के अतिरिक्त अब कमार सगर के समक्ष और कोई मार्ग ही अवशिष्ट नहीं रह गया था।
प्रभु अजित ने भव्य महोत्सव के साथ सगर कुमार का राज्याभिषेक किया।
।
वर्षादान सगर का राज्याभिषेक करने के पश्चात् प्रभु अजित ने वर्षीदान दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल एक करोड़ पाठ लाख स्वर्ण मद्राओं का दान देते थे। इस प्रकार प्रभु ने एक वर्ष में ३ अरव, अठ्यासी करोड़ और अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया।
वर्षीदान के सम्पन्न होते ही सौधर्म कल्प के शक प्रादि चौसठ इन्द्रों के प्रासन चलायमान हुए। वे सब तत्काल प्रभ की सेवा में उपस्थित हए । तदनन्तर शक प्रादि देवेन्द्रों और महाराजा सगर ने प्रभु के अभिनिष्क्रमण महो.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org