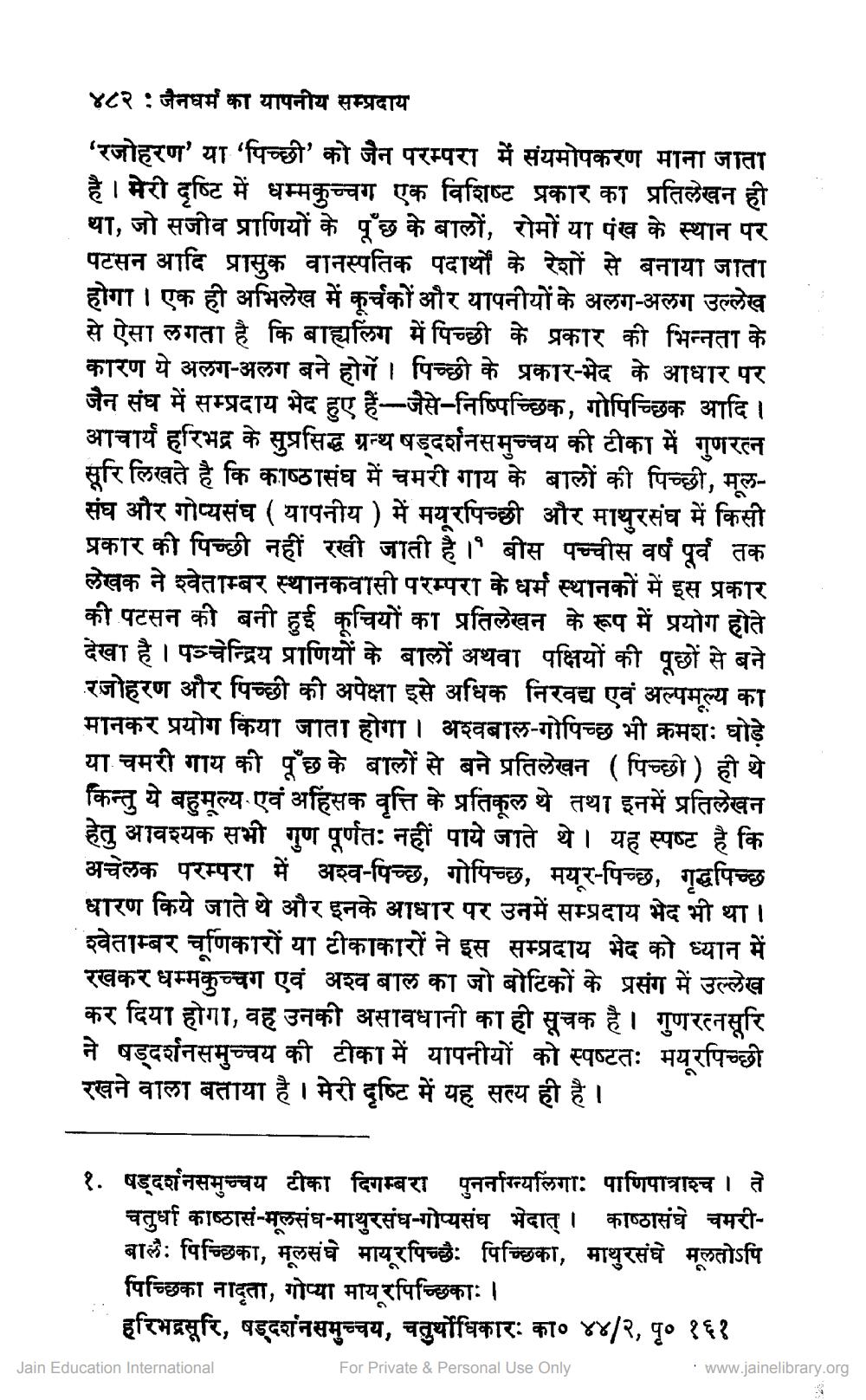________________
४८२ : जैनधर्म का यापनीय सम्प्रदाय 'रजोहरण' या 'पिच्छी' को जैन परम्परा में संयमोपकरण माना जाता है । मेरी दृष्टि में धम्मकुच्चग एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिलेखन ही था, जो सजीव प्राणियों के पूंछ के बालों, रोमों या पंख के स्थान पर पटसन आदि प्रासुक वानस्पतिक पदार्थों के रेशों से बनाया जाता होगा। एक ही अभिलेख में कर्चकों और यापनीयों के अलग-अलग उल्लेख से ऐसा लगता है कि बाह्यलिंग में पिच्छी के प्रकार की भिन्नता के कारण ये अलग-अलग बने होगें। पिच्छी के प्रकार-भेद के आधार पर जैन संघ में सम्प्रदाय भेद हुए हैं-जैसे-निष्पिच्छिक, गोपिच्छिक आदि । आचार्य हरिभद्र के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ षड्दर्शनसमुच्चय की टीका में गुणरत्न सूरि लिखते है कि काष्ठासंघ में चमरी गाय के बालों की पिच्छी, मूलसंघ और गोप्यसंघ ( यापनीय ) में मयूरपिच्छी और माथुरसंघ में किसी प्रकार की पिच्छी नहीं रखी जाती है। बीस पच्चीस वर्ष पूर्व तक लेखक ने श्वेताम्बर स्थानकवासी परम्परा के धर्म स्थानकों में इस प्रकार की पटसन की बनी हुई कूचियों का प्रतिलेखन के रूप में प्रयोग होते देखा है। पञ्चेन्द्रिय प्राणियों के बालों अथवा पक्षियों की पूछों से बने रजोहरण और पिच्छी की अपेक्षा इसे अधिक निरवद्य एवं अल्पमूल्य का मानकर प्रयोग किया जाता होगा। अश्वबाल-गोपिच्छ भी क्रमशः घोड़े या चमरी गाय की पूंछ के बालों से बने प्रतिलेखन (पिच्छी) ही थे किन्तु ये बहुमूल्य एवं अहिंसक वृत्ति के प्रतिकूल थे तथा इनमें प्रतिलेखन हेतु आवश्यक सभी गुण पूर्णतः नहीं पाये जाते थे। यह स्पष्ट है कि अचेलक परम्परा में अश्व-पिच्छ, गोपिच्छ, मयूर-पिच्छ, गृद्धपिच्छ धारण किये जाते थे और इनके आधार पर उनमें सम्प्रदाय भेद भी था। श्वेताम्बर चर्णिकारों या टीकाकारों ने इस सम्प्रदाय भेद को ध्यान में रखकर धम्मकुच्चग एवं अश्व बाल का जो बोटिकों के प्रसंग में उल्लेख कर दिया होगा, वह उनकी असावधानी का ही सूचक है। गुणरत्नसूरि ने षड्दर्शनसमुच्चय की टीका में यापनीयों को स्पष्टतः मयूरपिच्छी रखने वाला बताया है । मेरी दृष्टि में यह सत्य ही है।
१. षड्दर्शनसमुच्चय टीका दिगम्बरा पुन ग्न्यलिंगाः पाणिपात्राश्च । ते
चतुर्धा काष्ठासं-मूलसंघ-माथुरसंघ-गोप्यसंघ भेदात् । काष्ठासंघे चमरीबालैः पिच्छिका, मूलसंघे मायूरपिच्छैः पिच्छिका, माथुरसंघे मूलतोऽपि पिच्छिका नादृता, गोप्या मायूरपिच्छिकाः।
हरिभद्रसूरि, षड्दर्शनसमुच्चय, चतुर्थोधिकारः का० ४४/२, पृ० १६१ Jain Education International
For Private & Personal Use Only
- www.jainelibrary.org