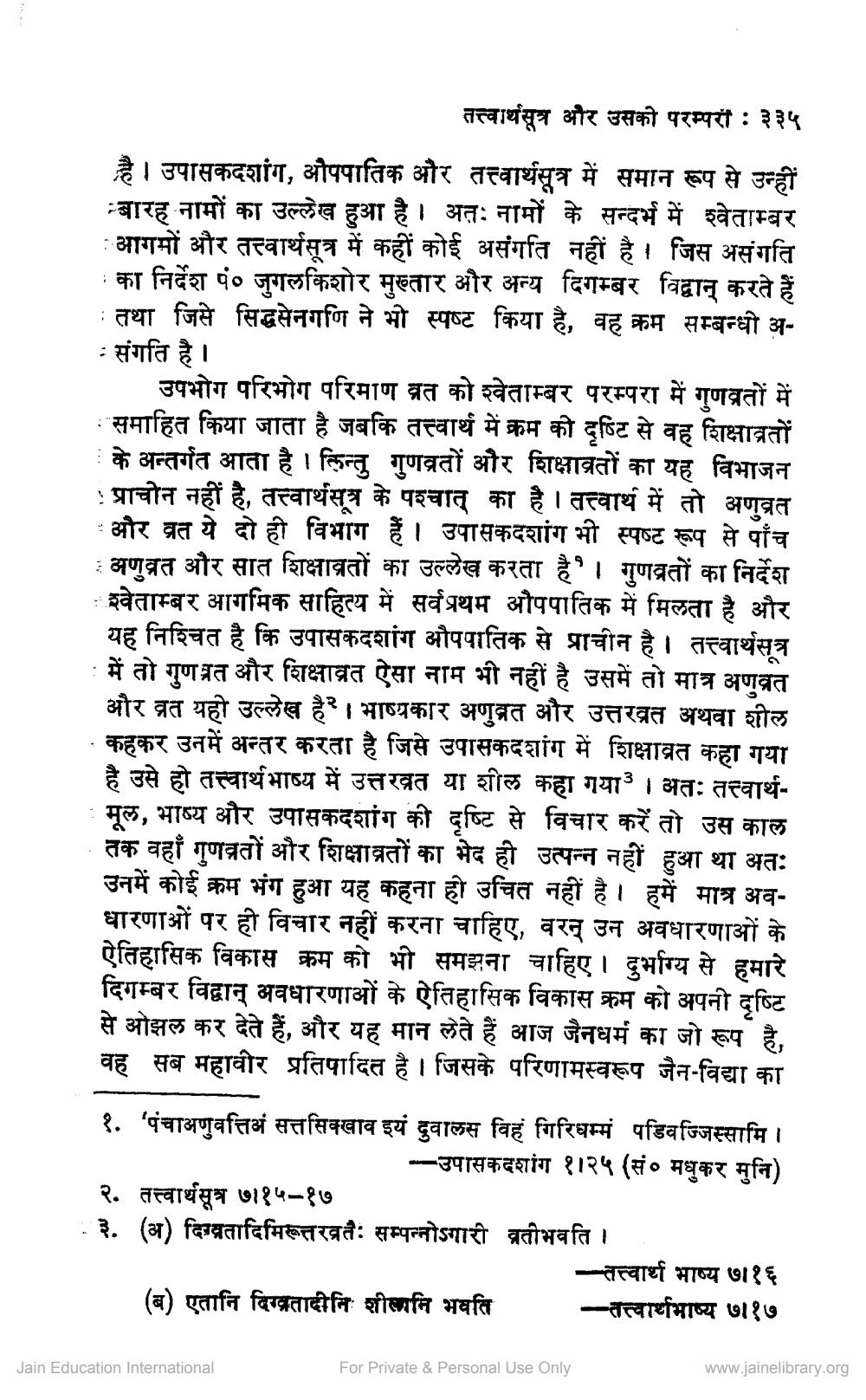________________
तत्त्वार्थसूत्र और उसको परम्परा : ३३५ है । उपासकदशांग, औपपातिक और तत्त्वार्थसूत्र में समान रूप से उन्हीं - बारह नामों का उल्लेख हुआ है । अतः नामों के सन्दर्भ में श्वेताम्बर आगमों और तत्त्वार्थसूत्र में कहीं कोई असंगति नहीं है । जिस असंगति • का निर्देश पं० जुगलकिशोर मुख्तार और अन्य दिगम्बर विद्वान् करते हैं : तथा जिसे सिद्धसेनगणि ने भी स्पष्ट किया है, वह क्रम सम्बन्धी असंगति है ।
उपभोग परिभोग परिमाण व्रत को श्वेताम्बर परम्परा में गुणव्रतों में समाहित किया जाता है जबकि तत्त्वार्थ में क्रम को दृष्टि से वह शिक्षाव्रतों के अन्तर्गत आता है । किन्तु गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों का यह विभाजन : प्राचीन नहीं है, तत्त्वार्थसूत्र के पश्चात् का है । तत्त्वार्थ में तो अणुव्रत - और व्रत ये दो ही विभाग हैं । उपासकदशांग भी स्पष्ट रूप से पाँच : अणुव्रत और सात शिक्षाव्रतों का उल्लेख करता है' । गुणव्रतों का निर्देश श्वेताम्बर आगमिक साहित्य में सर्वप्रथम औपपातिक में मिलता है और यह निश्चित है कि उपासकदशांग औपपातिक से प्राचीन है । तत्त्वार्थसूत्र में तो गुणव्रत और शिक्षाव्रत ऐसा नाम भी नहीं है उसमें तो मात्र अणुव्रत और व्रत यही उल्लेख है। भाष्यकार अणुव्रत और उत्तरव्रत अथवा शील कहकर उनमें अन्तर करता है जिसे उपासकदशांग में शिक्षाव्रत कहा गया है उसे हो तत्त्वार्थ भाष्य में उत्तरव्रत या शील कहा गया । अतः तत्त्वार्थमूल, भाष्य और उपासकदशांग की दृष्टि से विचार करें तो उस काल तक वहाँ गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों का भेद ही उत्पन्न नहीं हुआ था अतः उनमें कोई क्रम भंग हुआ यह कहना ही उचित नहीं है । हमें मात्र अवधारणाओं पर ही विचार नहीं करना चाहिए, वरन् उन अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास क्रम को भी समझना चाहिए । दुर्भाग्य से हमारे दिगम्बर विद्वान् अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास क्रम को अपनी दृष्टि से ओझल कर देते हैं, और यह मान लेते हैं आज जैनधर्म का जो रूप है, वह सब महावीर प्रतिपादित है । जिसके परिणामस्वरूप जैन - विद्या का
=
१. 'पंचाअणुवत्तिअं सत्तसिक्खाव इयं दुवालस विहं गिरिधम्मं पडिवज्जिस्सामि । -- उपासकदशांग १।२५ (सं० मधुकर मुनि)
२. तत्त्वार्थ सूत्र ७।१५-१७ ३. ( अ ) दिग्व्रतादिमिरूत्तरव्रतैः सम्पन्नोऽगारी व्रतीभवति ।
(ब) एतानि दिखतादीनि शील्ानि भवति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
- तत्त्वार्थ भाष्य ७।१६ - तत्त्वार्थभाष्य ७।१७
www.jainelibrary.org