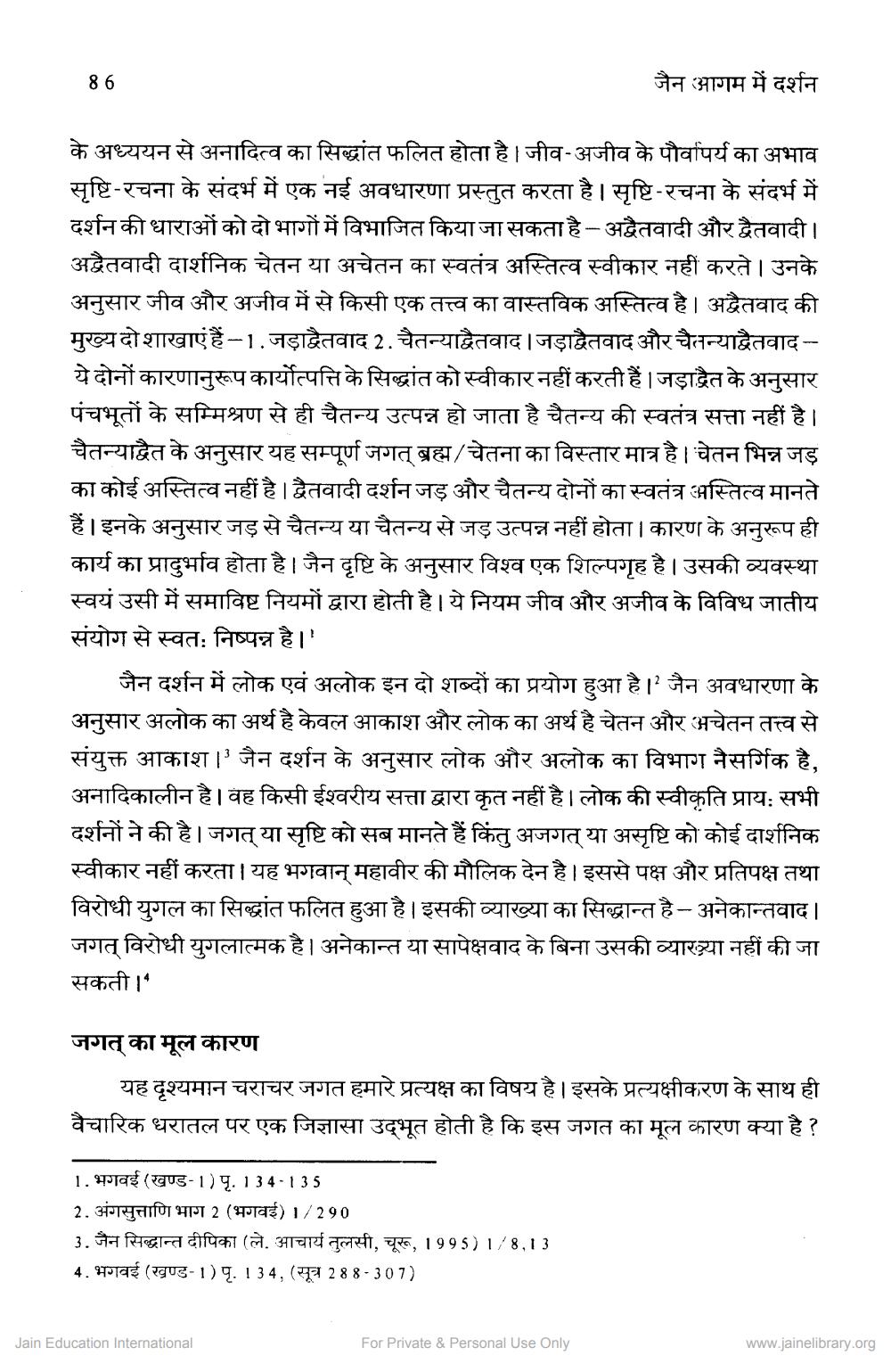________________
86
जैन आगम में दर्शन
के अध्ययन से अनादित्व का सिद्धांत फलित होता है। जीव-अजीव के पौर्वापर्य का अभाव सृष्टि-रचना के संदर्भ में एक नई अवधारणा प्रस्तुत करता है । सृष्टि-रचना के संदर्भ में दर्शन की धाराओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी दार्शनिक चेतन या अचेतन का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार जीव और अजीव में से किसी एक तत्त्व का वास्तविक अस्तित्व है। अद्वैतवाद की मुख्य दोशाखाएं हैं-1.जड़ाद्वैतवाद 2. चैतन्याद्वैतवाद | जड़ाद्वैतवाद और चैतन्याद्वैतवाद-- ये दोनों कारणानुरूप कार्योत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती हैं | जड़ाद्वैत के अनुसार पंचभूतों के सम्मिश्रण से ही चैतन्य उत्पन्न हो जाता है चैतन्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चैतन्याद्वैत के अनुसार यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्म/चेतना का विस्तार मात्र है। चेतन भिन्न जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। द्वैतवादी दर्शन जड़ और चैतन्य दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं। इनके अनुसार जड़ से चैतन्य या चैतन्य से जड़ उत्पन्न नहीं होता । कारण के अनुरूप ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है। जैन दृष्टि के अनुसार विश्व एक शिल्पगृह है। उसकी व्यवस्था स्वयं उसी में समाविष्ट नियमों द्वारा होती है। ये नियम जीव और अजीव के विविध जातीय संयोग से स्वत: निष्पन्न है।'
जैन दर्शन में लोक एवं अलोक इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैन अवधारणा के अनुसार अलोक का अर्थ है केवल आकाश और लोक का अर्थ है चेतन और अचेतन तत्त्व से संयुक्त आकाश ।' जैन दर्शन के अनुसार लोक और अलोक का विभाग नैसर्गिक है, अनादिकालीन है। वह किसी ईश्वरीय सत्ता द्वारा कृत नहीं है। लोक की स्वीकृति प्राय: सभी दर्शनों ने की है। जगत् या सृष्टि को सब मानते हैं किंतु अजगत् या असृष्टि को कोई दार्शनिक स्वीकार नहीं करता। यह भगवान् महावीर की मौलिक देन है। इससे पक्ष और प्रतिपक्ष तथा विरोधी युगल का सिद्धांत फलित हुआ है। इसकी व्याख्या का सिद्धान्त है- अनेकान्तवाद । जगत् विरोधी युगलात्मक है। अनेकान्त या सापेक्षवाद के बिना उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती।
जगत् का मूल कारण
यह दृश्यमान चराचर जगत हमारे प्रत्यक्ष का विषय है। इसके प्रत्यक्षीकरण के साथ ही वैचारिक धरातल पर एक जिज्ञासा उद्भूत होती है कि इस जगत का मूल कारण क्या है ?
1. भगवई (खण्ड-1) पृ. 1 34-135 2. अंगसुत्ताणि भाग 2 (भगवई) 1/290 3. जैन सिद्धान्त दीपिका (ले. आचार्य तुलसी, चूरू, 1995) 1/8,13 4. भगवई (खण्ड-1) पृ. 1 34, (सूत्र 288-307)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org