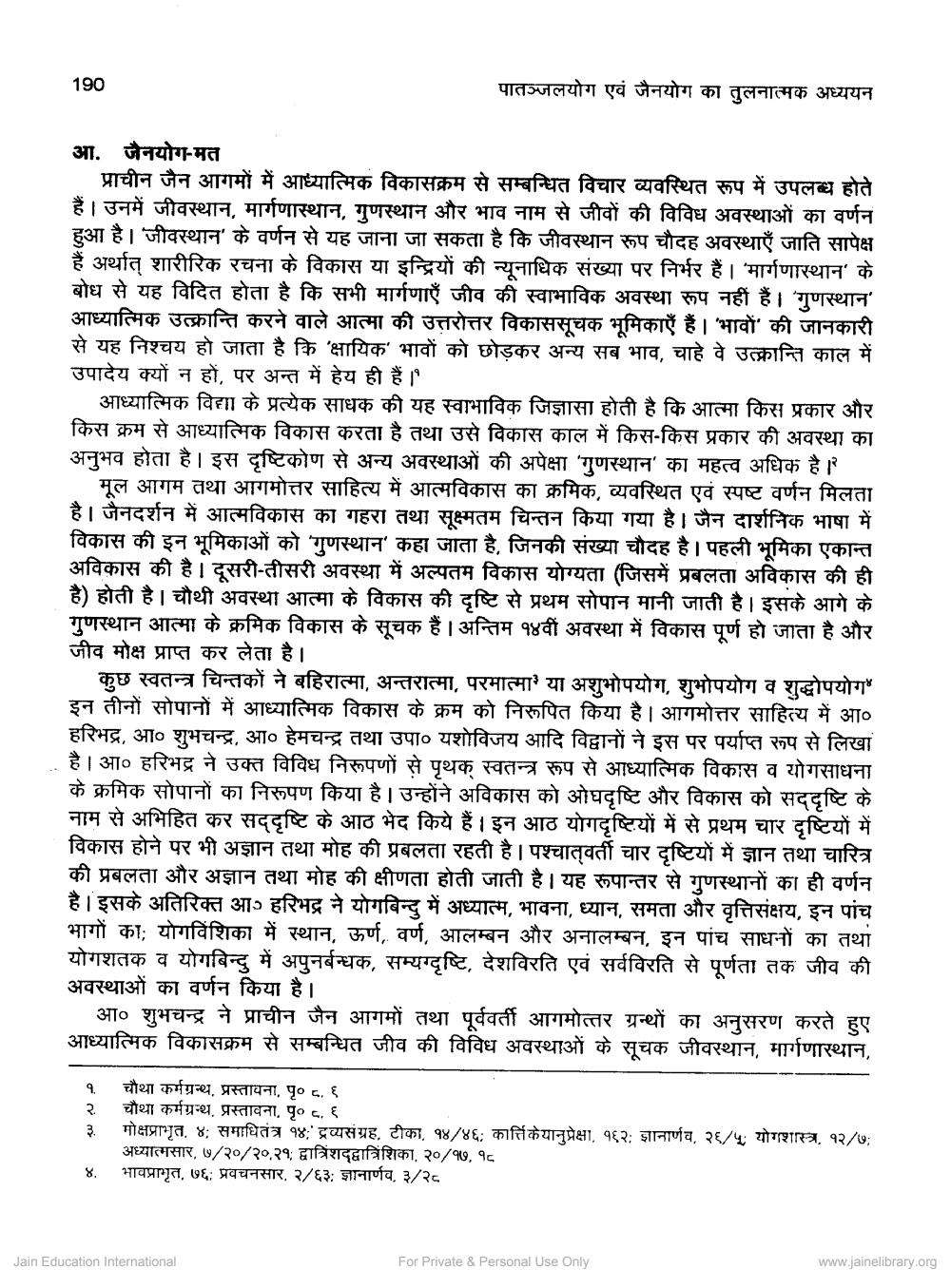________________
190
पातञ्जलयोग एवं जैनयोग का तुलनात्मक अध्ययन
आ. जैनयोग-मत
प्राचीन जैन आगमों में आध्यात्मिक विकासक्रम से सम्बन्धित विचार व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होते हैं। उनमें जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान और भाव नाम से जीवों की विविध अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। जीवस्थान' के वर्णन से यह जाना जा सकता है कि जीवस्थान रूप चौदह अवस्थाएँ जाति सापेक्ष हैं अर्थात् शारीरिक रचना के विकास या इन्द्रियों की न्यूनाधिक संख्या पर निर्भर हैं। ‘मार्गणास्थान' के बोध से यह विदित होता है कि सभी मार्गणाएँ जीव की स्वाभाविक अवस्था रूप नहीं हैं। गुणस्थान' आध्यात्मिक उत्क्रान्ति करने वाले आत्मा की उत्तरोत्तर विकाससूचक भूमिकाएँ हैं। 'भावों' की जानकारी से यह निश्चय हो जाता है कि 'क्षायिक' भावों को छोड़कर अन्य सब भाव, चाहे वे उत्क्रान्ति काल में उपादेय क्यों न हों, पर अन्त में हेय ही हैं।
आध्यात्मिक विहा के प्रत्येक साधक की यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि आत्मा किस प्रकार और किस क्रम से आध्यात्मिक विकास करता है तथा उसे विकास काल में किस-किस प्रकार की अवस्था का अनुभव होता है। इस दृष्टिकोण से अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा 'गुणस्थान' का महत्व अधिक है।
मूल आगम तथा आगमोत्तर साहित्य में आत्मविकास का क्रमिक, व्यवस्थित एवं स्पष्ट वर्णन मिलता है। जैनदर्शन में आत्मविकास का गहरा तथा सूक्ष्मतम चिन्तन किया गया है। जैन दार्शनिक भाषा में विकास की इन भूमिकाओं को 'गुणस्थान' कहा जाता है, जिनकी संख्या चौदह है। पहली भूमिका एकान्त अविकास की है। दूसरी-तीसरी अवस्था में अल्पतम विकास योग्यता (जिसमें प्रबलता अविकास की ही है) होती है। चौथी अवस्था आत्मा के विकास की दृष्टि से प्रथम सोपान मानी जाती है। इसके आगे के गुणस्थान आत्मा के क्रमिक विकास के सूचक हैं । अन्तिम १४वी अवस्था में विकास पूर्ण हो जाता है और जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
कुछ स्वतन्त्र चिन्तकों ने बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा या अशुभोपयोग, शुभोपयोग व शुद्धोपयोग* इन तीनों सोपानों में आध्यात्मिक विकास के क्रम को निरूपित किया है। आगमोत्तर साहित्य में आ० हरिभद्र, आ० शुभचन्द्र, आ० हेमचन्द्र तथा उपा० यशोविजय आदि विद्वानों ने इस पर पर्याप्त रूप से लिखा है। आ० हरिभद्र ने उक्त विविध निरूपणों से पृथक स्वतन्त्र रूप से आध्यात्मिक विकास व योगसाधना के क्रमिक सोपानों का निरूपण किया है। उन्होंने अविकास को ओघदृष्टि और विकास को सददृष्टि के नाम से अभिहित कर सदृष्टि के आठ भेद किये हैं। इन आठ योगदृष्टियों में से प्रथम चार दृष्टियों में विकास होने पर भी अज्ञान तथा मोह की प्रबलता रहती है। पश्चात्वर्ती चार दृष्टियों में ज्ञान तथा चारित्र की प्रबलता और अज्ञान तथा मोह की क्षीणता होती जाती है। यह रूपान्तर से गुणस्थानों का ही वर्णन है। इसके अतिरिक्त आ० हरिभद्र ने योगबिन्दु में अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्तिसंक्षय, इन पांच भागों का; योगविंशिका में स्थान, ऊर्ण, वर्ण, आलम्बन और अनालम्बन, इन पांच साधनों का तथा योगशतक व योगबिन्दु में अपुनर्बन्धक, सम्यग्दृष्टि, देशविरति एवं सर्वविरति से पूर्णता तक जीव की अवस्थाओं का वर्णन किया है। __ आ० शुभचन्द्र ने प्राचीन जैन आगमों तथा पूर्ववर्ती आगमोत्तर ग्रन्थों का अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक विकासक्रम से सम्बन्धित जीव की विविध अवस्थाओं के सूचक जीवस्थान, मार्गणास्थान,
२
चौथा कर्मग्रन्थ, प्रस्तावना, पृ०८.६ चौथा कर्मग्रन्थ, प्रस्तावना, पृ०८.६ मोक्षप्राभृत, ४: समाधितंत्र १४: द्रव्यसंग्रह, टीका. १४/४६: कार्तिकेयानुप्रेक्षा, १६२; ज्ञानार्णव, २६/५: योगशास्त्र. १२/७; अध्यात्मसार, ७/२०/२०,२१: द्वात्रिंशदवात्रिंशिका, २०/१७. १८ भावप्रामृत, ७६; प्रवचनसार. २/६३: ज्ञानार्णव. ३/२८
४.
www.jainelibrary.org
Jain Education International
For Private & Personal Use Only