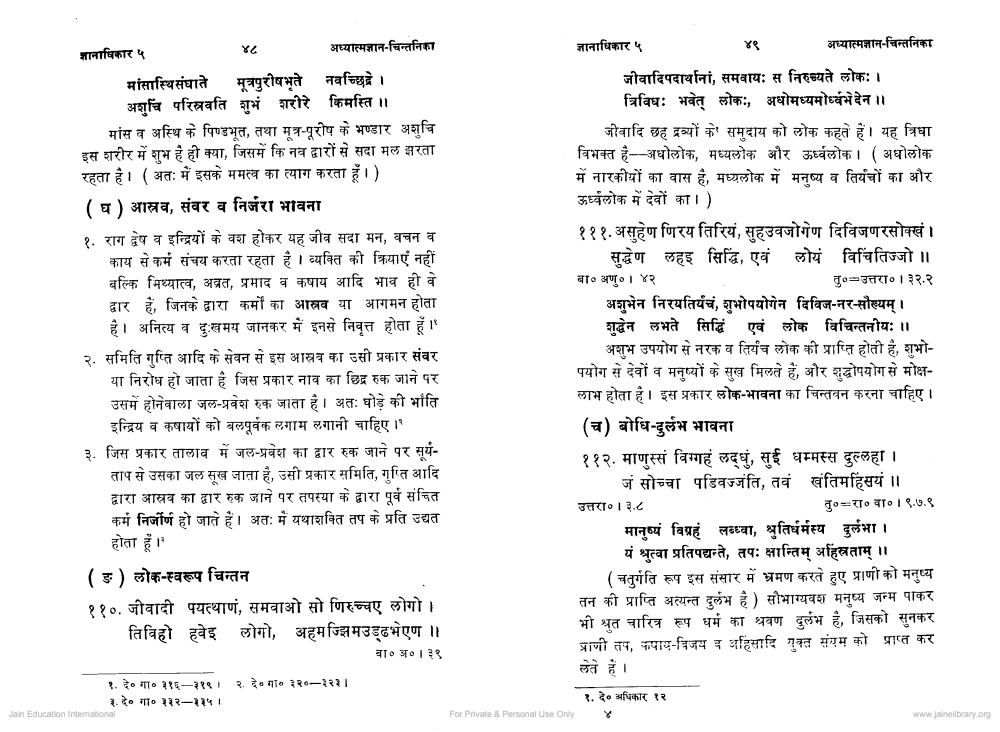________________
ज्ञानाधिकार ५
अध्यात्मज्ञान-चिन्तनिका मांसास्थिसंघाते मूत्रपुरीषभृते नवच्छिद्रे ।
अशुचि परिस्रवति शुभं शरीरे किमस्ति । मांस व अस्थि के पिण्डभूत, तथा मूत्र-पूरीष के भण्डार अशुचि इस शरीर में शुभ है ही क्या, जिसमें कि नव द्वारों से सदा मल झरता रहता है। ( अतः मैं इसके ममत्व का त्याग करता हूँ।) (घ) आस्रव, संवर व निर्जरा भावना १. राग द्वेष व इन्द्रियों के वश होकर यह जीव सदा मन, वचन व
काय से कर्म संचय करता रहता है। व्यक्ति की क्रियाएं नहीं बल्कि मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद व कषाय आदि भाव ही वे द्वार है, जिनके द्वारा कर्मों का आस्रव या आगमन होता
है। अनित्य व दुःखमय जानकर में इनसे निवृत्त होता हूँ।" २. समिति गुप्ति आदि के सेवन से इस आस्रव का उसी प्रकार संवर
या निरोध हो जाता है जिस प्रकार नाव का छिद्र रुक जाने पर उसमें होनेवाला जल-प्रवेश रुक जाता है। अतः घोड़े की भांति
इन्द्रिय व कषायों को बलपूर्वक लगाम लगानी चाहिए। ३. जिस प्रकार तालाब में जल-प्रवेश का द्वार रुक जाने पर सूर्य
ताप से उसका जल सूख जाता है, उसी प्रकार समिति, गुरित आदि द्वारा आस्रव का द्वार रुक जाने पर तपस्या के द्वारा पूर्व संचित कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं। अतः मैं यथाशक्ति तप के प्रति उद्यत
होता हूँ। (ङ) लोक-स्वरूप चिन्तन ११०. जीवादी पयत्थाणं, समवाओ सो णिरुच्चए लोगो। तिविहो हवेइ लोगो, अहमज्झिमउड्ढभेएण ॥
वा० अ०।३९
ज्ञानाधिकार ५
अध्यात्मज्ञान-चिन्तनिका जीवादिपदार्थानां, समवायः स निरुच्यते लोकः । त्रिविधः भवेत् लोकः, अधोमध्यमोलभेदेन ॥ जीवादि छह द्रव्यों के समुदाय को लोक कहते हैं। यह त्रिधा विभक्त है--अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। (अधोलोक में नारकीयों का वास है, मध्यलोक में मनुष्य व तिर्यंचों का और ऊर्ध्वलोक में देवों का।) १११. असुहेण णिरय तिरिय, सुहउवजोगेण दिविजणरसोक्खं ।
सुद्धण लहइ सिद्धि, एवं लोयं विचितिज्जो ॥ बा० अणुः । ४२
तु०उत्तरा० । ३२.२ अशुभेन निरयतिर्यचं, शुभोपयोगेन दिविज-नर-सौख्यम्। शुद्धेन लभते सिद्धि एवं लोक विचिन्तनीयः ॥
अशुभ उपयोग से नरक व तिर्यंच लोक की प्राप्ति होती है, शुभोपयोग से देवों व मनुष्यों के सुख मिलते हैं, और शुद्धोपयोग से मोक्षलाभ होता है। इस प्रकार लोक-भावना का चिन्तवन करना चाहिए। (च) बोधि-दुर्लभ भावना ११२. माणुस्सं विग्गहं ल , सुई धम्मस्स दुल्लहा ।
जं सोच्चा पडिवज्जति, तवं खंतिमहिंसयं ॥ उत्तरा०।३.८
तु०रा० वा० । ९.७.९ मानुष्यं विग्रहं लब्ध्वा, श्रुतिधर्मस्य दुर्लभा।
यं श्रुत्वा प्रतिपद्यन्ते, तपः क्षान्तिम् अहिंस्रताम् ॥ ( चतुर्गति रूप इस संसार में भ्रमण करते हुए प्राणी को मनुष्य तन की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है) सौभाग्यवश मनुष्य जन्म पाकर भी श्रुत चारित्र रूप धर्म का धवण दुर्लभ है, जिसको सुनकर प्राणी तप, कपाय-विजय द अहिंसादि गुक्त संयम को प्राप्त कर लेते हैं।
१. दे० गा०३१६–३१९ । २. देगा० ३२०-३२३ ।
३.दे० गा०३३२-३३५ । Jain Education International
१.दे० अधिकार १२
For Private & Personal use only
www.jainelibrary.org