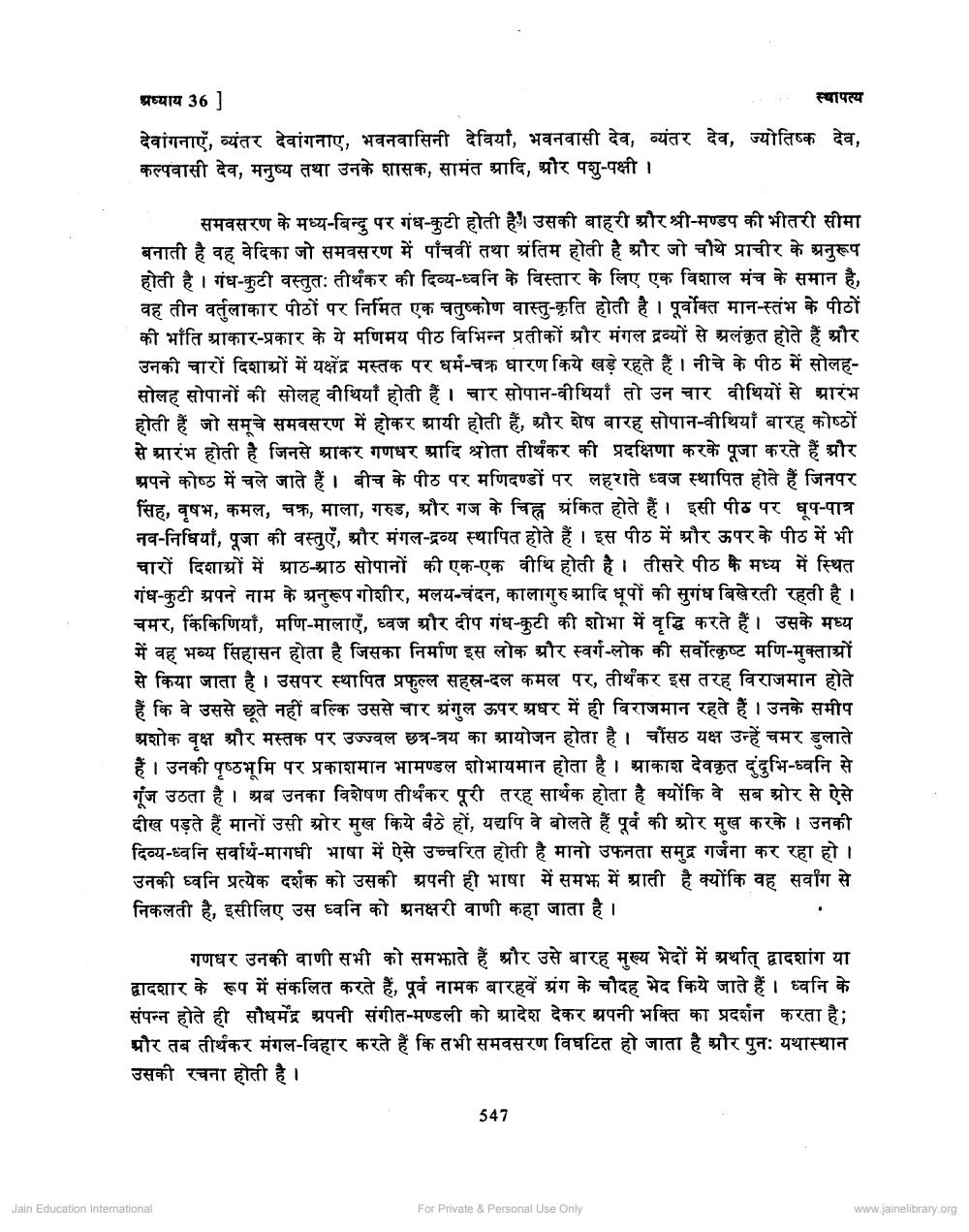________________
अध्याय 36 ]
स्थापत्य देवांगनाएँ, व्यंतर देवांगनाए, भवनवासिनी देवियां, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष्क देव, कल्पवासी देव, मनुष्य तथा उनके शासक, सामंत आदि, और पशु-पक्षी।
समवसरण के मध्य-बिन्दु पर गंध-कूटी होती है। उसकी बाहरी और श्री-मण्डप की भीतरी सीमा बनाती है वह वेदिका जो समवसरण में पाँचवीं तथा अंतिम होती है और जो चौथे प्राचीर के अनुरूप होती है। गंध-कूटी वस्तुतः तीर्थंकर की दिव्य-ध्वनि के विस्तार के लिए एक विशाल मंच के समान है, वह तीन वर्तुलाकार पीठों पर निर्मित एक चतुष्कोण वास्तु-कृति होती है । पूर्वोक्त मान-स्तंभ के पीठों की भाँति आकार-प्रकार के ये मणिमय पीठ विभिन्न प्रतीकों और मंगल द्रव्यों से अलंकृत होते हैं और उनकी चारों दिशाओं में यक्षंद्र मस्तक पर धर्म-चक्र धारण किये खड़े रहते हैं। नीचे के पीठ में सोलहसोलह सोपानों की सोलह वीथियाँ होती हैं। चार सोपान-वीथियाँ तो उन चार वीथियों से प्रारंभ होती हैं जो समूचे समवसरण में होकर आयी होती हैं, और शेष बारह सोपान-वीथियाँ बारह कोष्ठों से प्रारंभ होती है जिनसे पाकर गणधर आदि श्रोता तीर्थंकर की प्रदक्षिणा करके पूजा करते हैं और अपने कोष्ठ में चले जाते हैं। बीच के पीठ पर मणिदण्डों पर लहराते ध्वज स्थापित होते हैं जिनपर सिंह, वृषभ, कमल, चक्र, माला, गरुड, और गज के चिह्न अंकित होते हैं। इसी पीठ पर धूप-पात्र नव-निधियाँ, पूजा की वस्तुएँ, और मंगल-द्रव्य स्थापित होते हैं । इस पीठ में और ऊपर के पीठ में भी चारों दिशाओं में पाठ-पाठ सोपानों की एक-एक वीथि होती है। तीसरे पीठ के मध्य में स्थित गंध-कुटी अपने नाम के अनुरूप गोशीर, मलय-चंदन, कालागुरु आदि धूपों की सुगंध बिखेरती रहती है। चमर, किंकिणियाँ, मणि-मालाएँ, ध्वज और दीप गंध-कुटी की शोभा में वृद्धि करते हैं। उसके मध्य में वह भव्य सिंहासन होता है जिसका निर्माण इस लोक और स्वर्ग-लोक की सर्वोत्कृष्ट मणि-मुक्ताओं से किया जाता है । उसपर स्थापित प्रफुल्ल सहस्र-दल कमल पर, तीर्थंकर इस तरह विराजमान होते हैं कि वे उससे छूते नहीं बल्कि उससे चार अंगुल ऊपर अधर में ही विराजमान रहते हैं । उनके समीप अशोक वृक्ष और मस्तक पर उज्ज्वल छत्र-त्रय का आयोजन होता है। चौंसठ यक्ष उन्हें चमर डुलाते हैं। उनकी पृष्ठभमि पर प्रकाशमान भामण्डल शोभायमान होता है। आकाश देवकृत दंदुभि-ध्वनि से गूंज उठता है। अब उनका विशेषण तीर्थकर पूरी तरह सार्थक होता है क्योंकि वे सब ओर से ऐसे दीख पड़ते हैं मानों उसी ओर मुख किये बैठे हों, यद्यपि वे बोलते हैं पूर्व की ओर मुख करके । उनकी दिव्य-ध्वनि सर्वार्थ-मागधी भाषा में ऐसे उच्चरित होती है मानो उफनता समुद्र गर्जना कर रहा हो। उनकी ध्वनि प्रत्येक दर्शक को उसकी अपनी ही भाषा में समझ में आती है क्योंकि वह सर्वांग से निकलती है, इसीलिए उस ध्वनि को अनक्षरी वाणी कहा जाता है।
गणधर उनकी वाणी सभी को समझाते हैं और उसे बारह मुख्य भेदों में अर्थात् द्वादशांग या द्वादशार के रूप में संकलित करते हैं, पूर्व नामक बारहवें अंग के चौदह भेद किये जाते हैं। ध्वनि के संपन्न होते ही सौधर्मेंद्र अपनी संगीत-मण्डली को आदेश देकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करता है; पौर तब तीर्थकर मंगल-विहार करते हैं कि तभी समवसरण विघटित हो जाता है और पुनः यथास्थान उसकी रचना होती है।
547
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org