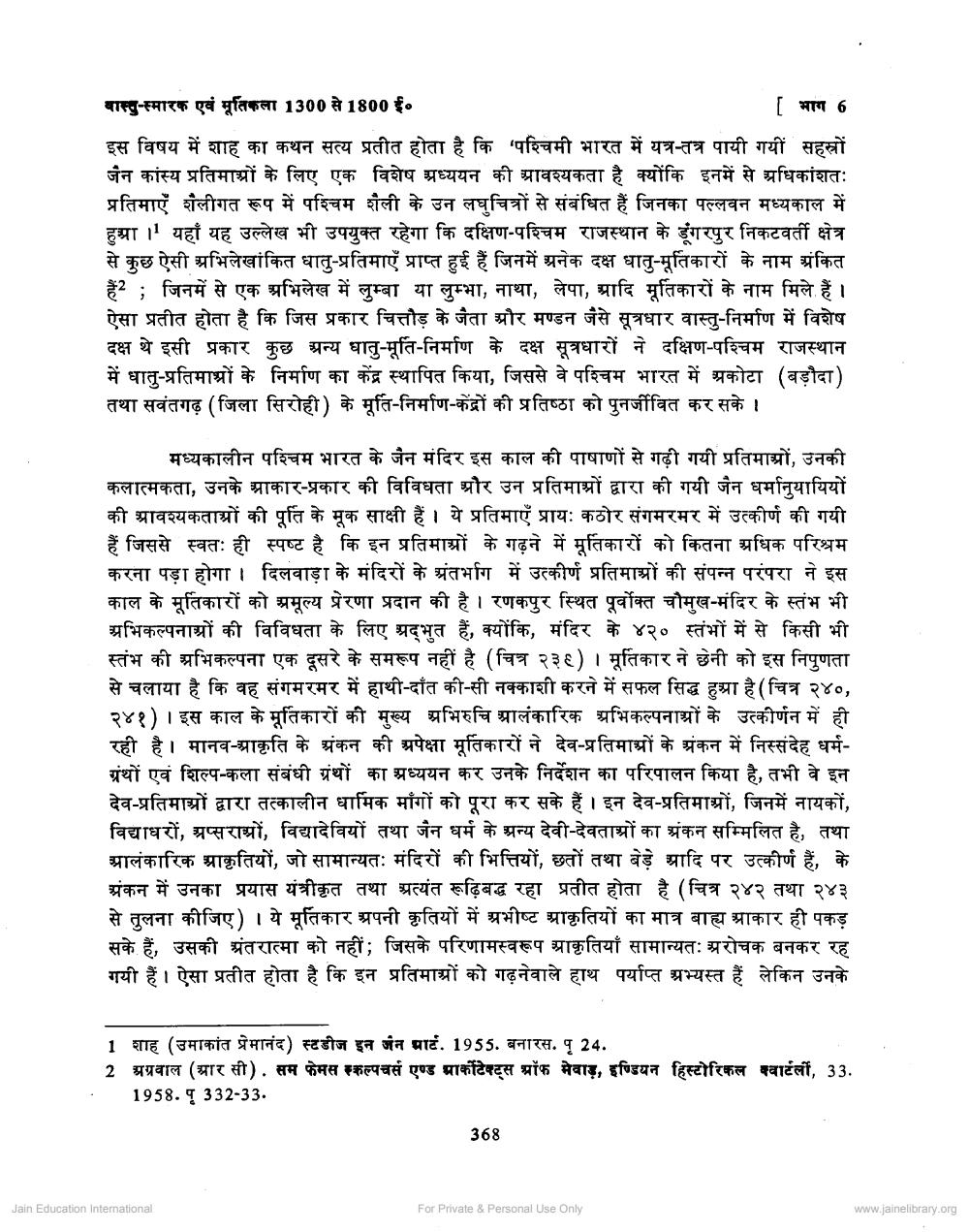________________
वास्तु-स्मारक एवं मूर्तिकला 1300 से 1800 ई.
[ भाग 6 इस विषय में शाह का कथन सत्य प्रतीत होता है कि 'पश्चिमी भारत में यत्र-तत्र पायी गयीं सहस्रों जैन कांस्य प्रतिमाओं के लिए एक विशेष अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से अधिकांशतः प्रतिमाएँ शैलीगत रूप में पश्चिम शैली के उन लघुचित्रों से संबंधित हैं जिनका पल्लवन मध्यकाल में हुआ । यहाँ यह उल्लेख भी उपयुक्त रहेगा कि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के डूंगरपुर निकटवर्ती क्षेत्र से कुछ ऐसी अभिलेखांकित धातु-प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जिनमें अनेक दक्ष धातु-मूर्तिकारों के नाम अंकित हैं2 ; जिनमें से एक अभिलेख में लुम्बा या लुम्भा, नाथा, लेपा, आदि मूर्तिकारों के नाम मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार चित्तौड़ के जैता और मण्डन जैसे सूत्रधार वास्तु-निर्माण में विशेष दक्ष थे इसी प्रकार कुछ अन्य धातु-मूर्ति-निर्माण के दक्ष सूत्रधारों ने दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में धातु-प्रतिमाओं के निर्माण का केंद्र स्थापित किया, जिससे वे पश्चिम भारत में अकोटा (बड़ौदा) तथा सवंतगढ़ (जिला सिरोही) के मूर्ति-निर्माण-केंद्रों की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित कर सके ।
मध्यकालीन पश्चिम भारत के जैन मंदिर इस काल की पाषाणों से गढ़ी गयी प्रतिमाओं, उनकी कलात्मकता, उनके आकार-प्रकार की विविधता और उन प्रतिमाओं द्वारा की गयी जैन धर्मानुयायियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के मूक साक्षी हैं। ये प्रतिमाएँ प्रायः कठोर संगमरमर में उत्कीर्ण की गयी हैं जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि इन प्रतिमाओं के गढ़ने में मूर्तिकारों को कितना अधिक परिश्रम करना पड़ा होगा। दिलवाड़ा के मंदिरों के अंतर्भाग में उत्कीर्ण प्रतिमाओं की संपन्न परंपरा ने इस काल के मूर्तिकारों को अमूल्य प्रेरणा प्रदान की है। रणकपुर स्थित पूर्वोक्त चौमुख-मंदिर के स्तंभ भी अभिकल्पनाओं की विविधता के लिए अद्भुत हैं, क्योंकि, मंदिर के ४२० स्तंभों में से किसी भी स्तंभ की अभिकल्पना एक दूसरे के समरूप नहीं है (चित्र २३६)। मूर्तिकार ने छेनी को इस निपुणता से चलाया है कि वह संगमरमर में हाथी-दाँत की-सी नक्काशी करने में सफल सिद्ध हआ है (चित्र २४०, २४१) । इस काल के मूर्तिकारों की मुख्य अभिरुचि आलंकारिक अभिकल्पनाओं के उत्कीर्णन में ही रही है। मानव-आकृति के अंकन की अपेक्षा मूर्तिकारों ने देव-प्रतिमाओं के अंकन में निस्संदेह धर्मग्रंथों एवं शिल्प-कला संबंधी ग्रंथों का अध्ययन कर उनके निर्देशन का परिपालन किया है, तभी वे इन देव-प्रतिमाओं द्वारा तत्कालीन धार्मिक मांगों को पूरा कर सके हैं। इन देव-प्रतिमाओं, जिनमें नायकों, विद्याधरों, अप्सराओं, विद्यादेवियों तथा जैन धर्म के अन्य देवी-देवताओं का अंकन सम्मिलित है, तथा आलंकारिक प्राकृतियों, जो सामान्यतः मंदिरों की भित्तियों, छतों तथा बेड़े आदि पर उत्कीर्ण हैं, के अंकन में उनका प्रयास यंत्रीकृत तथा अत्यंत रूढिबद्ध रहा प्रतीत होता है (चित्र २४२ तथा २४३ से तुलना कीजिए) । ये मूर्तिकार अपनी कृतियों में अभीष्ट आकृतियों का मात्र बाह्य आकार ही पकड़ सके हैं, उसकी अंतरात्मा को नहीं; जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतियाँ सामान्यतः अरोचक बनकर रह गयी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रतिमाओं को गढ़नेवाले हाथ पर्याप्त अभ्यस्त हैं लेकिन उनके
1 शाह (उमाकांत प्रेमानंद) स्टडीज इन जैन मार्ट. 1955. बनारस. पृ 24. 2 अग्रवाल (आर सी). सम फेमस स्कल्पचर्स एण्ड मार्कीटेक्ट्स ऑफ मेवाड़, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टलों, 33.
1958. पृ 332-33.
368
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org