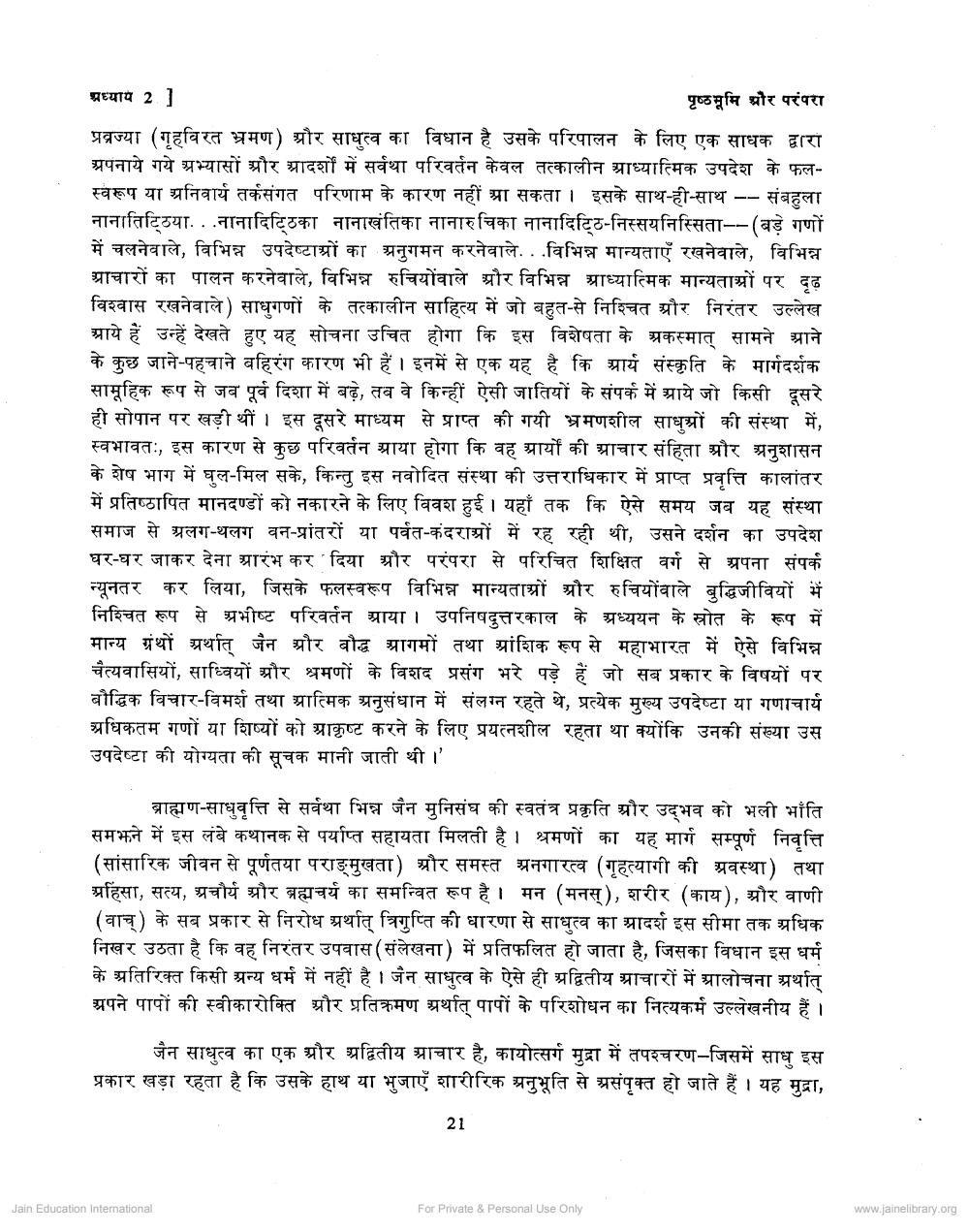________________
अध्याय 2 ]
पृष्ठभूमि और परंपरा
प्रव्रज्या (गृहविरत भ्रमण ) और साधुत्व का विधान है उसके परिपालन के लिए एक साधक द्वारा अपनाये गये अभ्यासों और आदर्शों में सर्वथा परिवर्तन केवल तत्कालीन आध्यात्मिक उपदेश के फलस्वरूप या अनिवार्य तर्कसंगत परिणाम के कारण नहीं आ सकता। इसके साथ-ही-साथ संबहुला नानातिट्ठिया नानादिट्टिका नानाखंतिका नानारुचिका नानादिट्ठि निस्सयनिस्सिता -- ( बड़े गणों में चलनेवाले, विभिन्न उपदेष्टाओं का अनुगमन करनेवाले विभिन्न मान्यताएँ रखनेवाले, विभिन्न आचारों का पालन करनेवाले, विभिन्न रुचियोंवाले और विभिन्न प्राध्यात्मिक मान्यताओं पर दृढ़ विश्वास रखनेवाले) साधुगणों के तत्कालीन साहित्य में जो बहुत-से निश्चित और निरंतर उल्लेख
ये हैं उन्हें देखते हुए यह सोचना उचित होगा कि इस विशेषता के अकस्मात् सामने आने के कुछ जाने-पहचाने बहिरंग कारण भी हैं । इनमें से एक यह है कि आर्य संस्कृति के मार्गदर्शक सामूहिक रूप से जब पूर्व दिशा में बढ़े, तब वे किन्हीं ऐसी जातियों के संपर्क में आये जो किसी दूसरे ही सोपान पर खड़ी थीं । इस दूसरे माध्यम से प्राप्त की गयी भ्रमणशील साधुओं की संस्था में, स्वभावतः, इस कारण से कुछ परिवर्तन आया होगा कि वह आर्यों की आचार संहिता और अनुशासन के शेष भाग में घुल-मिल सके, किन्तु इस नवोदित संस्था की उत्तराधिकार में प्राप्त प्रवृत्ति कालांतर में प्रतिष्ठापित मानदण्डों को नकारने के लिए विवश हुई । यहाँ तक कि ऐसे समय जब यह संस्था समाज से अलग-थलग वन प्रांतरों या पर्वत कंदराओं में रह रही थी, उसने दर्शन का उपदेश घर-घर जाकर देना आरंभ कर दिया और परंपरा से परिचित शिक्षित वर्ग से अपना संपर्क न्यूनतर कर लिया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न मान्यताओं और रुचियोंवाले बुद्धिजीवियों में निश्चित रूप से अभीष्ट परिवर्तन आया। उपनिषदुत्तरकाल के अध्ययन के स्रोत के रूप में मान्य ग्रंथों अर्थात् जैन और बौद्ध आगमों तथा प्रांशिक रूप से महाभारत में ऐसे विभिन्न चैत्यवासियों, साध्वियों और श्रमणों के विशद प्रसंग भरे पड़े हैं जो सब प्रकार के विषयों पर बौद्धिक विचार-विमर्श तथा प्रात्मिक अनुसंधान में संलग्न रहते थे, प्रत्येक मुख्य उपदेष्टा या गणाचार्य अधिकतम गणों या शिष्यों को आकृष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहता था क्योंकि उनकी संख्या उस उपदेष्टा की योग्यता की सूचक मानी जाती थी ।'
ब्राह्मण साधुवृत्ति से सर्वथा भिन्न जैन मुनिसंघ की स्वतंत्र प्रकृति और उद्भव को भली भाँति समझने में इस लंबे कथानक से पर्याप्त सहायता मिलती है । श्रमणों का यह मार्ग सम्पूर्ण निवृत्ति ( सांसारिक जीवन से पूर्णतया पराङ्मुखता ) और समस्त अनगारत्व (गृहत्यागी की अवस्था ) तथा अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य का समन्वित रूप है । मन (मनस् ), शरीर ( काय ), और वाणी ( वाच्) के सब प्रकार से निरोध अर्थात् त्रिगुप्ति की धारणा से साधुत्व का आदर्श इस सीमा तक अधिक निखर उठता है कि वह निरंतर उपवास (संलेखना ) में प्रतिफलित हो जाता है, जिसका विधान इस धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म में नहीं है । जैन साधुत्व के ऐसे ही अद्वितीय प्राचारों में आलोचना अर्थात् अपने पापों की स्वीकारोक्ति और प्रतिक्रमण अर्थात् पापों के परिशोधन का नित्यकर्म उल्लेखनीय हैं ।
जैन साधुत्व का एक और अद्वितीय आचार है, कायोत्सर्ग मुद्रा में तपश्चरण - जिसमें साधु इस प्रकार खड़ा रहता है कि उसके हाथ या भुजाएँ शारीरिक अनुभूति से असंपृक्त हो जाते हैं । यह मुद्रा,
Jain Education International
11
21
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org